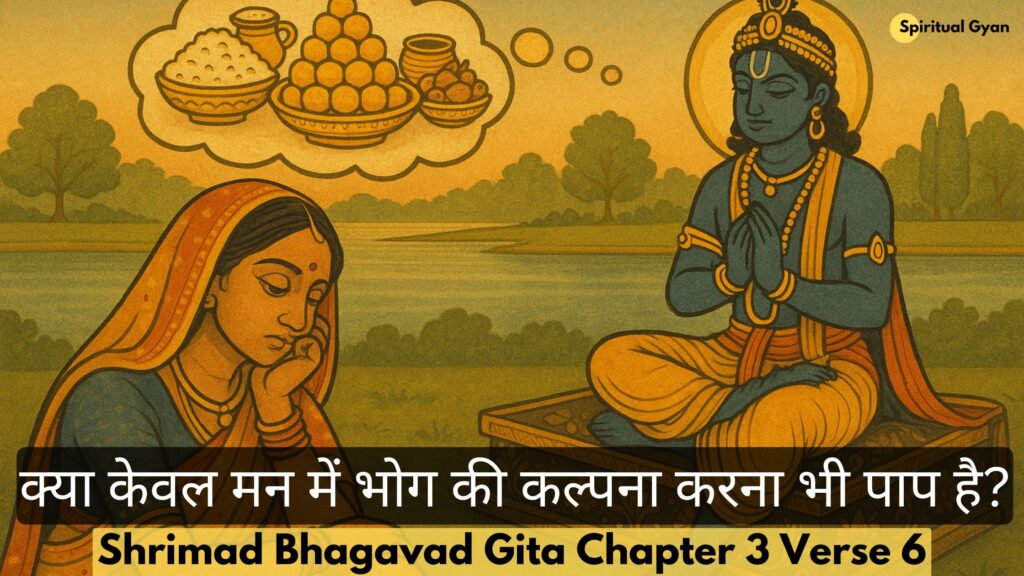
Bhagavad Gita Chapter 3 Verse 6
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् |
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते || 6 ||
अर्थात भगवान कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य कर्मेन्द्रियों (समस्त इन्द्रियों) को बलपूर्वक रोककर मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करता रहता है, उसे मिथ्याचारी (झूठ का आचरण करने वाला) कहा जाता है।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 6 Meaning in Hindi
क्यों गीता मानसिक चिंतन को भी कर्म मानती है?
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते
यहां ‘कर्मेन्द्रियाणि’ पद का अभिप्राय पाँच कर्मेन्द्रियाँ (वाणी, हाथ, पैर, मुख और गुदा) ही नहीं, अपितु पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण) भी सम्मिलित हैं, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों के बिना केवल कर्मेन्द्रियों से ही कर्म नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त केवल हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियों को रोकने से और आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों को न रोकने से पूर्ण मिथ्यात्व भी प्राप्त नहीं होता। गीता में ज्ञानेन्द्रियों को कर्मेन्द्रियों के अन्तर्गत माना गया है। इसीलिए गीता में कर्मेन्द्रियाँ शब्द तो आता है, परन्तु ज्ञानेन्द्रियाँ शब्द कहीं नहीं आता। पाँचवें अध्याय के आठवें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेन्द्रियों के कर्मों को भी कर्मेन्द्रियों के कर्मों के साथ सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेन्द्रियों को भी कर्मेन्द्रियाँ ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है, पांचवें श्लोक में कहा गया है: ‘शरीर का मन शरीर में ही क्रियाशील रहता है।’ (Ch 18/15) तात्पर्य यह है कि चूँकि प्रकृति के कार्य में ही प्रकृति क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति के कार्य में ही प्रकृति क्रियाशील रहती है।
मूढ़ बुद्धि वाला (सत्य-असत्य का विवेक न रखने वाला) मनुष्य बाहर से तो इन्द्रियों के कर्मों को बलपूर्वक रोक लेता है, परन्तु मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करता रहता है और ऐसी अवस्था को निष्कर्म मानता है। इसीलिए वह मिथ्या अर्थात् मिथ्या कर्म करने वाला कहलाता है।
यद्यपि उसने बाहर से इन्द्रियों के विषयों का त्याग कर दिया है और समझता है कि मैं कर्म नहीं करता, परन्तु ऐसी अवस्था में भी वह वास्तव में निष्कर्म नहीं हुआ है। क्योंकि बाहर से निष्कर्म प्रतीत होने पर भी अहंकार, आसक्ति और कामना के कारण इन्द्रिय-भोग रूपी चिन्तन रूपी कर्म तो चल ही रहा है।
यह भी पढ़ें : क्या अशांत मन वाला व्यक्ति सच्चा सुख पा सकता है?
सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और बाहर से राग से भोगने पर जैसे भोगों के संस्कार हृदय में बनते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगने पर अर्थात् राग से भोगों का चिंतन करने पर भी बनते हैं। मनुष्य बाहर से भोगों को विचार, लोक-लाज तथा व्यवहार में विपत्ति आने के भय से त्याग सकता है, परंतु मन से भोगों को भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। इसलिए वह मन से भोगता रहता है और झूठ-मूठ दावा करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूं। मन से भोगना विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि उसके उपभोग का अवसर अधिक मिलता है, इसलिए साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वह बाहरी भोगों से अपने को बचाकर उनका त्याग करता है, वैसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे।
अर्जुन भी कर्म का त्याग करना चाहता है और भगवान से पूछता है कि आप मुझे ऐसे जघन्य कर्म में क्यों लगाते हैं? उत्तर में भगवान यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार, ममता, आसक्ति, वासना आदि को धारण करके केवल बाह्य रूप से कर्म का त्याग करता है और अपने को कर्म से रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु वासना और आसक्ति से रहित होकर तत्परता से कर्म करते रहना चाहिए।
चौथे श्लोक में भगवान् ने कर्मयोग और सांख्ययोग दोनों की दृष्टि से कर्मों के त्याग को अनावश्यक बताया। फिर पाँचवें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। छठे श्लोक में उन्होंने उन लोगों के आचरण की मिथ्याता बताई जो बलपूर्वक इन्द्रियों के कर्मों को रोकते हैं और अपने को कर्महीन मानते हैं। इससे सिद्ध होता है कि केवल कर्मों का रूप से त्याग करने से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः अगले श्लोक में भगवान् वास्तविक त्याग का परिचय देते हैं।
FAQs
क्या केवल मन में भोग की कल्पना करना भी पाप है?
हाँ, भगवद गीता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाह्य रूप से इन्द्रियों को नियंत्रित करता है, परंतु मन से भोग-विषयों का चिंतन करता रहता है, तो वह भी मिथ्याचार (पाखंडी) कहलाता है। मन में किया गया भोग भी वैसा ही प्रभाव छोड़ता है जैसा वास्तविक भोग। इसलिए केवल बाहरी त्याग पर्याप्त नहीं, मन से भी वासना, आसक्ति और भोग की कल्पनाओं को त्यागना आवश्यक है।
क्या सिर्फ विचारों में भोग की इच्छा भी पाप मानी जाती है?
हाँ, गीता के अनुसार मन में भोग-विषयों का चिंतन करते रहना भी पाप है। यह भीतर की वासना को बढ़ाता है और व्यक्ति के साधन को भ्रष्ट करता है।
क्या इन्द्रियों को रोकना पर्याप्त है, अगर मन भटकता रहे?
नहीं, यदि केवल इन्द्रियों को बलपूर्वक रोका जाए और मन में इच्छाओं का चिंतन चलता रहे, तो वह स्थिति गीता अनुसार ‘मिथ्याचार’ कहलाती है।
गीता के अनुसार सच्चा त्याग क्या है?
सच्चा त्याग केवल बाहरी कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि मन की वासना, मोह और कामना का पूर्ण परित्याग है। यही निष्काम कर्म का मार्ग है।











