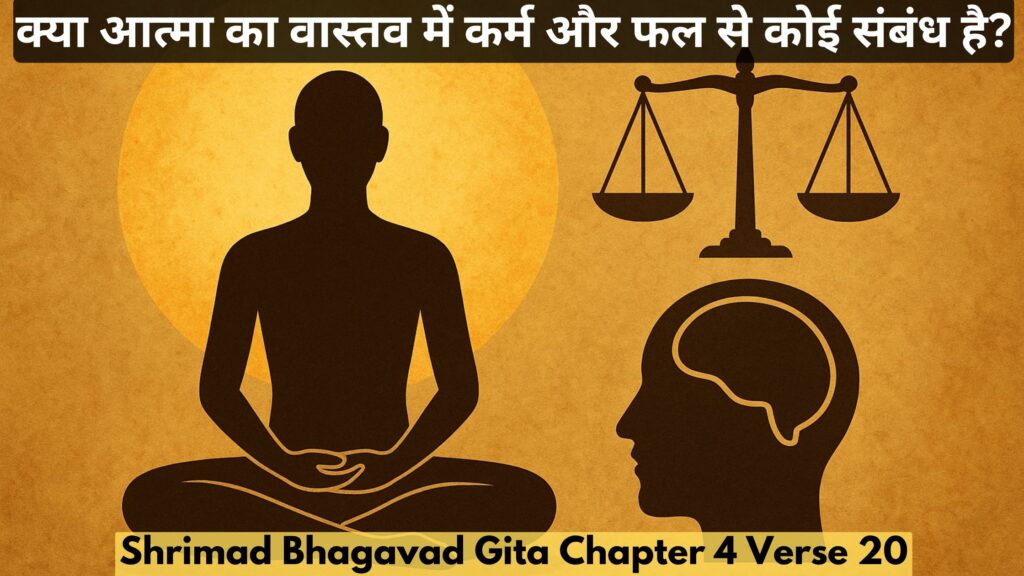
Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 20
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥२०॥
अर्थात भगवान कहते हैं, जो मनुष्य कर्म और फल की आसक्ति को त्यागकर, आश्रय से मुक्त होकर तथा सदैव संतुष्ट रहता है, वह कर्म में भली-भाँति संलग्न रहता है, फिर भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 4 Shloka 20 Meaning in Hindi
क्या आत्मा का वास्तव में कर्म और फल से कोई संबंध है?
–त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग
जब कर्ता कर्म करते हुए यह अनुभव करता है कि शरीर आदि उसकी भौतिक वस्तुएँ हैं। मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म मेरा है और मेरे लिए है तथा मुझे इसका कुछ फल मिलेगा। तब वह कर्म के फल की इच्छा करता है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष प्राकृतिक वस्तुओं से पूर्ण वैराग्य का अनुभव करता है। इसीलिए, चूँकि उसे कर्म की भौतिक वस्तुओं, कर्म और कर्म के फल में किंचितमात्र भी आसक्ति नहीं होती, इसलिए वह कर्म के फल की इच्छा नहीं करता।
सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। जब विजय प्राप्त होती है, तो विजय सेना की नहीं, बल्कि राजा की होती है। क्योंकि राजा ने स्वयं सेना की जीविका की व्यवस्था की है। उन्हें युद्ध की सामग्री दी है और युद्ध के लिए प्रेरित किया है और सेना भी राजा के लिए युद्ध करती है। इसी प्रकार, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि कर्म की भौतिक वस्तुओं से जुड़कर, आत्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी बन जाती है।
वास्तव में, स्वरूप और कर्मफल में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि स्वरूप चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है,किन्तु कर्म और कर्मफल दोनों अनित्य और परिवर्तनशील हैं तथा उनका आदि और अंत है। शाश्वत रूप के साथ न तो कर्म रहता है और न ही फल। इस प्रकार, यद्यपि स्वरूप का कर्म और फल से कोई संबंध नहीं है, फिर भी जीव ने भूलवश उनसे अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। यदि इस माने हुए संबंध को हटा दिया जाए, तो कर्म और फल से उसकी अंतर्निहित अनासक्ति का बोध होता है।
गीता के अनुसार ‘निराश्रय’ कौन कहलाता है?
–निराश्रयः
देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति किंचित मात्र भी शरण न लेना ‘निराश्रय’ कहलाता है, अर्थात शरण से रहित होना। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान या शक्तिशाली क्यों न हो, उसे देश, काल आदि की शरण लेनी ही पड़ती है। परन्तु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि को शरण नहीं मानता। उसे आश्रम मिले या न मिले, इसकी उसे तनिक भी परवाह नहीं, इसीलिए वह निराश्रय है।
यह भी पढ़ें : क्या भगवान हर युग में अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए?
आत्मा को शाश्वत संतोष कब मिलता है?
–नित्यतृप्त:
आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत्यस्वरूप है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। जब वह असत् के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब उसे अभाव अर्थात् न्यूनता का अनुभव होने लगता है। उस न्यूनता की पूर्ति के लिए वह सांसारिक पदार्थों की कामना करने लगता है। इच्छित पदार्थों की प्राप्ति से तृप्ति होती है, परन्तु वह तृप्ति स्थायी नहीं होती, क्षणिक होती है। क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर अग्रसर हो रही है, अतः उनका आश्रय लेने वाला संतोष स्थायी कैसे रह सकता है? असत् वस्तु से सत् वस्तु का संतोष कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः जब तक आत्मा उत्पत्ति और विनाश के अधीन कर्मों और पदार्थों के साथ अपना सम्बन्ध मानता है और उनके अधीन रहता है, तब तक उसे स्वतःसिद्ध शाश्वत संतोष का अनुभव नहीं होता।
गीता के अनुसार कर्म में संलग्न होकर भी निष्क्रिय कैसे रहा जा सकता है?
–कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः
‘अभिप्रवृत्तः’ शब्द का अर्थ है कि कर्मयोग को प्राप्त महापुरुष द्वारा किए गए सभी कर्म सम्यक् रीति से किए जाते हैं, क्योंकि उसके कर्मफल में इस शक्ति का लेशमात्र भी अंश नहीं होता, उसके सभी कर्म संसार के विनाश के लिए ही होते हैं।
‘अपि’ शब्द का अर्थ यह है कि वह सभी कर्मों को समभावपूर्वक करता हुआ भी वास्तव में कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि वह पूर्णतया अनासक्त होने के कारण कर्मों से अछूता रहता है। उसके सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं।
प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है। अतः जब तक प्रकृति के गुणों (क्रिया और द्रव्य) के साथ संबंध बना रहता है, तब तक मनुष्य कर्म न करने पर भी कर्म से संबंधित रहता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न होने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति में निहित गुणों के साथ कोई संबंध नहीं रहता, इसीलिए वह लोकहित के लिए सभी कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता।
19 20 श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से विरक्ति का वर्णन करके अब भगवान् इक्कीसवें श्लोक में निर्वतीपरायण का अभ्यास करने वाले कर्मयोगी की और बाईसवें श्लोक में कर्मयोग का अभ्यास करने वाले कर्मयोगी की कर्मों से विरक्ति का वर्णन करते हैं।
यह भी पढ़ें :
गीता के अनुसार सच्चा विद्वान किसे कहा गया है?
कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने का रहस्य क्या है?











