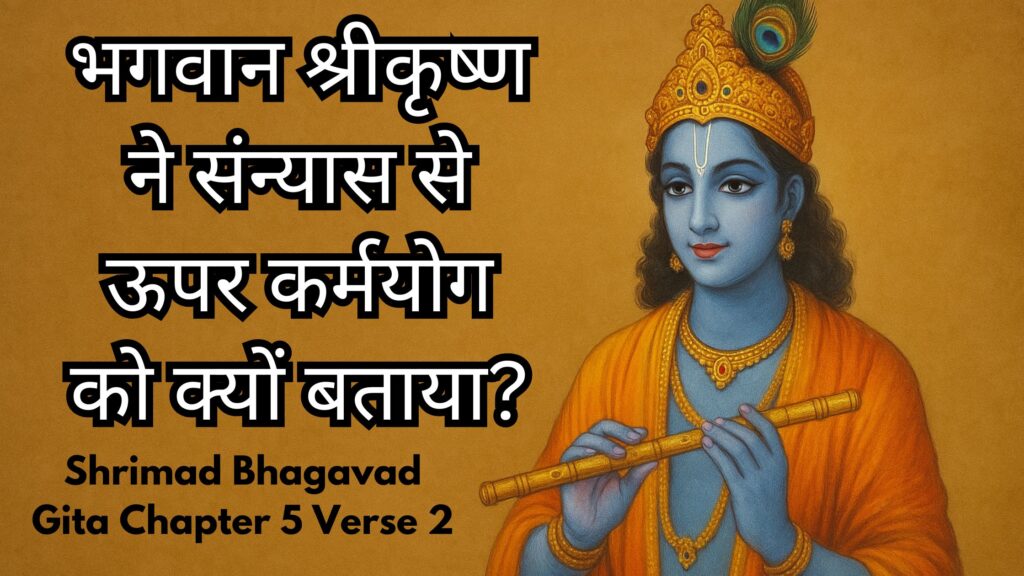
Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 2
श्रीभगवानुवाच ।
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥
भगवान ने कहा – संन्यास (सांख्य योग) और कर्म योग – दोनों ही लाभकारी हैं। लेकिन दोनों में से कर्म योग, कर्म संन्यास (सांख्य योग) से बेहतर है।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 2 Meaning in hindi
क्या संन्यास से श्रेष्ठ है कर्मयोग?
–संन्यासः
यहां ‘संन्यास’ अर्थात् ‘सांख्य योग’, कर्मों का यथावत् त्याग नहीं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् कर्मों के त्याग की नहीं, बल्कि सांख्य योग मार्ग की आलोचना करते हैं, जो कर्म करके ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। सांख्य योग के माध्यम से व्यक्ति हर परिस्थिति में, हर जाति, आश्रम, संप्रदाय आदि में रहते हुए स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण स्वयं कर सकता है।
सांख्ययोग की साधना में विवेक को प्रधानता दी गई है। विवेक और तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और दृष्टि एकमात्र परब्रह्म पर ही रहती है। राग को दूर किए बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना अत्यंत कठिन है। इसीलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए इस उपाय को कष्टकारक बताया है। इसी अध्याय के छठे श्लोक में भगवान ने यह भी कहा है कि कर्मयोग के साधन के बिना निवृत्ति का साधन बनना कठिन है, क्योंकि कर्मयोग ही संसार से राग को दूर करने का एकमात्र सुगम उपाय है।
कर्मयोग क्या है और इसका महत्व क्यों है?
–कर्मयोगश्च
कर्म करने की इच्छा अनादि काल से मनुष्य में विद्यमान है, जिसे दूर करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु उन कर्मों को किस भावना और उद्देश्य से करना है, जिससे कर्म करने की इच्छा पूर्णतः दूर हो जाए, इस कला को ‘कर्मयोग’ कहते हैं। कर्मयोग में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि कर्म छोटा है या बड़ा। जो भी कर्म हमारे सामने आए, उसे निःस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए करना होता है। कर्मों से विरक्त होने के लिए आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाएं। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ पाने की इच्छा न रखना। जब तक अपने लिए कुछ पाने की इच्छा है, तब तक कर्मों से संबंध बना रहता है।
सांख्य योग और कर्मयोग में से कौन है अधिक लाभदायक?
–निःश्रेयसकरावुभौ
अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में से कौन सा निश्चित रूप से लाभदायक है? उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन! ये दोनों साधन निश्चित रूप से लाभदायक हैं। क्योंकि दोनों के माध्यम से समान समता की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय के चौथे और पाँचवें श्लोक में भगवान ने भी इसी बात की पुष्टि की है। तेरहवें अध्याय के चौबीसवें श्लोक में भगवान ने यह भी कहा है कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों के माध्यम से परब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है, अतः ये दोनों परब्रह्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं।
कर्मसंन्यास और सांख्ययोग में क्या है अंतर?
–तयोस्तु कर्मसंन्यासात
एक ही सांख्य योग के दो भेद हैं—एक तो चौथे अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में वर्णित सांख्य योग, जिसमें कर्म का उसके स्वरूप से त्याग है, और दूसरा दूसरे अध्याय के ग्यारहवें से तीसवें श्लोक तक वर्णित सांख्य योग, जिसमें कर्म का उसके स्वरूप से त्याग नहीं है। यहाँ “कर्मसंन्यासात” पद दोनों प्रकार के सांख्ययोग का वाचक है।
भगवान श्रीकृष्ण ने संन्यास से ऊपर कर्मयोग को क्यों बताया?
–कर्मयोगो विशिष्यते
अगले तीसरे श्लोक में भगवान ने इन श्लोकों की परिभाषा करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्यसंन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर छठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग के बिना सांख्ययोग का साधन बनना कठिन है और केवल कर्मयोगी ही शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि सांख्ययोग में कर्मयोग की आवश्यकता है, किन्तु कर्मयोग में सांख्ययोग की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दोनों साधन लाभदायक होते हुए भी भगवान कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं।
अब भगवान अगले श्लोक में कर्म योग को श्रेष्ठ बताने का कारण बताते हैं।
यह भी पढ़ें :











