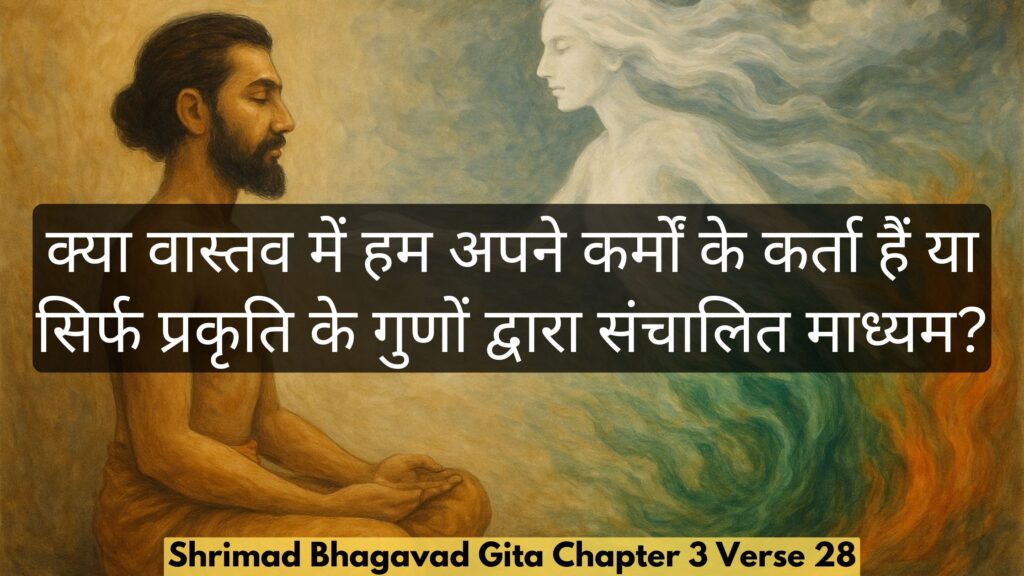
Bhagavad gita Chapter 3 Verse 28
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो: |
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते || 28 ||
अर्थात भगवान कहते हैं, हे महापुरुष! जो महापुरुष गुणों के विभाग को तथा कर्म के विभाग को उनके सार से जानता है, वह यह मानता है कि समस्त गुण गुणों में ही कार्य कर रहे हैं, वह उनमें आसक्त नहीं होता।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 28 Meaning in hindi
क्या हम सच में अपनी सोच और कर्मों के मालिक हैं?
–तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो:
सत्व, रज और तम—ये तीन गुण प्रकृति में निहित हैं। चूँकि ये तीनों गुण इन्हीं तीन गुणों के कार्य हैं, अतः सम्पूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। अतः शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सभी गुण हैं। इसे ‘गुण विभाग’ कहते हैं। इसके (शरीर आदि) माध्यम से होने वाली क्रिया को ‘कर्म विभाग’ कहते हैं।
गुण और कर्म, अर्थात् वस्तुएँ और क्रियाएँ, निरंतर परिवर्तनशील हैं। वस्तुएँ उत्पत्ति और विनाश के अधीन हैं, और क्रियाएँ आदि और अंत के अधीन हैं। इनका ठीक से अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को सार से जानना कहलाता है। चेतना (रूप) में कभी कोई क्रिया नहीं होती। यह सदैव अनासक्त और अपरिवर्तनशील रहती है, अर्थात् इसका किसी भी प्राकृतिक वस्तु और क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। इनका ठीक से अनुभव करना ही चेतना को सार से जानना कहलाता है।
जब अज्ञानी व्यक्ति इस गुण विभाग और कर्म विभाग के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है, तो वह बंध जाता है। शास्त्रों की दृष्टि से इस बंधन का मुख्य कारण ‘अज्ञान’ है, किन्तु साधक की दृष्टि से ‘रजो’ ही इसका मुख्य कारण है। ‘अज्ञान’ से ही राग उत्पन्न होता है। जब बुद्धि जागृत होती है, तो राग लुप्त हो जाता है। यह बुद्धि मनुष्यों के लिए अद्वितीय है। आवश्यकता केवल इस बुद्धि को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को (बुद्धि जागृत करके) राग को विशेष रूप से दूर करना चाहिए।
तत्त्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक यदि गुण (पदार्थ) और कर्म (क्रिया) के साथ अपना संबंध स्वीकार न भी करे, तो भी वह तत्त्व से गुण विभाग और कर्म विभाग को जान लेता है। चाहे वह तत्त्व से गुण विभाग और कर्म विभाग को जाने, अथवा तत्त्व से स्वयं को (चेतन रूप को) जाने, दोनों का परिणाम एक ही होगा।
यह भी पढ़ें : निर्मम निरहंकारी और नि:स्पृह व्यक्ति ही क्यों पाता है शांति?
‘अहम्’ से परे अपने स्वरूप (चेतना) को कैसे जाना जा सकता है?
गहरी नींद में, यद्यपि बुद्धि अज्ञान में लीन रहती है, फिर भी जागने पर व्यक्ति कहता है कि ‘मैं’ बहुत सुख से सोया। इस प्रकार, जागने पर सभी को ‘मैं हूँ’ का अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि निद्रा काल में भी व्यक्ति की अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो, ‘मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था’— तो ऐसी स्मृति या ज्ञान का अस्तित्व ही न होता। स्मृति अनुभवजन्य होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में अपनी शक्ति का निरंतर अनुभव करता है। किसी भी अवस्था में उसे अपनी अनुपस्थिति (‘मैं नहीं हूँ’) का अनुभव नहीं होता। जिन्होंने कल्पित ‘अहं’ (मैं हूँ) से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप (है) का साक्षात्कार कर लिया है, उन्हें ‘तत्त्वविद’ कहते हैं।
अपरिवर्तनशील परमात्मा के साथ हमारा एक स्व-निर्मित शाश्वत संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वास्तव में है ही नहीं, वह केवल कल्पित है। यदि हम विचार द्वारा प्रकृति के साथ कल्पित संबंध को हटा दें, तो उसे ‘ज्ञान योग’ कहते हैं, और यदि हम दूसरों के लिए कर्म करके उसी संबंध को हटा दें, तो उसे ‘कर्म योग’ कहते हैं। जैसे ही हम स्वयं को प्रकृति से पृथक करते हैं, ‘योग’ (परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध का अनुभव) घटित होता है, अन्यथा केवल ‘ज्ञान’ और ‘कर्म’ ही घटित होते हैं। अतः स्वयं को प्रकृति से पृथक करके हम परमात्मा के साथ अपना शाश्वत संबंध स्थापित करते हैं। जो पहचानता है, वही ‘तत्त्वविद’ है।
क्या हम कर्ता हैं या प्रकृति का माध्यम?
–गुणा गुणेषु वर्तन्त
प्रकृतिजन्य गुणों की उत्पत्ति के कारण शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि भी ‘गुण’ कहलाते हैं और इन्हीं से समस्त कर्म होते हैं। विवेक के अभाव में अज्ञानी मनुष्य अपने को इन गुणों से संबंधित मानता है और इनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का स्वयं को कर्ता मानता है। किन्तु जब ‘एक’ (सामान्य ज्योति-चेतना) में अपनी आत्म-प्रतिष्ठित स्थिति का अनुभव करता है, तब ‘मैं कर्ता हूँ’ यह भाव उत्पन्न नहीं हो पाता।
रेलगाड़ी का इंजन चलता है, अर्थात् वह क्रिया करता है, किन्तु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के संयोग से आती है। वस्तुतः खींचने की शक्ति इंजन की ही होती है, किन्तु वह अपने गंतव्य तक तभी पहुँचती है जब उसे चालक द्वारा चलाया जाता है। चूँकि इंजन में इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि नहीं होती, इसलिए उसे इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि से युक्त चालक (मानव) की आवश्यकता होती है। किन्तु मनुष्य के पास शरीर रूपी इंजन भी है और संचालन के लिए इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि भी हैं। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि – ये चारों एक सामान्य प्रकाश (चेतना) से शक्ति प्राप्त करके ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश (ज्ञान) बुद्धि को मिलता है, मन बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करता है, इन्द्रियाँ मन का ज्ञान प्राप्त करती हैं, और तब शरीर रूपी इंजन संचालित होता है। बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, शरीर – ये सभी गुण हैं और जो इन्हें प्रकाशित करता है, अर्थात् इन्हें शक्ति प्रदान करता है, वह इन गुणों से असंबद्ध और विरक्त रहता है। अतः वास्तव में सभी गुण गुणों में ही कार्य कर रहे हैं।
श्रेष्ठ पुरुष के कर्मों का ही सभी लोग अनुसरण करते हैं। इसीलिए भगवान, ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोकसंग्रह कैसे होता है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष ‘सभी गुण गुणों में ही कार्य कर रहे हैं’ ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए।
क्या हमें जीवन की घटनाओं से अनासक्त रहना चाहिए?
-इति मत्वा न सज्जते
दूयहां ‘मत्वा’ पद ‘जानना’ के अर्थ में आया है। प्रकृति (जड़) और पुरुष (चेतन) को जानने वाला महापुरुष स्वभावतः ही जानता है कि प्रकृति भिन्न है। इसीलिए वह प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं होता।
‘मत्वा’ पद का प्रयोग करके भगवान मानो साधकों को आदेश दे रहे हैं कि वे भी प्रकृति के गुणों को भिन्न मानकर उनमें आसक्त न हों।











