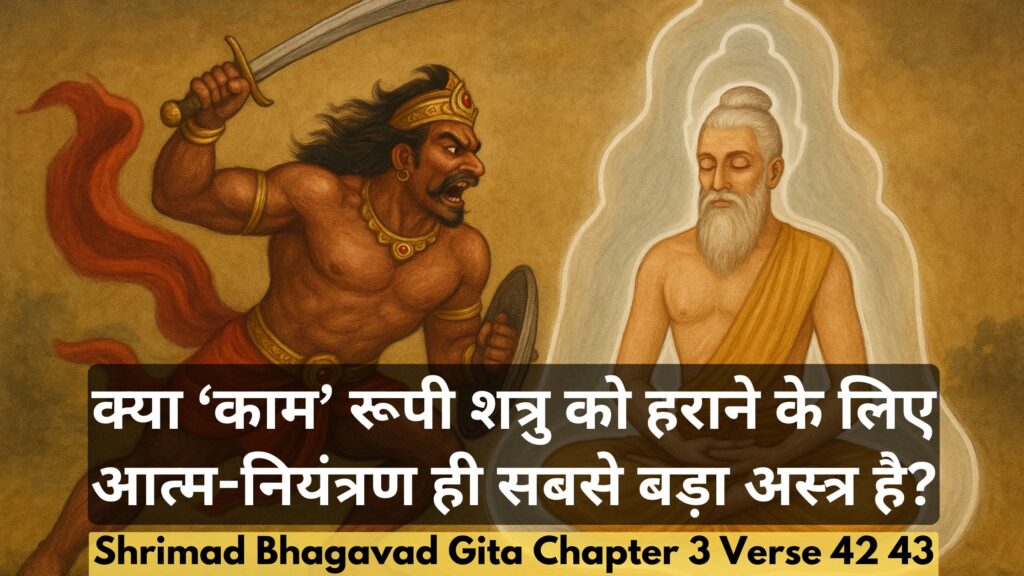
Bhagavad Gita Chapter 3 Verse 42 43
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: परं मन: |
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे: परतस्तु स: || 42 ||
एवं बुद्धे: परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना |
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् || 43 ||
अर्थात भगवान कहते हैं, इन्द्रियाँ (शरीर से ऊपर) सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान, सबसे तेजस्वी, सबसे विस्तृत और सबसे सूक्ष्म कही गई हैं। इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे जो (आत्मा) है, वही (आत्मा) है। इस प्रकार बुद्धि से परे (आत्मा) को जानकर और अपने द्वारा अपने को वश में करके, हे महाबाहो! आप इस कामरूपी दुष्ट शत्रु का वध करें।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 42 43 Meaning in Hindi
क्या हमारी इन्द्रियाँ विषयों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं?
–इन्द्रियाणि पराण्याहु
शरीर या विषय से पर इंद्रिया हैं। तात्पर्य यह है कि विषयों का ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है, परन्तु विषयों से इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। विषयों के बिना भी इंद्रियां रहती हैं, परन्तु विषयों की शक्ति इंद्रियों के बिना प्राप्त नहीं होती। विषयों में इंद्रियों को प्रकाशित करने की शक्ति नहीं होती, इसके विपरीत, इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां वही रहती हैं, परन्तु विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक हैं और विषय व्यापक हैं, अर्थात् विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, परन्तु इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आतीं। विषयों की तुलना में इंद्रियां सूक्ष्म हैं। इसीलिए विषयों की तुलना में इंद्रियां श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशवान, व्यापक और सूक्ष्म हैं।
क्या मन इन्द्रियों से कहीं अधिक शक्तिशाली और व्यापक है?
–इंद्रीयेभ्य: परं मन:
इन्द्रियाँ मन को नहीं जानतीं, परन्तु मन सब इन्द्रियों को जानता है। इन्द्रियों में भी प्रत्येक इन्द्रिय अपने ही विषय को जानती है, अन्य इन्द्रियों के विषयों को नहीं, जैसे कान केवल शब्द को जानता है, परन्तु स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानता, त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, परन्तु शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती, आँखें केवल रूप को जानती हैं, परन्तु शब्द, स्पर्श, रस और गंध को नहीं जानतीं, आँखें केवल रसना का स्वाद जानती हैं, परन्तु शब्द, स्पर्श, रूप और गंध को नहीं जानतीं, और नासिका केवल गंध को जानती है, परन्तु शब्द, स्पर्श, रूप और स्वाद को नहीं जानती, परन्तु मन पाँचों इन्द्रियों और उनके विषयों को जानता है। इसीलिए मन इन्द्रियों से श्रेष्ठ, बलवान, तेजवान, व्यापक और सूक्ष्म है।
यह भी पढ़ें : क्या हमारा स्वभाव ही हमारे कर्मों का निर्धारक है?
क्या बुद्धि ही मन और इन्द्रियों से श्रेष्ठ मार्गदर्शक है?
–मनसस्तु परा बुद्धिर्यो
मन बुद्धि को नहीं जानता, परन्तु बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है? शांत है या अशांत? स्वस्थ है या नहीं? बुद्धि ऐसी बातें जानती है। इन्द्रियाँ ठीक से काम कर रही हैं या नहीं?— बुद्धि यह भी जानती है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि मन और उसके विचारों को जानती है, तथा इन्द्रियों और उनके विषयों को भी जानती है। अतः इन्द्रियों से परे जो मन है, वह मन से (श्रेष्ठ, बलवान, तेजोमय, व्यापक और सूक्ष्म) है, परन्तु बुद्धि से ऊपर है।
क्या अहंकार ही इच्छाओं का असली ठिकाना है?
–य: बुद्धे: परतस्तु स:
बुद्धि का स्वामी अहंकार है, इसीलिए कहा गया है – ‘मेरी बुद्धि’। बुद्धि कारण है और अहंकार कर्ता है। कारण नियन्त्रण के अधीन है, किन्तु कर्ता स्वतंत्र है। उस ‘अहंकार’ में, जो जड़ अंश है, ‘काम’ निवास करता है। जड़ अंश के साथ अपनी तादात्म्यता के कारण, वह काम (चेतना) के रूप में निवास करता हुआ प्रतीत होता है।
एवं बुद्धे: परं बुद्ध्वा
पहले शरीर से परे इन्द्रियाँ, इन्द्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे ‘काम’ को दर्शाया गया। अब उपरोक्त पद में! बुद्धि से परे ‘काम’ को जानने का अभिप्राय यह है कि यह ‘काम’ ‘अह’ में स्थित है। काम अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है। यदि ‘काम’ आकार में होता, तो वह कभी नहीं जाता। नाशवान जड़ के साथ तादात्म्य करने से ही ‘काम’ उत्पन्न होता है। यदि ‘काम’ तादात्म्य में भी स्थित है, तो वह जड़ में ही है, परन्तु रूप में प्रकट होता है। इसलिए बुद्धि से परे स्थित इस ‘काम’ को जानना और नष्ट करना चाहिए।
क्या ‘काम’ रूपी शत्रु को हराने के लिए आत्म-नियंत्रण ही सबसे बड़ा अस्त्र है?
–संस्तभ्यात्मानमात्मना
बुद्धि से परे अहंकार में निवास करने वाली ‘कामना’ को मारने का उपाय है स्वयं के द्वारा स्वयं को वश में करना, अर्थात् केवल अपने शुद्ध स्वरूप से अथवा अपने ईश्वर से, जो कि वास्तव में है, अपना संबंध बनाए रखना।
स्वरूप (स्वयं) सत् परमात्मा का अंश है और शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि संसार के अंश हैं। जब स्वरूप परमात्मा के अपने अंश से विमुख होकर प्रकृति (संसार) के साक्षात् हो जाता है, तब उसमें कामनाएँ उत्पन्न होती हैं। कामनाएँ अभाव से उत्पन्न होती हैं और अभाव संसार के संबंध से उत्पन्न होता है, क्योंकि संसार का रूप अभाव ही है – ‘नासतो विद्यते भावः’। संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं रहता।
ईश्वर से विमुख होकर संसार से अपना सम्बन्ध मानते हुए भी जीव की वास्तविक इच्छा (आवश्यकता या भूख) अपने अंशी ईश्वर को प्राप्त करना ही है। ‘मैं सदा जीवित रहूँ, सब कुछ जानूँ, सदा सुखी रहूँ’ – इस रूप में वह वास्तव में सत्, मन और आनन्दस्वरूप ईश्वर की कामना करता है, किन्तु संसार से अपना सम्बन्ध मानते हुए वह भूलवश संसार के माध्यम से ही इन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है – यही ‘काम’ है। यह ‘काम’ कभी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए इस ‘काम’ का नाश करना ही होगा।
जिसने संसार से अपना सम्बन्ध जोड़ा है, वही इसे तोड़ सकता है। इसीलिए ईश्वर ने स्वयं के माध्यम से संसार से अपना सम्बन्ध तोड़कर ‘काम’ को मारने की आज्ञा दी है।
क्या कामरूपी शत्रु को हराना ही सच्चा आत्म-विजय है?
–जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्
‘महाबाहो’ का अर्थ है – बड़ी और मजबूत भुजाओं वाले, अर्थात् वीर, अर्जुन को ‘महाबाहो’ अर्थात् वीर कहने से भगवान् इस लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं कि तुम इस ‘काम’ रूपी शत्रु का दमन करने में समर्थ हो।
संसार से जुड़े रहते हुए ‘काम’ का नाश करना अत्यंत कठिन है। यह ‘काम’, जो तुम्हारे पतन का कारण बनता है, बड़े-बड़े लोगों के विवेक को भी आच्छादित कर देता है और उन्हें अपने कर्तव्यों से विमुख कर देता है। इसीलिए भगवान् ने इसे दुर्जेय शत्रु कहा है।
‘काम’ को दुर्जेय शत्रु कहने का तात्पर्य है, इससे अधिक सावधान रहना, इसे दुर्जेय शत्रु मानकर निराश न होना।
इच्छाओं के त्याग में अथवा ईश्वर प्राप्ति में सभी स्वतंत्र, समर्थ, योग्य एवं समर्थ हैं। किन्तु इच्छाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र, समर्थ, योग्य एवं समर्थ नहीं है। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। ईश्वर ने अपनी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर दिया है। अतः इच्छाओं का त्याग कठिन नहीं है। सांसारिक वस्तुओं को महत्व देने के कारण ही इच्छाओं का त्याग कठिन प्रतीत होता है।
सुख (अनुकूलता) को दूर करने के लिए ईश्वर समय-समय पर दुःख (प्रतिकूलता) भेजते हैं, जो सुख की इच्छा नहीं रखते, यदि इच्छा करोगे तो दुःख भोगना पड़ेगा। सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखने वाला व्यक्ति दुःख से कभी नहीं बच सकता – यही नियम है, क्योंकि आकस्मिक सुख ही दुःख का कारण है।











