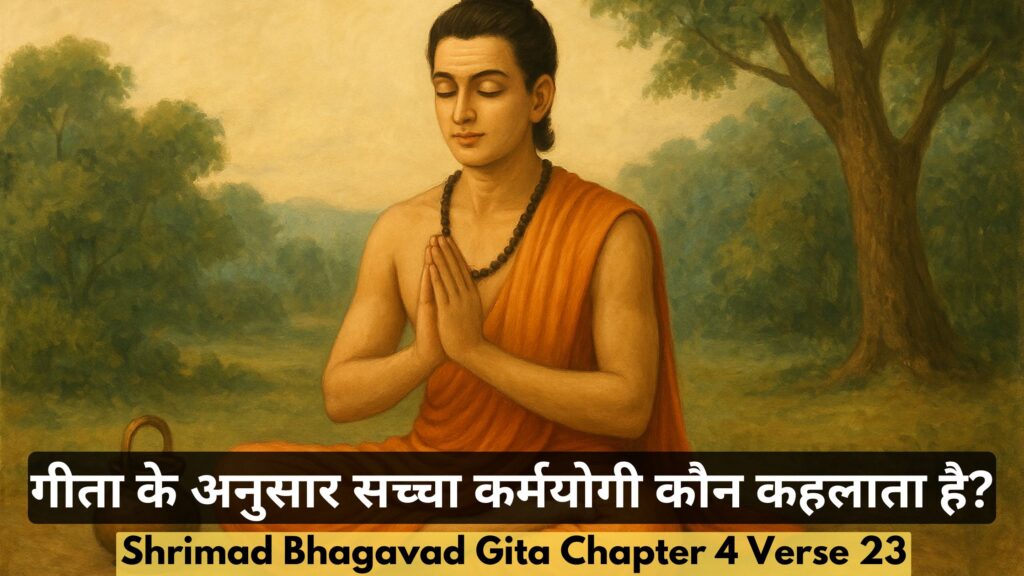
Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 23
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥
अर्थात भगवान कहते हैं, जिसकी आसक्ति पूर्णतया नष्ट हो गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूपज्ञान में स्थित हो गई है, उस मनुष्य के समस्त कर्म, जो केवल त्याग के लिए कर्म करता है, नष्ट हो जाते हैं।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 4 Shloka 23 Meaning in Hindi
गीता के अनुसार कर्मयोगी वस्तुओं और कर्मों से कैसे विरक्त होता है?
–गतसङ्गस्य
वस्तुओं, घटनाओं, परिस्थितियों, व्यक्तियों का संग, उनसे जो आसक्ति होती है, वही वास्तव में बाँधती है या जन्म-मरण देती है। स्वार्थ को त्यागकर केवल लोकहित के लिए, सर्वजनहित के लिए कर्म करने से कर्मयोगी कर्म, वस्तु आदि से विरक्त हो जाता है, अर्थात् उसकी आसक्ति सर्वथा दूर हो जाती है।
कर्मयोगी संसार से प्राप्त वस्तुओं, जैसे शरीर, को अपना और अपने लिए नहीं मानता, बल्कि उन्हें संसार का मानकर संसार की सेवा में अर्पित कर देता है। इससे वस्तुओं और कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और उसका अपना अनासक्त स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है।
कर्मयोगी का अहंकार भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके हृदय में ‘मैं सेवक हूँ’ यह भाव नहीं रहता। वह भाव व्यक्ति को सेवक होने के अभिमान से बाँध देता है। सेवक होने का अभिमान तभी होता है जब सेवा की वस्तु के प्रति अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसकी थी, यदि उसने उसे दे दी, तो सेवा का क्या हुआ? हम उसके ऋण से मुक्त हो गए, इसलिए हम अब सेवक नहीं रहे, केवल सेवा ही शेष रह गई। यह भाव रहता है कि हम सेवा के बदले में कुछ भी नहीं लेना चाहते, जैसे धन, मान, महानता, पद, अधिकार आदि, क्योंकि हम इसके अधिकारी नहीं लगते। इसे स्वीकार करना अन्याय है। लोग मुझे सेवक कहें, तो भी ऐसा भाव नहीं रहता, और यदि कहें, तो हम उससे सहमत भी नहीं होते। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को सब प्रकार से संसार की सेवा में व्यवस्थित करने से हृदय में सुख की अनुभूति होती है। यदि वह सुख भी अनुभव न हो, तो स्वतः ही असंगठितता का अनुभव होता है।
Read Bhagavad Gita All Chapter
गीता के अनुसार सच्ची मुक्ति कैसे प्राप्त होती है?
–मुक्तस्य
जो अपने स्वरूप से सर्वथा भिन्न है, यद्यपि शरीर आदि कर्मों और पदार्थों से उसका कोई संबंध नहीं होता, फिर भी काम, ममता और आसक्ति द्वारा उनसे अपना संबंध मानकर मनुष्य बंध जाता है, अर्थात् पराधीन हो जाता है। जब कर्मयोग के अभ्यास द्वारा यह कल्पित (अवास्तविक) संबंध हट जाता है, तब कर्मयोगी पूर्णतः अनासक्त हो जाता है। अनासक्त होते ही वह पूर्णतः मुक्त अर्थात् स्वतंत्र हो जाता है।
गीता के अनुसार ज्ञानावस्थित चेतना किसे कहते हैं?
–ज्ञानावस्थितचेतसः
जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान निरंतर जागृत रहता है, वही ज्ञानावस्थितचेतसः है। स्वरूप का ज्ञान होते ही स्वरूप की स्थिति वही हो जाती है जो वास्तव में पहले से ही थी।
वास्तव में ज्ञान जगत का ही है। स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ही ज्ञान का रूप है। क्रिया और पदार्थ ही जगत हैं। क्रिया और पदार्थ का विभाग भिन्न है और स्वरूप का विभाग भिन्न है, अर्थात् क्रिया और पदार्थ का रूप से किंचित भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं और रूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाशमान हैं और स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार, जैसे ही स्वरूप सहित क्रिया और पदार्थ का भेद भली-भाँति ज्ञात हो जाता है, क्रिया और पदार्थ के जगत से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्व: सिद्ध, अनासक्त रूप में स्थिति का अनुभव होता है।
गीता के अनुसार सच्चा कर्मयोगी कौन कहलाता है?
–यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते
कर्म में ‘अकर्म’ देखने का एक ही उपाय है— ‘यज्ञार्थ कर्म’ अर्थात् यज्ञ के लिए कर्म करना। केवल दूसरों के हित के लिए निःस्वार्थ भाव से कर्म करना ही ‘यज्ञ’ है। जो केवल यज्ञ के लिए ही समस्त कर्म करता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता, अर्थात् अपने लिए कर्म करता है, वह कर्म से बंध जाता है।
संसार में अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और अनेक प्रकार की वस्तुएँ विद्यमान हैं। किन्तु व्यक्ति जिन कर्मों और वस्तुओं के साथ अपना संबंध आसक्ति, ममता और वासना मानता है, वह उन्हीं कर्मों और वस्तुओं से बंध जाता है। जब व्यक्ति वासना, ममता और आसक्ति का त्याग कर देता है और सभी कर्म केवल दूसरों के हित के लिए करता है तथा प्राप्त वस्तुओं को दूसरों का मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्मयोगी के सभी कर्म (संचित और प्रारब्ध कर्म) विलीन हो जाते हैं, अर्थात् उसे कर्मों के साथ अपनी आत्म-साक्षात्कार/वैराग्य का अनुभव हो जाता है।
इस श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। साधकों की रुचि, श्रद्धा और उपयुक्तता के भेद से साधन भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः अब अगले सात श्लोकों में (चौबीसवें श्लोक से तीसवें श्लोक तक) भगवान विभिन्न प्रकार के साधनों को ‘यज्ञ’ कहते हैं।
यह भी पढ़ें :
क्या सफलता-असफलता में समभाव रखने से जीवन के तनाव से मुक्ति मिल सकती है?
क्या निष्काम कर्मयोगी पाप से मुक्त रहता है? गीता का रहस्य











