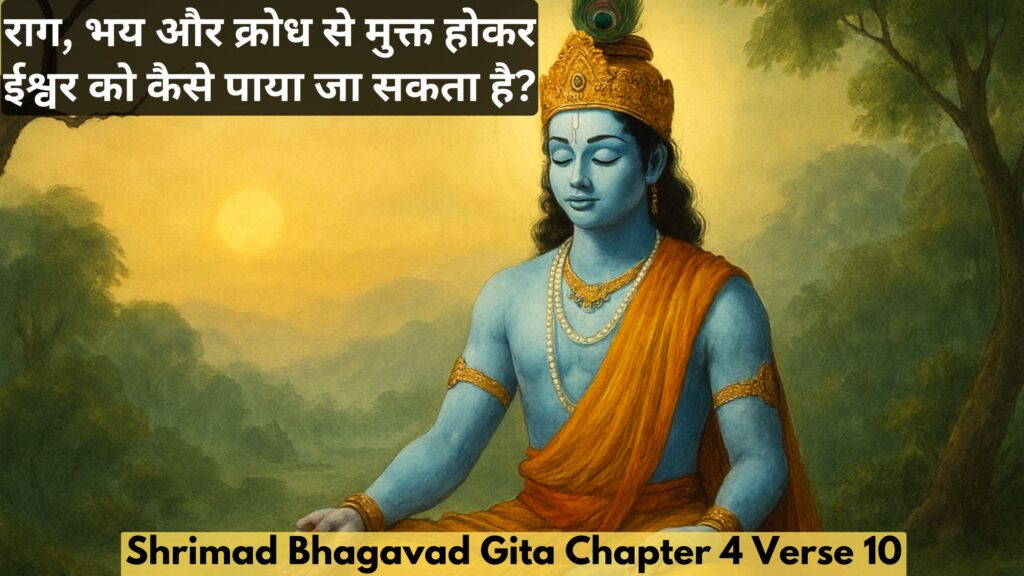
Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 10
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।।१०।।
अर्थात भगवान कहते हैं, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए कितने ही भक्त मेरे भाव (स्वरूप) को प्राप्त हो चुके हैं।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 4 Shloka 10 Meaning in Hindi
राग भय और क्रोध से मुक्त होकर ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है?
–वीतरागभयक्रोधा
जब मनुष्य परमात्म-सत्ता से विमुख हो जाता है, तब नाशवान विषयों के प्रति ‘आसक्ति’ उत्पन्न होती है। मोह से प्राप्त वस्तु के प्रति ‘मोह’ और अप्राप्य के प्रति ‘इच्छा’ उत्पन्न होती है। मोह के विषयों (प्रिय) की प्राप्ति होने पर ‘लोभ’ उत्पन्न होता है, किन्तु जब उनकी प्राप्ति में विघ्न आते हैं, तब ‘क्रोध’ उत्पन्न होता है। यदि विघ्न उत्पन्न करने वाला व्यक्ति स्वयं से अधिक बलवान हो और उस पर अपना अधिकार न जमाया जा सके तथा यह संभावना हो कि वह कालान्तर में अपना ही अहित कर लेगा, तब ‘भय’ उत्पन्न होता है। इस प्रकार नाशवान विषयों के प्रति मोह से भय, क्रोध, लोभ, मोह, काम आदि सभी दोष उत्पन्न होते हैं। मोह के दूर होने पर ये सभी दोष दूर हो जाते हैं। विषयों को अपने और अपने लिए न मानकर, पर और पर के लिए मानने से मोह दूर होता है, क्योंकि वास्तव में वस्तु और कर्म के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।
यह भी पढ़ें : ईश्वर अजन्मा होकर भी क्यों प्रकट होते हैं? जानें योगमाया का रहस्य
भगवान में लीन होकर जीवन कैसे बदलता है? जानें गीता का रहस्य”
–मन्मया
भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानकर, लोगों में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम होने से वे भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और समर्पित होने से वे स्वतः ही ‘मन्मया’ अर्थात् भगवत्-भावित हो जाते हैं।
सांसारिक भोगों में आसक्त लोग भोगों से डरते हैं – ‘कामात्मानः’ (गीता Ch 2/43) और भगवान में आसक्त लोग ‘तन्मय’ हो जाते हैं। वे भगवान में ही लीन रहते हैं। उनके विचार, कर्म आदि में भगवान ही प्रधान रहते हैं। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवान के स्वरूप हो जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई पृथक सत्ता ही न हो।
सच्चा आश्रय किसका लें? गीता के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग
–मामुपाश्रिताः
मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु की शरण लिए बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि ईश्वर का अंश, आत्मा, ईश्वर से विमुख होकर किसी अन्य की शरण ले ले, तो वह शरण स्थायी नहीं रहती, बल्कि चली जाती है। धन आदि नाशवान पदार्थों की शरण विनाशकारी होती है। इतना ही नहीं, सत्कर्मों का, ईश्वर प्राप्ति के साधनों का, तथा धन-संग्रह के त्याग का आश्रय लेने से भी ईश्वर प्राप्ति में विलम्ब होता है। जब तक मनुष्य स्वयं (स्वरूप से) ईश्वर पर आश्रित नहीं हो जाता, तब तक उसकी निर्भरता दूर नहीं होती और वह दुःख भोगता रहता है।
मनुष्य का संसार के पदार्थों में आकर्षण और आश्रय भिन्न-भिन्न होते हैं, जैसे— मनुष्य का आकर्षण स्त्री, पुत्र आदि में होता है और आश्रय वृद्धों में होता है। परंतु ईश्वर में आसक्त मनुष्य का आकर्षण केवल ईश्वर में ही होता है और ईश्वर ही उसके आश्रय हैं, क्योंकि प्रियतम भी ईश्वर ही हैं और महानतम भी ईश्वर ही हैं।
ज्ञानतप क्या है? गीता के अनुसार परम शुद्धि और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग
–बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः
यद्यपि ज्ञानयोग (सांख्यनिष्ठा) से भी व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, किन्तु यहाँ भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्त्व से जानना ही ‘ज्ञान’ कहलाता है। इस ज्ञान से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान का पवित्रोद्धार पक्ष शुद्ध है – ‘पवित्राणां पवित्रां यः’ भगवान का अंश होने के कारण आत्मा में भी स्वतः ही शुद्ध हो जाता है – स्वभावि पवित्रता छे- ‘चेतन अमल सहज सुख रासी’। नाशवान वस्तुओं को महत्त्व देकर, उन्हें अपना मानकर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि नाशवान वस्तुओं में आसक्ति ही एकमात्र अशुद्धता (अशुद्धता) है। जब भगवान के जन्म और कर्म का तत्त्व जानकर नाशवान वस्तुओं का आकर्षण और उनकी आसक्ति पूर्णतः दूर हो जाती है, तब समस्त अशुद्धता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति परम शुद्ध हो जाता है।
चूँकि यह कर्मयोग का प्रसंग है, अतः उपरोक्त पदों में ‘ज्ञान’ शब्द का अर्थ भी कर्मयोग का ज्ञान माना जा सकता है। कर्मयोग का ज्ञान है – शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, भूमि आदि प्राप्त सभी वस्तुएँ संसार की और संसार के लिए हैं, खुद की और खुद के लिए नहीं। क्योंकि आत्मा (स्वरूप) नित्य ह, अतः अनित्य वस्तु उसके साथ कैसे रह सकती है? और उसके काम कैसे आ सकती है? शरीर जैसी वस्तुएँ जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थीं और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगी और इस समय भी उनका प्रतिबिम्ब हमसे अलग हो रहा है। इन प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का अधिकार उन्हें अपना मानने का अधिकार नहीं है। वे वस्तुएँ संसार की हैं। अतः उनका उपयोग संसार की सेवा में ही करना है। यही उनका सदुपयोग है। उन्हें अपनी और अपने लिए समझना वास्तव में बंधन या कलंक है।
इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपना और अपने लिए न समझना ‘ज्ञानतप’ है, जिससे मनुष्य परम शुद्ध हो जाता है। सभी तप ‘ज्ञानतप’ से बढ़कर हैं। इस ज्ञानतप से शरीर के साथ माना जाने वाला संबंध पूर्णतः टूट जाता है। जब तक मनुष्य शरीर के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक अन्य तप उसे उतना शुद्ध नहीं कर पाते, जितना ज्ञानतप द्वारा शरीर से संबंध विच्छेद करने से प्राप्त होने वाली शुद्धि होती है। इस ज्ञानतप से शुद्ध होकर मनुष्य ईश्वर अर्थात् परब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति (शक्ति) को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ईश्वर नित्य निरन्तर रहते हैं, उसी प्रकार वे भी उनमें नित्य निरन्तर रहते हैं, जिस प्रकार ईश्वर अनासक्त और अविचल रहते हैं, उसी प्रकार वे भी अनासक्त और अविचल रहते हैं, जैसे ईश्वर के लिए करने को कुछ नहीं बचता, उसी प्रकार उनके लिए करने को कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार ज्ञानमार्ग से मनुष्य ईश्वरचेतना को प्राप्त करता है।
पाँचों लोकों के भक्तों ने तपस्या द्वारा पवित्र होकर ईश्वर को प्राप्त किया है। अतः साधकों को वर्तमान समय में तपस्या द्वारा पवित्र होकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए सभी स्वतंत्र हैं, कोई परतंत्रता नहीं है। क्योंकि मानव शरीर ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मिला है।
जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया अब कर्मों की दिव्यता क्या होती हैं? इसका विषय अगले श्लोक में आरंभ करते हैं।











