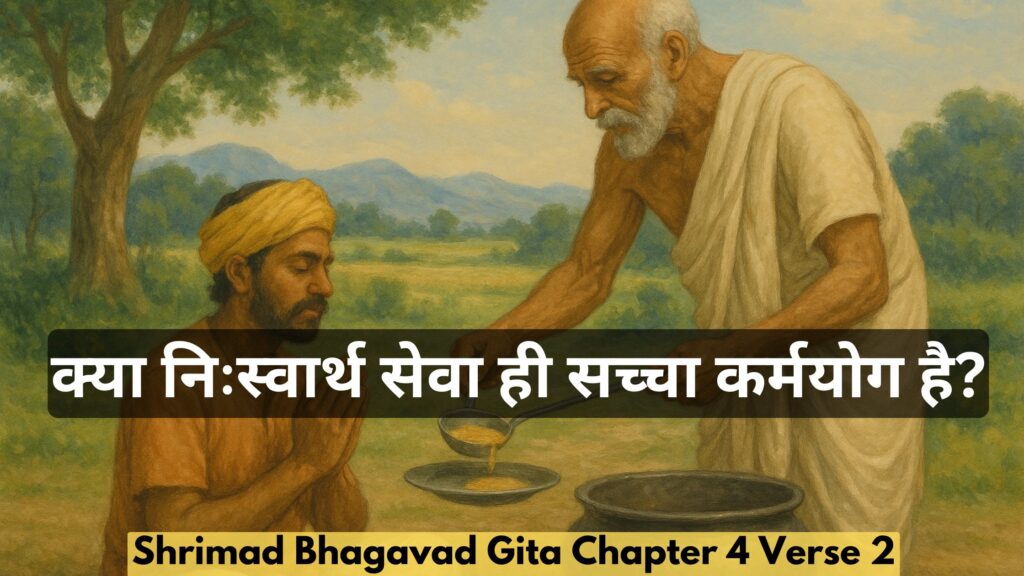
Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 2
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥
अर्थात भगवान कहते हैं, हे परंतप! इस प्रकार राजर्षियों को परम्परा से प्राप्त इस योग का ज्ञान हुआ। किन्तु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मानव लोक में लुप्त हो गया।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 4 Shloka 2 Meaning in Hindi
क्या आज के नेताओं और समाज प्रमुखों को भी राजर्षियों की तरह कर्मयोग का पालन करना चाहिए?
–एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः
सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली-भाँति जानकर स्वयं भी इसका अभ्यास किया और प्रजा से भी करवाया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चलती रही। इन राजाओं (क्षत्रियों) की अपनी विशेष व्यवस्था होती है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह व्यवस्था जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, ग्राम आदि के प्रमुख व्यक्तियों को भी यह व्यवस्था अवश्य जाननी चाहिए।
राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में एकत्रित धन को स्वयं प्रजा के हित में खर्च करते थे, तथा अपने स्वार्थ के लिए तनिक भी व्यय नहीं करते थे। वे अपनी जीविका के लिए पृथक् खेती आदि करते थे। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को स्वतः ही अद्वितीय ज्ञान और भक्ति प्राप्त हो जाती थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े-बड़े ऋषिगण भी ज्ञान प्राप्ति हेतु उन राजाओं के पास जाते थे। श्रीवेदव्यासजी के पुत्र शुकदेवजी भी ज्ञान प्राप्ति हेतु राजर्षि जनक के पास गए थे। छान्दोग्य उपनिषद् के पंचम अध्याय में भी उल्लेख है कि छः ऋषिगण एक साथ महाराजा अश्वपति के पास ब्रह्मविद्या सीखने गए थे।
यह भी पढ़ें : क्या भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ही मनुष्य के पतन का कारण है?
क्या निःस्वार्थ सेवा ही सच्चा कर्मयोग है?
–स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप
ईश्वर नित्य हैं और उनकी प्राप्ति के साधन—कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि—भी नित्य हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा निर्धारित हैं। अतः उनका कभी अभाव नहीं होता। यद्यपि वे कर्म करते हुए दिखाई नहीं देते, फिर भी वे नित्य हैं। इसीलिए यहाँ ‘नष्टः’ शब्द का अर्थ है लुप्त होना, अदृश्य हो जाना, अभाव न होना।
यद्यपि कर्मयोग का अभ्यास लगभग लुप्त हो चुका है, फिर भी इसका स्वयं के लिए कुछ न करने का सिद्धांत सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना कोई भी योग (ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि) निरंतर क्रिया का साधन नहीं बन सकता। कर्म तो मनुष्य को ही करना होता है। हाँ, ज्ञानयोगी अपनी बुद्धि से कर्मों को नाशवान मानकर उनसे अपना संबंध तोड़ लेता है, और भक्तियोगी अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके उनसे अपना संबंध तोड़ लेता है। इसलिए ज्ञानयोगी और भक्तियोगी को कर्मयोग के सिद्धांत को अपनाना ही पड़ता है, भले ही वे कर्मयोग का अभ्यास न करें। तात्पर्य यह है कि यद्यपि वर्तमान में कर्मयोग लगभग लुप्त हो चुका है, फिर भी यह एक सिद्धांत के रूप में विद्यमान है।
मानव शरीर कर्मयोग का पालन करने, अर्थात् निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए मिला है। परन्तु आज मनुष्य दिन-रात अपने सुख-सुविधा, मान-सम्मान आदि की प्राप्ति में लगा रहता है। अत्यधिक स्वार्थ के कारण, वह दूसरों की सेवा की ओर ध्यान ही नहीं देता। इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए मानव शरीर मिला है, उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लोप कहलाता है।
सेवा के माध्यम से मनुष्य पशु-पक्षियों से लेकर मनुष्यों, देवताओं, पितरों, ऋषियों, महात्माओं और ईश्वर तक को वश में कर सकता है। किन्तु सेवा भावना को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के अधीन हो जाता है, जिसका परिणाम नरक और चौरासी नरकों में गिरना होता है। यही कर्मयोग का लुप्त होना है।

📖 Explore the Complete Bhagavad Gita
Read all 18 chapters of the Bhagavad Gita in Hindi with meaning and deep explanations. Discover ancient knowledge that transforms life.
Read NowAlso Read:
क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है?










