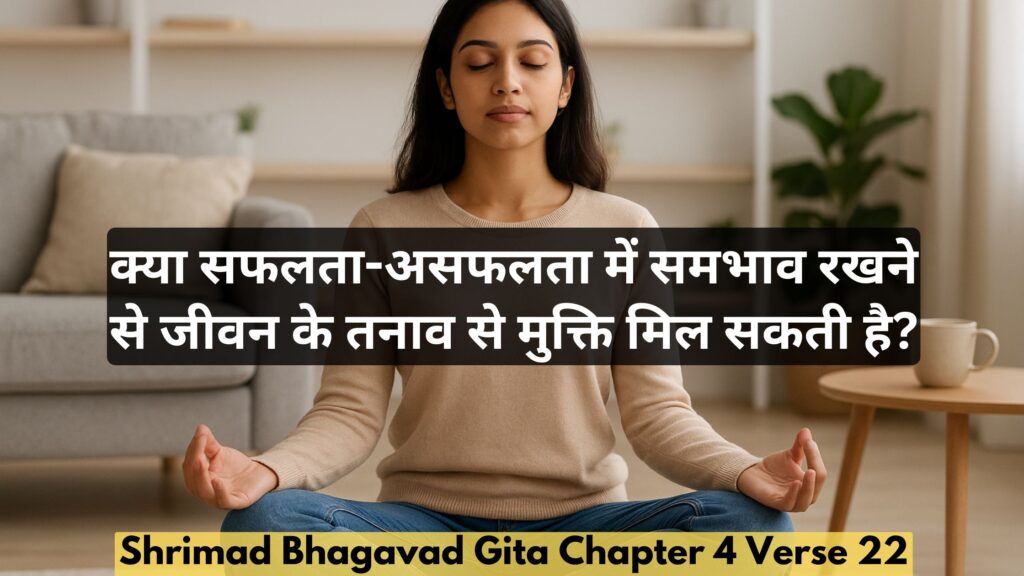
Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 22
यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥
अर्थात भगवान कहते हैं, जो मनुष्य(कर्मयोगी) अपनी इच्छा से जो कुछ प्राप्त होता है, उसी में संतुष्ट रहता है, फल की इच्छा नहीं रखता, ईर्ष्या से रहित है, द्वैत से परे है, सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करता हुआ भी उससे बंधता नहीं है।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 4 Shloka 22 Meaning in Hindi
लाभ-हानि में समभाव रखना क्यों जरूरी है?
–यदृच्छालाभसंतुष्टो
कर्मयोगी अपने सभी कर्तव्यों का पालन संतुलित भाव से, अनासक्त भाव से करता है। वह फल प्राप्ति की इच्छा न रखते हुए कर्म करता है और फलस्वरूप जो भी प्राप्त होता है, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, लाभ हो या हानि, मान हो या अपमान, प्रशंसा हो या निन्दा आदि, उससे उसके हृदय में किसी प्रकार का असंतोष उत्पन्न नहीं होता। जैसे, यदि वह व्यापार कर रहा है, तो व्यापार में लाभ हो या हानि, उसका उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह प्रत्येक स्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका मन फल की इच्छा नहीं करता। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ-हानि का ज्ञान होता है और वह तदनुसार कर्म भी करता है, किन्तु वह फल से सुखी या दुःखी नहीं होता। यदि साधक का हृदय अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित भी हो, तो भी उसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह प्रभाव साधक के हृदय में स्थायी नहीं रहता, शीघ्र ही लुप्त हो जाता है।
Read Shrimad Bhagavad Gita Chapter 1
क्या सच्चा कर्मयोगी ईर्ष्या से मुक्त रहता है?
–विमत्सरः
कर्मयोगी सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। इसीलिए वह किसी भी प्राणी के प्रति किंचितमात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखता।
विमत्सरः पद को अलग देना का तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसके मन में किसी भी जीव के प्रति ज़रा भी ईर्ष्या का भाव न आए। क्योंकि कर्मयोगी के सभी कर्म जीव के हित के लिए ही होते हैं, इसलिए यदि उसमें ज़रा भी ईर्ष्या का भाव है, तो उसके सभी कर्म दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकते।
क्या कर्मयोगी हर द्वन्द्व से मुक्त रह सकता है?
–द्वन्द्वातीतो:
कर्मयोगी लाभ-हानि, मान-अपमान, स्तुति-निंदा, सुविधा-असुविधा, सुख-दुःख आदि द्वैतों से परे होता है, इसलिए उसके मन में राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि द्वैत नहीं होते जो इन द्वन्द्व से उत्पन्न होते हैं।
द्वन्द्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ईश्वर का सगुण स्वरूप श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार स्वरूप श्रेष्ठ है, अद्वैत तत्त्व श्रेष्ठ है या द्वैत तत्त्व श्रेष्ठ है, ईश्वर में मन लगा या नहीं, एकांत मिला या नहीं, शांति मिली या नहीं, सिद्धि मिली या नहीं, आदि। साधक इन सभी द्वन्द्व से मुक्त हो जाता है, केवल इनसे संबंध न रखने से। जैसे तराजू किसी भी दिशा में झुका हो तो उसे सम नहीं कहा जाता, वैसे ही साधक का मन किसी भी दिशा में झुका हो तो उसे द्वन्द्व से परे नहीं कहा जाता।
कर्मयोगी सभी प्रकार के द्वन्द्व से परे होता है, इसलिए वह संसार के बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है।
क्या सफलता-असफलता में समभाव रखने से जीवन के तनाव से मुक्ति मिल सकती है?
–समः सिद्धावसिद्धौ च
किसी भी कर्तव्य का निर्विघ्न पूर्ण होना सिद्धि है और किसी प्रकार की बाधा या रुकावट के कारण उसका पूरा न होना असिद्धि है। कर्मों का फल प्राप्त होना सिद्धि है और उसका न मिलना असिद्धि है। सिद्धि और असिद्धि में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों का अभाव होना सिद्धि और असिद्धि में समभाव कहा गया है।
अपना कुछ न होना, अपने लिए कुछ न चाहना, और अपने लिए कुछ न करना – जब ये तीन बातें उचित अनुभव में आ जाएँगी, तो उपलब्धि और असफलता के बीच पूर्ण संतुलन हो जाएगा।
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समान कैसे रहें?
–कृत्वापि न निबध्यते
यहाँ ‘कृत्वा अपि’ शब्दों का अर्थ यह है कि कर्मयोगी कर्म करने से भी नहीं बंधता, तो फिर कर्म न करने पर बंधने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह दोनों अवस्थाओं में अनासक्त रहता है।
जिस प्रकार केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से बंधता नहीं, उसी प्रकार शास्त्रविधि से कर्म करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से बंधता नहीं।
यदि हम विशेष विचार से देखें, तो समानता स्वयंसिद्ध है। प्रत्येक मनुष्य का यह अनुभव है कि अनुकूल परिस्थितियों में हम जैसे भी रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आने पर भी हम वैसे ही बने रहते हैं। यदि हम एक न होते, तो दो भिन्न (अनुकूल-प्रतिकूल) परिस्थितियों को कैसे जानते? इससे सिद्ध होता है कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, हमारे स्वरूप में नहीं। इसीलिए परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर भी हम स्वरूप में वही रहते हैं। (जैसे हम हैं)। भूल यही है कि हम परिस्थितियों को देखते हैं, स्वरूप को नहीं। अपने समान स्वरूप को न देखने के कारण ही हम आती-जाती परिस्थितियों में सुखी-दुःखी होते हैं।
यह भी पढ़ें :
क्या निष्काम कर्मयोगी पाप से मुक्त रहता है? गीता का रहस्य
क्या आत्मा का वास्तव में कर्म और फल से कोई संबंध है?











