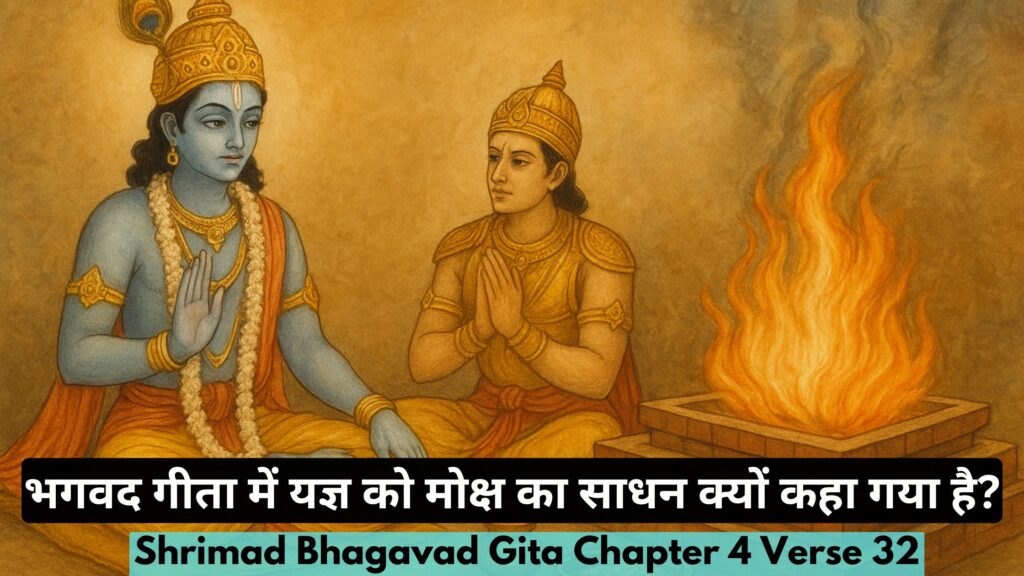
Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 32
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥
अर्थात भगवान कहते हैं, इस प्रकार वेदों में अन्य अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। उन सभी यज्ञों को तू कर्म-संबंधी जान। ऐसा जानकर, यज्ञों को करने से तू (कर्म के बंधन से) मुक्त हो जाएगा।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 4 Shloka 32 Meaning in Hindi
भगवद गीता में यज्ञ को मोक्ष का साधन क्यों कहा गया है?
–एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे
चौबीस से तीस श्लोकों में वर्णित बारह यज्ञों के अतिरिक्त वेदों में अनेक अन्य प्रकार के यज्ञों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। क्योंकि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी भक्ति भी भिन्न-भिन्न होती है और तदनुसार उनके साधन भी भिन्न-भिन्न होते हैं।
वेदों में भी सकाम कर्मों का विस्तार से वर्णन है, किन्तु उन सभी से नाशवान फल ही प्राप्त होते हैं, अविनाशी फल नहीं। अतः वेदों में वर्णित सकाम कर्मों को करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आता है। इस प्रकार वह जन्म-मरण के बंधनों से बंधा रहता है (गीता अ. 9/21)। किन्तु यहाँ उन सकाम कर्मों की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ निष्काम कर्म रूपी उन यज्ञों की चर्चा की गई है, जिनके करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है।
ऐसा नहीं है कि वेद केवल सकाम कर्मों को ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन बताते हैं। वे श्रवण, ध्यान, निदिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि कर्मों को भी परमात्मा प्राप्ति का साधन बताते हैं।
Read Bhagavad Gita All Chapter
भगवद गीता में ‘कर्मजान्विद्धि’ का क्या अर्थ है और अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश क्यों दिया गया?
–कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं
योबिस से तीसवें श्लोक तक जिस बारह यज्ञों का वर्णन किया गया है और वेदों में भी उसी प्रकार जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है, उन सभी यज्ञों के लिए यहाँ ‘तान सर्वान’ शब्द का प्रयोग किया गया है।
कर्मजान्विद्धि शब्दों का तात्पर्य यह है कि सभी यज्ञ कर्मजन्य हैं, अर्थात् कर्मों से उत्पन्न होते हैं। जो कर्म शरीर से किए जाते हैं, जो वचन वाणी से कहे जाते हैं और जो संकल्प मन से किए जाते हैं, वे सभी कर्म कहलाते हैं।
अर्जुन अपना कल्याण तो चाहता है, किन्तु युद्ध के कर्तव्य को पाप मानकर उसका परित्याग करना चाहता है। इसीलिए ‘कर्मजान्विद्धि’ शब्दों के द्वारा भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध-कर्तव्य का त्याग करके तू अपने कल्याण के लिए जो भी साधन करेगा, वह भी कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं, बल्कि कर्मों से पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद करने से होता है। अतः यदि तू आसक्ति रहित होकर युद्ध-कर्तव्य करेगा, तो तेरा भी कल्याण होगा, क्योंकि कर्म मनुष्य को नहीं बाँधते, अपितु केवल आसक्ति (कर्म और उसके फल में) ही बाँधती है। युद्ध तेरा स्वाभाविक कर्तव्य (स्वधर्म) है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सहज है।
गीता में ‘एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे’ का क्या अर्थ है और कर्मों से मुक्ति कैसे संभव है?
–एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे
भावार्थ यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे अनासक्त रहने (कर्मफलों में आसक्ति न रखने) की विधि सीख ली है और अनुभव कर ली है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर पंद्रहवें श्लोक में भगवान ने ‘ज्ञात्वा पद’ शब्दों से यही बात कही। वहाँ भी यही अर्थ है कि ज्ञानी पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते रहे हैं। सोलहवें श्लोक में कर्मों से अनासक्त रहने के इसी सिद्धांत का विस्तार करने के लिए भगवान ने व्रत लिया और कहा, ‘यज्ञत्व मोक्ष- ऽशुभात्वा मोक्ष्यसे- ऽशुभात्’ उन्होंने बताया कि ज्ञान का फल मोक्ष है। अब इस श्लोक में ‘एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे’ कहकर चतुर्थ श्लोक में विषय का समापन किया गया है। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा त्यागकर केवल लोकहितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
संसार में असंख्य कर्म होते हैं, किन्तु व्यक्ति जिन कर्मों के साथ स्वयं को जोड़ता है, वह उनसे बंध जाता है। संसार में कहीं भी कोई भी कर्म (घटना) घटित होती है, और व्यक्ति स्वयं को उससे जोड़ता है – चाहे वह उससे प्रसन्न हो या अप्रसन्न, तो वह उस कर्म से बंध जाता है। जब व्यक्ति का शरीर या संसार में होने वाले किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं रह जाता, तब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है।
यज्ञ का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि यह यज्ञ में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? इसका समाधान भगवान अगले श्लोक में करते हैं।
यह भी पढ़ें :
गीता के अनुसार यज्ञशिष्टामृतभुजः श्लोक का क्या अर्थ है और यज्ञ क्यों आवश्यक है?
गीता में प्राणायाम रूपी यज्ञ क्या है और इससे पाप कैसे नष्ट होते हैं?
गीता के अनुसार द्रव्ययज्ञ तपोयज्ञ योगयज्ञ और ज्ञानयज्ञ क्या हैं?
क्या समाधि में इन्द्रियों और प्राणों की क्रियाएँ पूरी तरह रुक जाती हैं











