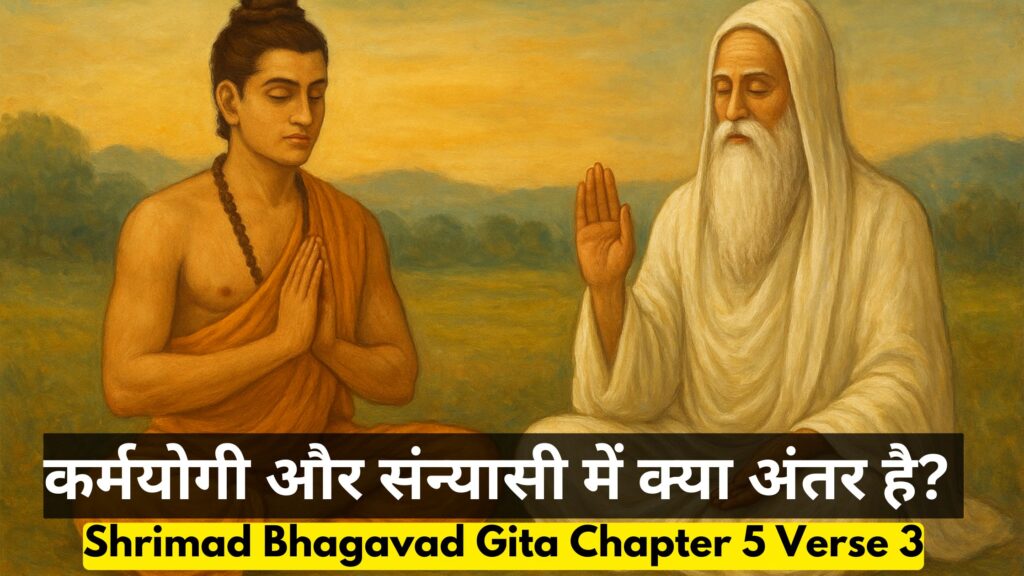
Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 3
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥३॥
भगवान ने कहा हे महाबाहो! जो पुरुष न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी की इच्छा करता है, वह (कर्मयोगी) नित्य तपस्वी मानने योग्य है, क्योंकि जो पुरुष द्वन्द्वों से रहित है, वह सुखपूर्वक संसार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 3 Meaning in hindi
कर्मयोगी और संन्यासी में क्या अंतर है?
–महाबाहो
महाबाहो का अर्थ है, जिसकी भुजाएँ बड़ी और मजबूत हों, अर्थात् वीर हों, और दूसरे, जिसके मित्र और भाई महान पुरुष हों। अर्जुन के मित्र सभी प्राणियों के मित्र भगवान कृष्ण थे, और उनके भाई अजेय शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर थे। अतः यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुममें कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने की शक्ति है। अतः तुम सहजता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो।
कर्मयोगी कौन है और वह द्वेष से कैसे मुक्त रहता है?
–यो न द्वेष्टि
कर्मयोगी वह है जो किसी भी प्राणी, वस्तु, परिस्थिति, सिद्धांत आदि के प्रति द्वेष नहीं रखता। कर्मयोगी का कार्य सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुँचाना है। यदि उसके मन में किसी के प्रति ज़रा भी द्वेष है, तो उसके द्वारा कर्मयोग की साधना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए कर्मयोगी को सबसे पहले उस व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए जिससे वह द्वेष रखता है।
कर्मयोग में कामनाओं का त्याग क्यों आवश्यक है?
–न काङ्क्षति
कर्मयोग में कामनाओं का त्याग ही प्रधान है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, वस्तु, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामनाओं के त्याग और पर-परोपकार में परस्पर संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरों का उपकार करना आवश्यक है। दूसरों का उपकार करने से कामनाओं के त्याग को बल मिलता है।
कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकता। कर्म कर्ता के अधीन है, अर्थात् कर्म का प्रकटीकरण कर्ता के माध्यम से ही होता है। निष्काम कर्म निष्काम कर्ता के माध्यम से ही होता है, जिसे कर्मयोग कहते हैं। अतः ‘कर्मयोग’ कहने पर भी दोनों का अर्थ एक ही है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने पर कर्ता अपने कर्मों के फल से विरक्त रहता है, किन्तु जब कर्ता में सकाम चेतना उत्पन्न होती है, तो वह अपने कर्मों के फल से बंध जाता है। सकाम चेतना तभी नष्ट होती है जब कर्ता अपने लिए कोई कर्म न करके, दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। इसलिए कर्ता की चेतना सदैव निष्काम रहनी चाहिए। कर्ता में जितनी अधिक सकाम चेतना विद्यमान होगी, कर्मयोग का उतना ही अधिक वास्तविक अभ्यास होगा। सब कुछ करने से, और कर्म करने से ही कर्मयोग की प्राप्ति होती है।
यह भी पढ़ें : भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की सलाह क्यों दी?
गीता के अनुसार नित्यसंन्यास क्या है?
–ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी
अर्जुन ने युद्ध करने के स्थान पर भिक्षा मांगकर जीविका चलाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा: ‘गुरुहनात्वा हि महानुभावन श्रेयो भोक्तुं माइक्ष्यमः (गीता अ. 2/5)। अर्थात् गुरु को मारे बिना ही संन्यास लेना श्रेष्ठ है। भगवान् उसी बात का उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं, हे अर्जुन! वह संन्यास गुरु की मृत्यु के भय से किया गया बाह्य त्याग है, किन्तु कर्मयोग का त्याग राग-द्वेष को त्यागकर किया गया स्थायी त्याग है, अर्थात् आन्तरिक एवं सच्चा त्याग है।
संसार से आसक्ति छूट जाने पर उसे संन्यास आश्रम जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब यह निश्चय हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि उसके अपने नहीं हैं, तब वह संसार से आसक्ति मुक्त हो जाता है और उसी सत्य अनुभव का अनुभव करता है। तब, भले ही वह अपने कर्मों में संसार से संबंधित प्रतीत होता हो, परन्तु भीतर से (संसार से आसक्ति के अभाव के कारण) कोई संबंध नहीं रह जाता। यही ‘नित्यसंन्यास’ है। कर्मयोगी प्रत्येक कर्म करते हुए, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, संसार से पूर्णतः विरक्त रहता है, इसलिए उसे नित्यसंन्यास समझना चाहिए।
संन्यास संसार से संबंध का निरोध है, अर्थात् संसार से आसक्ति का अभाव है, और चूँकि कर्मयोगी में संसार से आसक्ति नहीं होती, इसलिए संसार से आसक्ति भी नहीं रहती। इसलिए, कर्मयोगी नित्यसंन्यासी है।
राग-द्वेष से मुक्त होकर साधक कैसे बंधनों से छूट सकता है?
–निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते
साधना के आरंभ में साधक के हृदय में द्वन्द्व बना रहता है। सत्संग, स्वाध्याय, चिन्तन आदि करके वह परमात्मा की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य मानता है, किन्तु उसके अपने मन, इन्द्रियों आदि की रुचि, जो उसे निर्देशित करती है, स्वाभाविक रूप से भोगों के भोग और संचय में ही रहती है। इसीलिए साधक कभी परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो कभी भोगों के भोग और संचय में। उसे जैसी संगति मिलती है, उसके अनुसार उसकी भावनाएँ बदलती रहती हैं। ऐसा होते हुए भी, वह सुखों का शान्तिपूर्वक भोग नहीं कर पाता, क्योंकि सत्संग आदि के अनुष्ठान उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के हृदय में द्वन्द्व (भोगों का भोगना या साधन करना) चलता रहता है। अहंकार इसी द्वैत पर आधारित है। हमें सांसारिक भोगों और संचय में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु केवल परमात्म तत्त्व की प्राप्ति करनी चाहिए – ऐसे दृढ़ निश्चय से द्वैत समाप्त हो जाता है और अहंकार परमात्म तत्त्व में विलीन हो जाता है।
संसार वासनाओं का संसार है, जो उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। वह वासना कभी स्थायी नहीं रहती, किन्तु हम नए जीवों में वासना उत्पन्न करके उसे जारी रखने का प्रयास करते हैं, किन्तु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट नहीं होती, क्योंकि परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का परमात्मा के साथ अटूट संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती या बढ़ती नहीं। संसार में ही ऐसा प्रतीत होता है कि अभिलाषा बढ़ने पर वह घटती है और राग घटने पर बढ़ती है। इसीलिए ‘मैं सदा जीवित रहूँ, मैं सब कुछ जानूँ, मैं सदा सुखी रहूँ’ – इस भाव से, परमात्मा की, जो सच्चिदानन्दस्वरूप है, इच्छा आत्मा में निरन्तर बनी रहती है। जब संसार की वासना हट जाती है और केवल परमात्मा की ही अभिलाषा रह जाती है, तब कोई द्वन्द नहीं रहता।
संसार में भ्रम के केवल दो ही कारण हैं – राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं, वे राग और द्वेष के निवारण के लिए हैं। जब राग और द्वेष दूर हो जाते हैं, तो नित्य प्राप्त होने वाले दिव्य तत्त्व की प्राप्ति स्वयंसिद्ध हो जाती है। इसमें कोई प्रयास नहीं है। क्योंकि दिव्य तत्त्व की प्राप्ति मिथ्यात्व से नहीं, अपितु मिथ्यात्व के त्याग से होती है। मिथ्यात्व की शक्ति राग और द्वेष पर टिकी है। मिथ्या संसार स्वतः ही लुप्त हो रहा है, परन्तु अपने भीतर राग और द्वेष को धारण करने से संसार स्थिर प्रतीत होता है। अतः राग और द्वेष के अभाव से निरन्तर लुप्त हो रहे संसार में यदि मुक्ति न हो तो क्या होगा? इसीलिए राग और द्वेष से मुक्त व्यक्ति सुखपूर्वक सांसारिक जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाले बताया था उसकी व्याख्या अब अगले दो श्लोक में करते हैं।
यह भी पढ़ें :
भगवान श्रीकृष्ण ने संन्यास से ऊपर कर्मयोग को क्यों बताया?
भगवद गीता में संन्यास और कर्मयोग में कौन है श्रेष्ठ?











