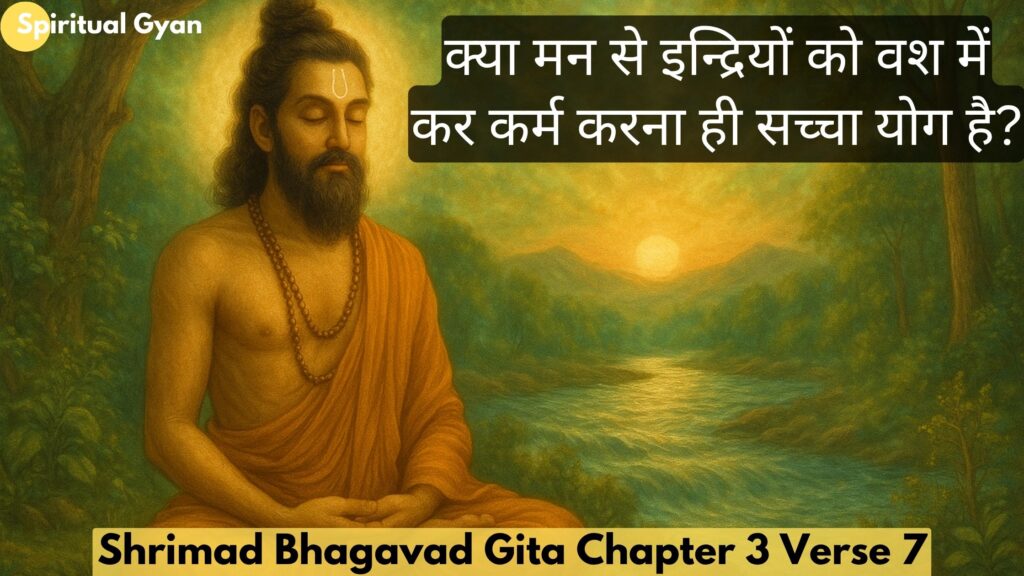
Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 7
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन |
कर्मेन्द्रियै: कर्मयोगमसक्त: स विशिष्यते || 7 ||
अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन! जो पुरुष मन से इन्द्रियों को वश में करता है और आसक्ति से रहित होकर (शुद्ध भाव से) समस्त इन्द्रियों से कर्मयोग का अभ्यास करता है, वह श्रेष्ठ है।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 7 Meaning in hindi
‘तू‘ – यहाँ ‘तू’ पद उस पुरुष को दिया गया है जो निष्काम भाव से, केवल मिथ्या की अपेक्षा से ही नहीं, अपितु सांख्य योगी की अपेक्षा से भी, श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से आसक्ति रहित होकर कर्म करता है।
‘अर्जुन’- ‘अर्जुन’ शब्द का अर्थ है – ‘शुद्ध’। यहाँ ‘अर्जुन’ संबोधन से भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि तू शुद्ध हृदय से युक्त है, अतः तेरे हृदय में कर्तव्य और कर्म के विषय में यह क्या संशय है? अर्थात् यह संशय तुझमें स्थिर नहीं रह सकता।
क्या इन्द्रियों का नियंत्रण ही कर्मयोग की शुरुआत है?
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य
यहाँ मनसा शब्द सम्पूर्ण बुद्धि (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) को दर्शाता है
मन द्वारा इन्द्रियों को वश में करने का अर्थ विवेकशील बुद्धि द्वारा यह अनुभव करना है कि ‘मन और इन्द्रियों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।’ मन द्वारा इन्द्रियों को वश में करने से इन्द्रियों की अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती, अर्थात् उन्हें जहाँ लगाना चाहो, वे वहाँ लग जाती हैं और जहाँ लगाना चाहो, वे वहाँ लग जाती हैं।
इन्द्रियाँ तब वश में हो जाती हैं, जब उनमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। बारहवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में कर्मयोगी ने भी इन्द्रियों को वश में करने की बात कही है- ‘सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत्त्मवान।’ तात्पर्य यह है कि वश में की गई इन्द्रियों से ही कर्मयोग का अभ्यास होता है।
क्या बिना आसक्ति के किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है?
असक्त
आसक्ति दो स्थानों पर होती है- (1) कर्मों में और (2) उनके फलों में। सारे दोष आसक्ति में हैं, कर्मों और उनके फलों में नहीं। आसक्ति! आसक्ति में रहकर योग की प्राप्ति नहीं होती। आसक्ति का त्याग करके ही योग की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनमें आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आसक्ति से विरक्त हुए बिना तथा सावधानी और तत्परता के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों को किए बिना कर्मों से संबंध नहीं तोडा जा सकता।
साधक आसक्ति से तभी विरक्त हो सकता है, जब वह शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि को ‘मेरा’ या ‘मेरे लिए’ न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही समझे। यदि कोई अपने को ही एकमात्र मानकर संसार के हित के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने में तत्परता से लग जाए और अपने लिए न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कोई कर्म करे, तो उसका अपना फल स्वतः ही नष्ट हो जाता है।
कर्मेन्द्रियों द्वारा किये जाने वाले सामान्य कर्म से लेकर चिन्तन और समाधि तक के सभी कर्मों का हमारे स्वरूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु यह आत्मा स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी आसक्त होकर संसार से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है।
कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति से मुक्त होने में है। कर्मों का कोई फल न चाहना अर्थात् उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना आसक्ति से मुक्त होना कहलाता है।
सामान्य व्यक्ति केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कोई कर्म करता है, परंतु साधक केवल आसक्ति का त्याग करने के उद्देश्य से ही कोई कर्म करता है। ऐसे साधक को यहाँ “असक्त” कहा गया है।
कर्म का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह गीता का सिद्धांत नहीं है। गीता के अनुसार कर्म में केवल आसक्ति (अपने दोष के कारण) का त्याग करना चाहिए। कर्मयोग में ‘कर्म’ सदैव दूसरों के हित के लिए होता है और ‘योग’ स्वयं के लिए होता है। अर्जुन कर्म को ‘स्वयं के लिए’ मानता है, इसीलिए उन्हें युद्ध का कर्तव्य भयंकर लगता है। इस संबंध में भगवान स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति भयंकर है, कर्म नहीं।
यह भी पढ़ें : क्या राग-द्वेष से मुक्ति ही सच्चा सुख है?
क्या कर्मयोग का आधार है सेवा भाव और आसक्ति का त्याग?
कर्मेन्द्रियै: कर्मयोगम आरभते
जो कर्म अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, उन्हें कर्मयोग कहते हैं। अपने लिए कर्म करने से कर्म और कर्मफल का सम्बन्ध हो जाता है और अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म और कर्मफल का सम्बन्ध दूसरों से हो जाता है तथा परमात्मा का अपने साथ सम्बन्ध हो जाता है, जो सदा से चला आ रहा है। इस प्रकार देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्यों का निःस्वार्थ भाव से पालन करना ही कर्मयोग का आरम्भ है। कर्मयोगी साधक दो प्रकार के होते हैं-
(1) जिनके हृदय में कर्म करने की गति, आसक्ति और रुचि तो है, किन्तु अपना कल्याण करने की इच्छा ही मुख्य इच्छा है, उनके लिए नये-नये कर्म आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं रहती। उनके लिए तो केवल प्राप्त हुई परिस्थिति का सदुपयोग करने की आवश्यकता रहती है।
(2) जिसके हृदय में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य नहीं है, तथा संसार की सेवा करने, उसे सुख पहुँचाने, समाज को सुधारने में अधिक रुचि है, जिससे उसे यह लगता है कि यदि कुछ कार्य किए जाएँ, तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज सुधर सकता है, आदि। ऐसा साधक यदि नए कर्म आरंभ करे, तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, नए कर्म आरंभ करने का उद्देश्य केवल कर्म करने की आसक्ति को दूर करना है।
गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि वह जिस स्थिति में है उसका सदुपयोग करे, क्योंकि अर्जुन की मुख्य इच्छा स्वयं के कल्याण की थी।
स विशिष्यते
जो मनुष्य अपने स्वार्थ और फल की आसक्ति को त्यागकर केवल प्राणियों के हित के लिए ही कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि उसके समस्त कर्म संसार की ओर प्रवाहित होने से उसमें स्वतः ही वैराग्य आ जाता है।
FAQs
क्या मन से इन्द्रियों को वश में कर कर्म करना ही सच्चा योग है?
हाँ, गीता के अनुसार जो व्यक्ति मन द्वारा इन्द्रियों को वश में करता है और आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है।
क्या कर्मों से नहीं, केवल उनसे जुड़ी आसक्ति से मुक्त होना ज़रूरी है?
बिल्कुल। गीता में कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों की फल-आसक्ति का त्याग करने पर ज़ोर दिया गया है। यही कर्मयोग है।
क्या दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म ही ‘कर्मयोग’ है?
हाँ, जब कर्म अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और प्राणियों के हित के लिए किया जाए, तभी वह कर्मयोग कहलाता है।
क्या निष्काम भाव से कर्म करने वाला ही श्रेष्ठ योगी होता है?
गीता कहती है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा के बिना केवल कर्तव्य भावना से कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है – “स विशिष्यते”।
क्यों कहा गया है कि ‘कर्म दूसरों के लिए और योग अपने लिए होता है’?
क्योंकि कर्म से हम समाज की सेवा करते हैं, जबकि योग से आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ाव होता है।











