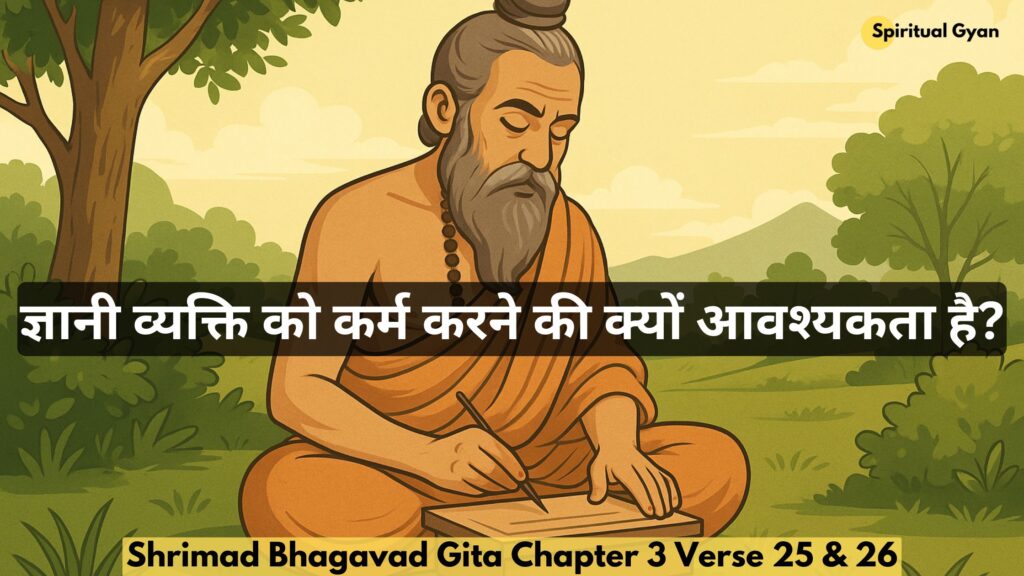
Bhagavad gita Chapter 3 Verse 25 26
सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत |
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् || 25 ||
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् |
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन् || 26 ||
अर्थात भगवान कहते हैं, हे भरतवंशोदभव अर्जुन! जिस प्रकार कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष कर्म करते हैं, उसी प्रकार आसक्ति से रहित विद्वान पुरुष को भी लोगों को एकत्रित करने की इच्छा रखते हुए उसी प्रकार कर्म करने चाहिए। तत्त्वों के ज्ञाता महापुरुष को चाहिए कि वह कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों के मन में भ्रम उत्पन्न न करे, अपितु स्वयं भी सभी कर्मों को भली-भाँति करके उनसे भी करवाए।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 25 26 Meaning in hindi
क्यों भगवान ने ज्ञानी को अज्ञानी की तरह कर्म करने की प्रेरणा दी?
–सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत
जिनकी शास्त्रों, शास्त्र-व्यवस्था और शास्त्रविहित शुभ कर्मों में पूर्ण श्रद्धा है, तथा जिन्हें शास्त्रविहित कर्मों का फल मिलना निश्चित है—उनमें पूर्ण श्रद्धा है, जो न सत्य में ज्ञानी हैं, न दुष्ट, परन्तु कर्म, भोग और विषयों में आसक्त हैं, ऐसे पुरुष अज्ञानी कहे जाते हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी केवल कामना के कारण अज्ञानी (अज्ञानी) कहे जाते हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं, परन्तु सत्य के ज्ञाता नहीं हैं। वे केवल अपने लिए ही कर्म करते हैं। इसीलिए वे अज्ञानी कहे जाते हैं।
ऐसे अज्ञानी लोग अपने कर्मों में कभी प्रमाद, आलस्य आदि नहीं करते, अपितु उन्हें सावधानी और तत्परता के साथ संतुलित भाव से करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यदि कर्म करने में कोई कमी है, तो उसके फल में भी कमी है। भगवान् उनकी इस प्रकार की कर्म-पद्धति को आदर्श मानकर, आसक्ति से सर्वथा मुक्त विद्वानों को भी उसी प्रकार लोकहितार्थ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं।
ज्ञानी व्यक्ति को कर्म करने की क्यों आवश्यकता है?
–कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्
जिन में कामना ममता आ सकती वासना पक्षपात स्वार्थ वगैरा का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर वगैरह पदार्थों के साथ किन-किन मात्रा भी मुंह नहीं रहा ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहां अनासक्त, विद्वान पद आए हैं।
श्रेष्ठ पुरुष (आसक्ति रहित विद्वान) के समस्त कर्म स्वाभाविक रूप से त्याग के लिए, मर्यादा के पालन के लिए होते हैं। जैसे भोगों का भोग करने वाला, कुटुम्ब में आसक्त व्यक्ति और धन का लोभी व्यक्ति, वैसे ही श्रेष्ठ पुरुष प्राणियों के कल्याण में ही रुचि रखता है। उसके हृदय में ‘मैं लोक कल्याण कर रहा हूँ’ ऐसा भाव नहीं रहता, प्रत्युत उससे स्वाभाविक लोक कल्याण स्वतः ही हो जाता है। प्राकृतिक विषयों से सर्वथा पृथक होने के कारण उस महाज्ञानी पुरुष के शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि भी ‘लोकसंग्रह’ की श्रेणी में ‘लोकसंग्रह’ के अंतर्गत आते हैं।
अज्ञानी व्यक्ति फल प्राप्ति की इच्छा से सावधानी और तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करता है, किन्तु ज्ञानी व्यक्ति फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता और न ही उसके प्रति कोई कर्तव्य रखता है। अतः उसके कर्मों की उपेक्षा होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए ईश्वर ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी (शक) व्यक्ति के समान ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं।
जब कोई विद्वान अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है, तो उसके कर्मों का आसक्त मनुष्यों के हृदय पर स्वतः ही प्रभाव पड़ता है, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से देखें या न देखें कि ‘यह महापुरुष अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य कर रहा है।’ यही सिद्धांत है कि व्यक्ति के आसक्त भावों का प्रभाव दूसरों पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। अतः इस शक्तिहीन विद्वान के भावों और कर्मों का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, पशु-पक्षियों आदि पर भी पड़ता है।
यह भी पढ़ें : क्या हमारे कर्म से होती है वर्षा? जानिए गीता के सृष्टि चक्र का रहस्य
क्या समाज की भलाई के लिए ज्ञानी को भी कर्म में लगना पड़ता है?
–न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन्
जिसके हृदय में सहज समता है, जिसकी स्थिति अविचल है, जिसकी सभी इन्द्रियाँ वश में हैं, तथा जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान हैं, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष को न्युक्त: विद्वान् कहते हैं।
श्रेष्ठ व्यक्ति का विशेष उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि अन्य लोग स्वभावतः ही उसका अनुसरण करते हैं। इसीलिए भगवान उपरोक्त श्लोकों के माध्यम से विद्वान व्यक्ति को आज्ञा देते हैं कि वह ऐसा कोई कार्य न करे और ऐसा कुछ न कहे, जिससे अज्ञानी (इच्छावान) मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से पतित हो जाएँ। अज्ञानी मनुष्यों को उनकी वर्तमान स्थिति से विचलित (निराश) करना, उनमें बुद्धिभेद उत्पन्न करना कहलाता है। अतः विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रमधर्म के अनुसार शास्त्रविहित शुभ कर्मों को हित का ध्यान रखते हुए करता रहे, जिससे अन्य मनुष्य भी निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित हों। यही बात समाज और परिवार के प्रमुख व्यक्तियों पर भी लागू होती है। उन्हें भी सावधान रहकर अपने कर्तव्यों का भली-भाँति पालन करना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
‘समाचरण’ और ‘जोषयेत्’ पदो द्वारा भगवान ने विद्वानों के लिए दो आज्ञाएँ दी गई हैं—(1) वह स्वयं शास्त्रविहित कर्तव्यों का सावधानीपूर्वक और उत्तम रीति से पालन करे और (2) कर्मों में आसक्त अज्ञानी मनुष्यों से भी वैसा ही कराए। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना ‘दम्भ’ है, जो पतन की ओर ले जाने वाले आसुरी सम्पदा का लक्षण है।
अतः भगवान् लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपितु लोगों को एकत्र करने के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं।
तत्त्वदर्शी पुरुष को कर्म करने में कोई प्रयोजन न होने पर भी अपने सभी कर्तव्यों का यथायोग्य पालन करते रहना चाहिए, जिससे कर्मों में आसक्त व्यक्तियों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्तर चेतना जागृत हो जाए और वे भी निष्काम कर्म करने लगें। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के निष्काम कर्मों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही करने का प्रयत्न करने लगेंगे।
इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्त व्यक्तियों को आदरपूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का सर्वथा (सभी प्रकार से) त्याग करवाए तथा उन्हें इच्छित कर्म करने का विचार त्यागने के लिए प्रेरित करे।
ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है?? इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में रहते हैं।











