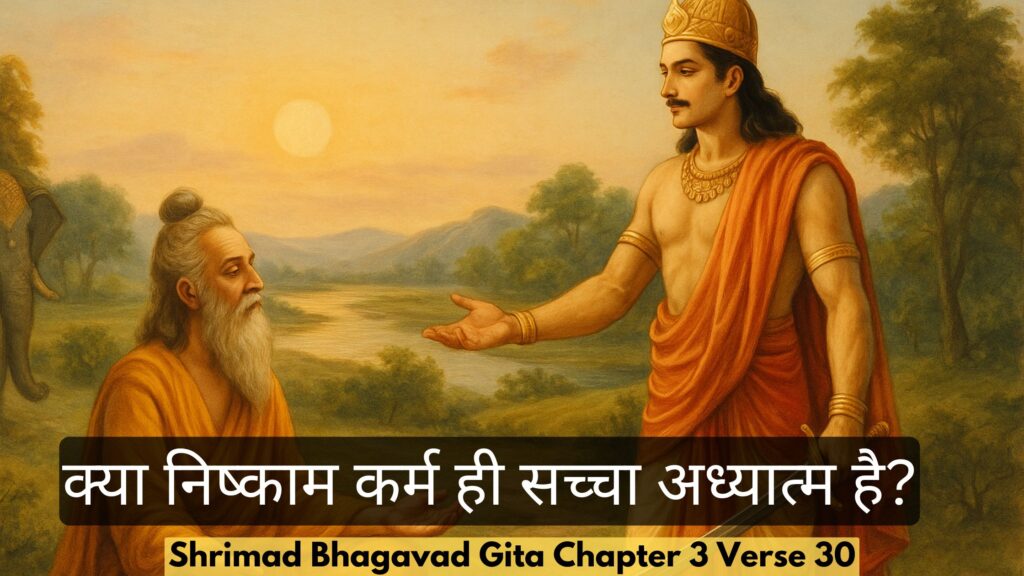
Bhagavad gita Chapter 3 Verse 30
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३०॥
अर्थात भगवान कहते हैं, तुम अपनी विवेकवान बुद्धि से अपने समस्त कर्तव्यों को मुझे अर्पण करके कामना, आसक्ति और मोह से रहित होकर युद्ध रूपी अपने कर्तव्यों का पालन करो।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 30 Meaning in hindi
क्या हर कर्म भगवान को समर्पित करना हमें मुक्त कर सकता है?
–मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा
अनेक साधकों का विचार है कि कर्म बाँधता है और कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता; अतः कर्म करने से मैं तो बँधूँगा ही! अतः कर्म किस प्रकार किया जाए कि कर्म बाँधे नहीं, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए – इसी कारण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्मनिष्ठ (विवेकपूर्ण अंतःकरण वाला) हो जा और अपने समस्त कर्तव्य-कर्मों को मुझे अर्पण कर दे, अर्थात् उनसे अपना कोई सम्बन्ध न समझ, क्योंकि वास्तव में जगत् के समस्त कार्यों में मेरी ही शक्ति कार्यरत है। शरीर, इन्द्रियाँ, जड़ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी ही है। अतः जब तू ऐसा गम्भीर विचार करके अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तब वे कर्म तुझे बाँधेंगे नहीं, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाएँगे।
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि पदार्थ का खुद पर कोई अधिकार नहीं है। यह तो केवल मनुष्य का अनुभव है। ये सभी प्रकृति के हैं और परमात्मा के हैं। अतः शरीर आदि के प्रति भ्रांति को दूर करके इन्हें ईश्वर का मानना (जो कि वास्तव में ये हैं) उन्हें ही ‘अर्पण’ कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देना और विषयों तथा कर्मों के साथ मूर्खतापूर्ण माने गए संबंध को त्यागना ही अर्पण का अर्थ है।
क्या निष्काम कर्म ही सच्चा अध्यात्म है?
–अध्यात्मचेतसा
इस पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कोई भी मार्ग का साधन हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए लौकिक नहीं, वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की (आध्यात्मिक) होती हैं और कामना सदैव अनित्य तत्व (उत्पत्ति विनाशशील वस्तु) की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतरण विवेक विचार युक्त ही रहता है।
किसी भी दार्शनिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि शरीर आदि स्वयं के हैं। वस्तुतः ये वस्तुएँ स्वयं की और स्वयं के लिए नहीं हैं, अपितु केवल अपने उचित उपयोग के लिए दी गई हैं। चूँकि ये स्वयं के नहीं हैं, इसलिए इन पर किसी का अधिकार नहीं है।
संसार तो केवल परमात्मा का है, परन्तु आत्मा परमात्मा की वस्तुओं को ही अपना मानकर भ्रमवश बंधन में पड़ जाती है। अतः विवेक द्वारा इस भूल को दूर करके सभी वस्तुओं और कर्मों को परमात्मा का मान लेना ही उन्हें आध्यात्मिक मन से अर्पण करना कहलाता है।
यह भी पढ़ें : क्या बिना ज़िम्मेदारी निभाए जीना बेकार है? जानिए गीता का नजरिया
क्या सच में समर्पण के बाद भी आसक्ति बची रहती है?
–निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः
सभी कर्मों और वस्तुओं (कर्मसामग्री) को भगवान को अर्पित करने के बाद भी, इच्छा, आसक्ति और दुःख का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरण के लिए— हमने किसी को एक पुस्तक दी है। उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यह आंशिक आसक्ति है, जो पुस्तक अर्पित करने के बाद भी बनी रहती है। इस अंश को त्यागने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तुओं की ‘इच्छा’ न कर, प्राप्त वस्तुओं में ‘आसक्ति’ न कर और नष्ट वस्तुओं का ‘संताप’ न कर। सब कुछ मुझे अर्पित करने की कसौटी यह है कि इच्छा, आसक्ति और दुःख का एक अंश भी शेष न रहे।
जो साधक भगवान को सब कुछ समर्पित करने के बाद भी शरीर आदि के प्रति वासना, आसक्ति और दुःख देखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिनमें वासना देखी जाती है, वे ही वासना से मुक्त होते हैं, जिनमें ममता देखी जाती है, वे ही ममता से मुक्त होते हैं और जिनमें दुःख देखा जाता है, वे ही अहंकार से मुक्त होते हैं। इस प्रकार जो शरीर को ‘मैं’ मानते हैं, वे ही अहंकार से मुक्त होते हैं। अतः मनुष्य को वासना और अहंकार से मुक्त होने का पूरा अधिकार है।











