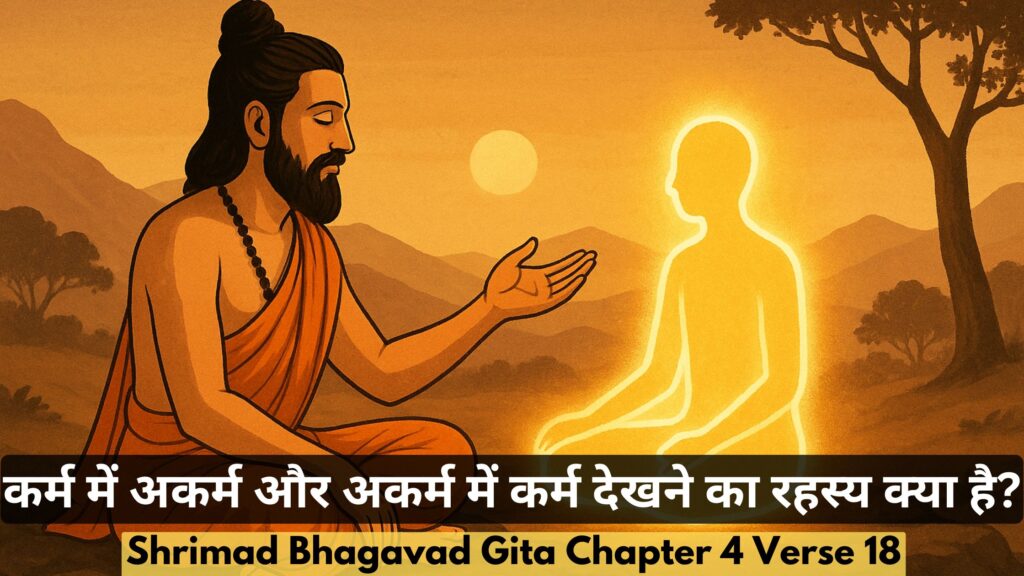
Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 18
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥१८॥
अर्थात भगवान कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो मनुष्य अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्मों का कर्ता है।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 4 Shloka 18 Meaning in Hindi
कर्म में अकर्म देखने का रहस्य क्या है?
–कर्मण्यकर्म यः पश्येत
कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है, कर्म करते हुए या न करते हुए भी उससे अनासक्त रहना, अर्थात् अपने लिए कोई क्रिया या निवृत्ति न करना। मैं कुछ कर्म करता हूँ, इस कर्म का कुछ फल मुझे मिलता है, इस भावना से कर्म करने मात्र से ही मनुष्य कर्म से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, अतः उसके फल का भी आदि और अंत होता है। परन्तु आत्मा स्वयं सनातन रहती है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा असंबद्ध है, फिर भी फल की इच्छा के कारण वह उनसे बंधी रहती है। इसीलिए चौदहवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म मुझे नहीं बांधता, क्योंकि कर्म के फल की मेरी कोई इच्छा नहीं है। फल की इच्छा बांधने वाली है।
जीवात्मा का जन्म कर्म के अनुबंध के कारण होता है। उदाहरण के लिए, जिस परिवार में जन्म होता है, उस परिवार के सदस्यों के साथ उसका ऋण संबंध होता है, अर्थात् किसी का ऋण चुकाना होता है और किसी से ऋण वसूल करना होता है क्योंकि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। ऋण का यह लेन-देन अनेक जन्मों से चलता आ रहा है। इसे रोके बिना जन्म-मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसे रोकने का उपाय है कि शुरू से ही लेना बंद कर दिया जाए, अर्थात् अपना अधिकार त्याग दिया जाए और जिनका अपने ऊपर अधिकार है, उनकी सेवा शुरू कर दी जाए। इस प्रकार यदि नया ऋण न लिया जाए और पुराना ऋण चुका दिया जाए (दूसरों के लिए कर्म करके), तो ऋण संबंध (ऋण लेने और सेवा करने का लेन-देन) समाप्त हो जाएगा, अर्थात् जन्म-मरण रुक जाएगा।
अपने लिए कुछ न करने या न चाहने से स्वतः ही वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इन्द्रियाँ (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण) और साधन (कर्म करने में उपयोगी पदार्थ) संसार के हैं और संसार की सेवा में ही लगाने के लिए दिए गए हैं, अपने लिए नहीं, इसलिए समस्त कर्तव्य (सेवा, भजन, जप, ध्यान, यहाँ तक कि समाधि भी) केवल संसार के हित के लिए करने से कर्म का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक स्वयं अनासक्त एवं विरक्त रहता है। इसे ही कर्म में अकर्म देखना कहते हैं।
अकर्म में कर्म देखने का अर्थ क्या है?
–अकर्मणि च कर्म यः
अकर्म में कर्म देखने का अर्थ है कर्म करते या न करते हुए भी उससे विरक्त रहना। सार यह है कि कर्म करते या न करते हुए भी निरंतर विरक्त रहना।
जब तक साधक प्रकृति के साथ अपने संबंध में विश्वास रखता है, तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति और कर्म न करने से अपनी आध्यात्मिक उन्नति मानता है, किन्तु वास्तव में क्रिया और निवृत्ति दोनों ही क्रियाएँ हैं, क्योंकि दोनों का प्रकृति के साथ संबंध है। जैसे घूमना-फिरना, खाना-पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएँ हैं, वैसे ही एकांत में बैठना, चिंतन-मनन करना आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएँ हैं और समाधि लगाने का कारण शरीर की क्रियाएँ हैं। अतः अनासक्त रहकर लोक-कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसे ही उसी कर्म में कर्म कहते हैं।
यह भी पढ़ें : क्या भगवान हर युग में अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए?
कर्म के तत्त्व को जानने वाला बुद्धिमान कौन है?
–स बुद्धिमान्मनुष्येषु
जो फल में अकर्म और कर्म में कर्म को देखता है, अर्थात् नित्य अनासक्त रहता है, वही वास्तव में कर्म के तत्त्व को जानता है। जब तक वह अनासक्त नहीं हो जाता, अर्थात् कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए नहीं मानता, तब तक उसने कर्म के तत्त्व को नहीं समझा है।
परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा के साथ अपनी अनस्तित्वता का अनुभव करना पड़ता है, और जगत् को जानने के लिए जगत् (कर्म और पदार्थ) से अपनी पूर्ण भिन्नता का अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि वास्तव में हम (स्वरूप में) परमात्मा से पृथक् और जगत् से भिन्न हैं। अतः कर्मों से अनासक्त होकर, अर्थात् विरक्त होकर ही हम कर्म के तत्त्व को जान सकते हैं। कर्मों का आदि और अंत होता है, और मैं (स्वयं आत्मा) नित्य हूँ; अतः मैं (रूप में) कर्मों (अनस्तित्व) से पृथक् हूँ – इस सत्य का अनुभव करना ही ‘जानना’ कहलाता है। सत्य के मूल में बैठे बिना ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है?
कर्मयोगी को योगी क्यों कहा जाता है?
–स युक्तः
कर्मयोगी सफलता और असफलता में सम रहता है।
कर्म का फल मिले या न मिले, उसमें कभी कोई भेद नहीं होता, क्योंकि उसने फल की इच्छा का पूर्णतः त्याग कर दिया है। समता को योग कहते हैं। वह समता में निरन्तर स्थित रहता है, इसीलिए वह योगी है।
प्राणीमात्र का ही परमात्मा के साथ स्वतःसिद्ध शाश्वत योग है। परन्तु मनुष्य ने संसार के साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है, इसलिए वह शाश्वत योग को भूल गया है। तात्पर्य यह है कि जड़ के साथ अपना सम्बन्ध मानना परमात्मा के साथ अपने शाश्वत सम्बन्ध को भूल जाना है। कर्मयोगी फल की इच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य करता है, जिससे जड़ के साथ उसका सम्बन्ध टूट जाता है और उसे परमात्मा के साथ स्वतःसिद्ध शाश्वत योग का बोध हो जाता है। इसीलिए उसे योगी कहा जाता है।
कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने का रहस्य क्या है?
–कृत्स्नकर्मकृत्
जब तक कुछ पाने को शेष है, तब तक हमेशा ‘करने को’ शेष है, अर्थात् जब तक कुछ पाने की इच्छा है, तब तक करने की इच्छा नहीं जाएगी।
नाशवान कर्मों से प्राप्त होने वाला फल भी नाशवान है। जब तक नाशवान फल की इच्छा रहती है, तब तक कर्म करना बंद नहीं होता। किन्तु जब मनुष्य नाशवान कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति का अविनाशी फल प्राप्त कर लेता है, तब कर्म करना सदा के लिए बंद हो जाता है और कर्मयोगी के करने या न करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा कर्मयोगी समस्त कर्मों का कर्ता होता है, अर्थात् उसके करने को कुछ शेष नहीं रहता, वह स्वयं कृतकृत्य बन जाता है।
जब कर्मयोगी के पास करने, जानने या पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता, तो वह संसार के अशुभ बंधनों से मुक्त हो जाता है।
अब भगवान अगले दो श्लोक में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्मों को तत्व से जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं।
यह भी पढ़ें :











