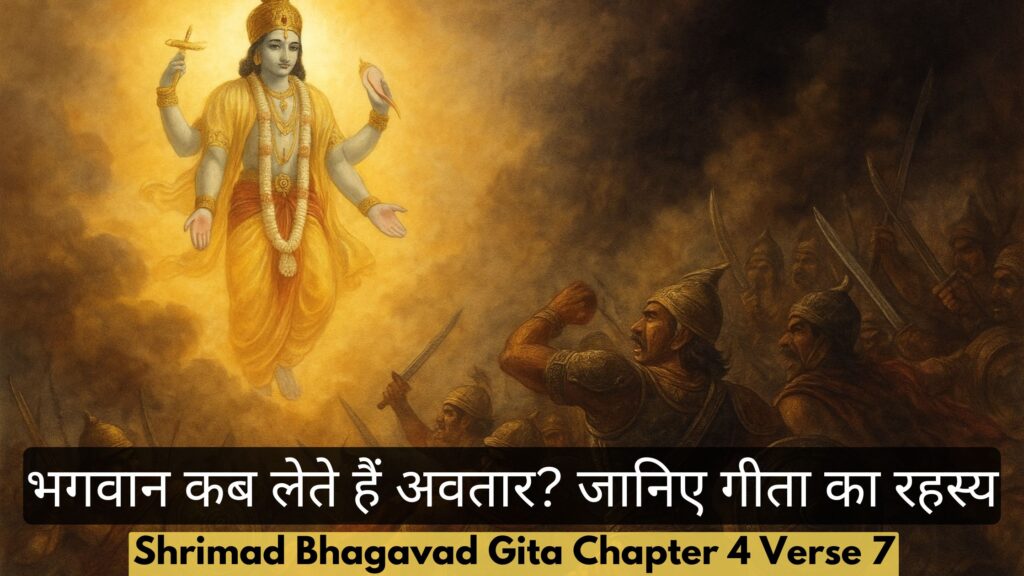
Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 7
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७॥
अर्थात भगवान कहते हैं, हे भरतपुत्र अर्जुन! जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 4 Shloka 7 Meaning in Hindi
भगवान कब लेते हैं अवतार? जानिए गीता का रहस्य
–यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है—ईश्वर-प्रेमी, धार्मिक, सदाचारी, भोले और दुर्बल लोगों पर नास्तिकों, पापियों, दुराचारियों और शक्तिशाली लोगों का अत्याचार बढ़ना, लोगों में सदाचार और सदाचार का अत्यधिक ह्रास और दुराचार तथा दुराचार में अत्यधिक वृद्धि।
यदा यदा का अर्थ है कि जब भी आवश्यकता होती है, भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी, वे आवश्यकता और अवसर के अनुसार जितनी बार अवतार लेने की आवश्यकता हो उतनी बार ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, समुद्र मंथन के समय, भगवान ने अजित रूप में समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप में मंदराचल को धारण किया और सहस्त्रबाहु रूप में ऊपर से मंदराचल को थामे रखा। फिर देवताओं को अमृत बाँटने के लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए।
अधर्म की वृद्धि और धर्म के पतन का मुख्य कारण नाशवान वस्तुओं के प्रति आकर्षण है। जैसे माता और पिता से शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि का निर्माण होता है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य रूपी जगत् प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, एक क्षण के लिए भी एक समान नहीं रहता और परमात्मा तथा उसका अंश रूपी जीवात्मा, दोनों ही सभी स्थानों, कालों आदि में नित्य एकरस रहते हैं, तथा इसमें कभी किंचितमात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीवात्मा अनित्य, नाशवान प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से सुख पाने की इच्छा करने लगती है और उनकी प्राप्ति में ही सुख मानने लगती है, तब उसका पतन होने लगता है। जैसे-जैसे लोगों की सांसारिक सुखों और संग्रह में आसक्ति बढ़ती है, वैसे-वैसे समाज में अधर्म बढ़ता है और जैसे-जैसे अधर्म बढ़ता है, वैसे-वैसे समाज में पाप, कलह, विद्रोह आदि भी बढ़ते हैं।
यदि हम सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग को देखें, तो इनमें भी धर्म का क्रमिक ह्रास होता है। सत्ययुग में धर्म के चारों चरण शेष रहते हैं, त्रेतायुग में धर्म के तीन चरण शेष रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के दो चरण शेष रहते हैं और कलियुग में धर्म का केवल एक चरण शेष रहता है। जब धर्म का ह्रास युग की सीमा से अधिक हो जाता है, तब भगवान धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं।
यह भी पढ़ें : क्या हम कर्ता हैं या प्रकृति का माध्यम?
क्या भगवान अभी अवतार क्यों नहीं लेते? जानिए गीता का उत्तर
–तदात्मानं सृजाम्यहम्
जब भ्रष्टाचार और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। अतः भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना है।
जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तो लोगों के कर्म अधर्म में बदल जाते हैं। अधर्म में सक्रिय रहने से स्वाभाविक रूप से पतन होता है। भगवान सभी जीवों के परम मित्र हैं। इसीलिए वे लोगों को पतन से बचाने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं।
कर्मों में तृप्ति की भावना का उदय धर्म की हानि है और अपने कर्तव्य से विमुख होकर निषिद्ध कर्म करना अधर्म का उदय है! ‘काम’ अर्थात् इच्छा ही समस्त अधर्म, पाप, अन्याय आदि का कारण है (गीता अ. 3/37)। अतः भगवान इस ‘काम’ का नाश करने और अकामना के भाव का विस्तार करने के लिए अवतार लेते हैं।
यहाँ एक शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत अधिक हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी भगवान के अवतार लेने का समय नहीं आया है। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह कलियुग है, जो त्रेता युग से बीत चुका है, किन्तु अभी भी धर्मात्मा पुरुष जीवित हैं, उनका विनाश कोई नहीं कर रहा। एक और बात अतिरिक्त है। जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं या यहाँ से विशेष साधक प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। कभी-कभी परमात्मा को प्राप्त महान कारक भी जगत का उद्धार करने आते हैं। जिस देश में साधक और संत रहते हैं, वहाँ अधर्म नहीं बढ़ता और धर्म की स्थापना होती है।
जब लोग साधकों और संतों पर भी विश्वास नहीं करते, उल्टे उनका विनाश करने लगते हैं, और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम लोग रह जाते हैं तथा इस युग में धर्म कैसा होना चाहिए, इसकी अपेक्षा में भी धर्म बहुत क्षीण हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं।
इस लोक में अपने अवतार का वर्णन करके अब भगवान अगले श्लोक में अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं।











