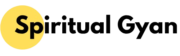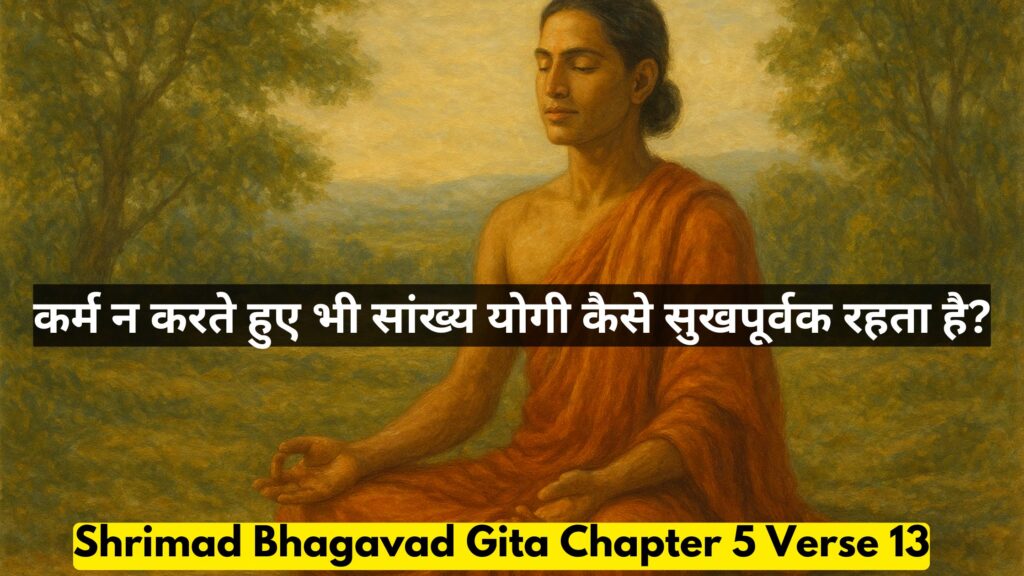
Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 13
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥१३॥
अर्थात भगवान कहते हैं, वश में किये हुए शरीर वाला मनुष्य, शुद्ध मन से सम्पूर्ण कर्मों का त्याग करके, नौ द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में (अपने स्वरूप में) सुखपूर्वक स्थित रहता है, भले ही वह स्वयं ऐसा न करता हो या दूसरों से ऐसा नहीं कराता हो।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 13 Meaning in hindi
कर्म से मुक्त रहने वाला ‘वशी देही’ कौन होता है?
–वशी देही
इंद्रिया, मन, बुद्धि वगैरा में ममता आसकती होने से ही वह मनुष्य ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, ममता आसक्ति ना रहने से वह अपने आप खुद के वश में रहते हैं संख्यायोगी की इंद्रियां, मन, बुद्धि, वगैरह में ममता आसकती न रहने से वह सर्वथा उनके वश में रहते हैं। इसीलिए उनके लिए यहां वशी शब्द आया है।
जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य (शरीर, इन्द्रिय आदि) से किंचितमात्र भी सम्बन्ध है, तब तक वह ‘अवश:’ है, अर्थात् प्रकृति के अधीन है। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है। अतः प्रकृति के साथ निरन्तर सम्बन्ध रहने के कारण मनुष्य कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। किन्तु प्रकृति के तीनों शरीरों – स्थूल, सूक्ष्म और कारण – में आसक्ति ममता न होने के कारण, सांख्य योगी उनके कर्मों का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर से किंचितमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, फिर भी वह लोगों की दृष्टि में शरीरधारी ही प्रतीत होता है। इसीलिए उसे ‘देही’ कहा गया है।
गीता के अनुसार आत्मा और शरीर नगर-निवासी के समान कैसे हैं?
–नवद्वारे पुरे
शब्द आदि विषयों के सेवन के लिए दो कान, दो आंखें, दो नासिका छिद्र और एक मुख शरीर के ऊपरी भाग में हैं, तथा मल त्याग के लिए दो द्वार, गुदा और मलद्वार, शरीर के निचले भाग में हैं। इन नौ द्वारों वाले शरीर को ‘पुर’ अर्थात् नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नगर और उसमें रहने वाला व्यक्ति दो भिन्न वस्तुएं हैं, उसी प्रकार यह शरीर और इसमें रहने की इच्छा रखने वाली आत्मा भी दो भिन्न वस्तुएं हैं। जिस प्रकार नगर में रहने वाला व्यक्ति नगर में होने वाले कर्मों को अपना कर्म नहीं मानता, उसी प्रकार सांख्य योगी शरीर में होने वाले कर्मों को अपना कर्म नहीं मानता।
गीता के अनुसार मन द्वारा कर्म का त्याग कैसे किया जाता है?
–सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य
यहाँ “मनसा संन्यस्य” शब्दों का अर्थ है – मन से, विवेक से त्याग करना। यदि उन शब्दों का अर्थ केवल मन से त्याग करना लिया जाए, तो दोष है। क्योंकि मन से त्याग भी मन की ही एक क्रिया है और गीता मन द्वारा किए गए कर्म को ‘कर्म’ मानती है। यद्यपि मन शरीर द्वारा किए गए कर्मों का कर्तापन त्याग देता है, फिर भी मन के कर्म (त्याग) का कर्तापन तो रहता ही है! अतः मनसा संन्यस्य पदों का अर्थ है – मन द्वारा विवेकपूर्वक कर्मों का कर्तापन त्यागना, अर्थात् कर्तापन के साथ ग्रहण किए गए संबंध का त्याग करना। जहाँ से कर्तापन का संबंध माना जाता है, वहाँ से उसके संबंध का त्याग करना पड़ता है। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है।
यह भी पढ़ें : क्या सांख्य योग और कर्म योग के फल अलग-अलग हैं?
गीता के अनुसार आत्मा कर्ता क्यों नहीं है?
–नैव कुर्वन्न कारयन्
सांख्य योगी न तो कर्ता है और न ही करता है। चूँकि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि से उसका किंचित् मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, अतः सांख्य योगी इनके द्वारा किए गए कर्मों का स्वयं को कर्ता कैसे मान सकता है? अर्थात् वह ऐसा कभी मान ही नहीं सकता। तेरहवें अध्याय के इकतीसवें श्लोक में भगवान् कहते हैं, शरीर में रहने के बावजूद भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता।
कर्म न करते हुए भी सांख्य योगी कैसे सुखपूर्वक रहता है?
–आसते सुखम
मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था केवल रूप में ही होती है, किन्तु वह शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि में अपनी अवस्था धारण कर लेता है, जिसके कारण उसे उस स्वाभाविक अवस्था का अनुभव नहीं होता। किन्तु सांख्य योगी अपनी स्वाभाविक अवस्था का निरन्तर रूप में अनुभव करता है। वह रूप सदैव सुखस्वरूप है। वह सुख निरन्तर, एकरस और विखण्डन से रहित है।
इस श्लोक में कहने में आया की सांख्य योगी ना तो कर्म करता है और ना करवाता भी है परंतु भगवान तो कर्मों कराते होंगे? इसका उत्तर अगले श्लोक में देखते हैं।