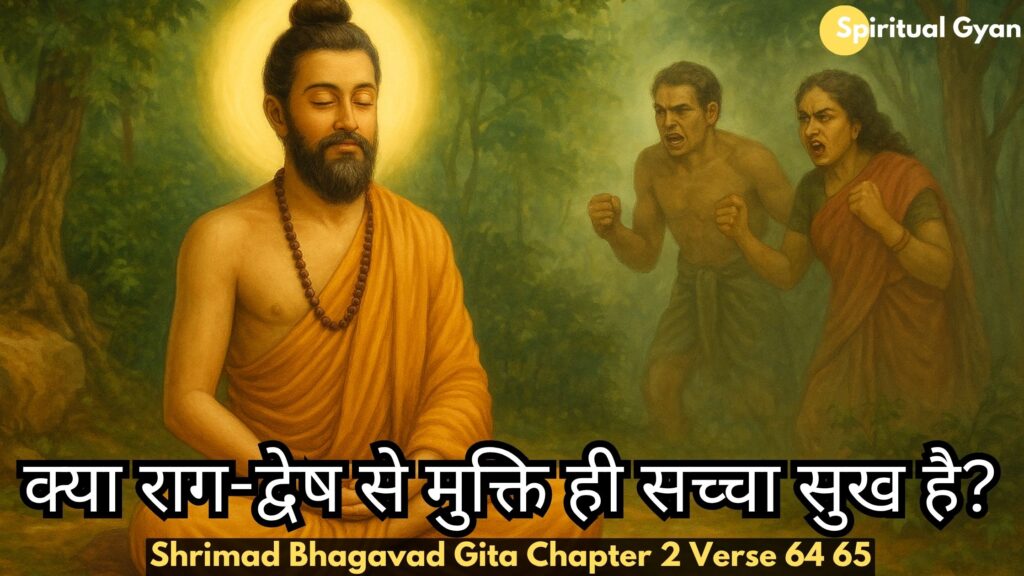
Bhagavad gita Chapter 2 Verse 64 65
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् |
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति || 64 ||
प्रसादे सर्वदु:खानां हानिरस्योपजायते |
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते || 65 ||
अर्थात भगवान कहते हैं, राग-द्वेष से रहित, वश में किये हुए हृदय वाला कर्म योगी, वश में की हुई इन्द्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करने पर भी हृदय के सुख को प्राप्त करता है। सुख को प्राप्त करके साधक के समस्त दुःख नष्ट हो जाते हैं तथा ऐसे आनन्दित साधक की बुद्धि निस्संदेह शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 2 Shloka 64 65 Meaning in hindi
कर्म करते समय मन को कैसे रखें वश में? गीता का दृष्टिकोण
र्विधेयात्मा
साधक का हृदय उसके वश में होना चाहिए। अंत:करण को वश में किए बिना कर्मयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके विपरीत कर्म करते हुए भी विषयों में आसक्ति और पतन की संभावना बनी रहती है। वस्तुतः प्रत्येक साधक के लिए हृदय को वश में रखना आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो यह विशेष रूप से आवश्यक है।
क्या राग-द्वेष से मुक्त हुए बिना इन्द्रियों पर नियंत्रण संभव है?
आत्मवश्यै रागद्वेषवियुक्तैस्तु इंद्रिये:
जिस प्रकार मन को वश में करने के अर्थ में र्विधेयात्मा शब्द का प्रयोग होता है, उसी प्रकार इन्द्रियों को वश में करने के अर्थ में आत्मवश्यै शब्द का प्रयोग होता है। तात्पर्य यह है कि अपने कार्य करते समय इन्द्रियों को अपने वश में रखना चाहिए और इन्द्रियों को वश में रखने के लिए इन्द्रियों का राग-द्वेष से मुक्त होना आवश्यक है। अतएव आसक्ति के कारण इन्द्रियों द्वारा किसी भी विषय को ग्रहण नहीं करना चाहिए और द्वेष के कारण किसी भी विषय को त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि विषयों का ग्रहण और त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना इन्द्रियों में राग-द्वेष को उत्पन्न न होने देने का महत्व है। अतएव तीसरे अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में भगवान ने साधक को सावधान किया है कि प्रत्येक इन्द्रिय के विषय में राग-द्वेष रहते हैं। साधक को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। पांचवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि ‘जो साधक राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों से मुक्त हो जाता है, वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है।’
यह भी पढ़ें : जन्म-मरण के बंधन से कैसे मुक्त हों?
कैसे करें काम और जीवन में संतुलन बिना आसक्ति के?
विषयान् चरन्
जिस साधक का मन उसके वश में है और जिसकी इन्द्रियाँ राग-द्वेष से रहित होकर उसके वश में हैं, ऐसा साधक इन्द्रियों का उपयोग विषयों के भोग के लिए करता है, अर्थात् सब प्रकार के कार्यों में संलग्न रहता है, परन्तु विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया गया विषयों का भोग पतन का कारण है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ र्विधेयात्मा, ‘आत्मवश्यै’ आदि का उल्लेख किया गया है।
क्या आसक्ति से रहित जीवन ही सच्चे सुख की कुंजी है?
प्रसादमधिगच्छति
आसक्ति और द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक को हृदय का सुख (शुद्धि) प्राप्त होता है। यह सुख मानसिक तप है, जो शारीरिक और वाचिक तप से भी श्रेष्ठ है। इसलिए साधक को न तो आसक्ति सहित विषयों का सेवन करना चाहिए और न आसक्ति सहित विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति और द्वेष-ये दोनों ही हमें संसार से जोड़ते हैं। आसक्ति और द्वेष से रहित होकर इन्द्रियों द्वारा विषयों का सेवन करने से जो सुख मिलता है, यदि उससे संबद्ध न हुआ जाए, यदि उसका भोग न किया जाए, तो वह सुख परब्रह्म की प्राप्ति कराता है।
प्रसादे सर्वदु:खानां हानिरस्योपजायते
मन की प्रसन्नता (शुद्धि) प्राप्त होने पर सभी दुःख नष्ट हो जाते हैं, अर्थात कोई दुःख नहीं रहता, क्योंकि आसक्ति के कारण ही मन में दुःख उत्पन्न होता है। दुःख उत्पन्न होते ही कामना उत्पन्न होती है और कामना से ही सभी दुःख उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब कामना दूर हो जाती है, तब मन में सुख उत्पन्न होता है। उस सुख से सभी दुःख दूर हो जाते हैं।
यहाँ ‘सर्वदुःखानां हानिकारकः‘ का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे किसी दुःखद स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, अपितु इसका तात्पर्य यह है कि उसके कर्मों के अनुसार उसके सामने दुःखद घटनाएँ और परिस्थितियाँ आ सकती हैं, किन्तु उसका अन्तःकरण दुःख, शोक, व्याकुलता आदि से विचलित नहीं हो सकता।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते
प्रसन्न (स्वच्छ) मन वाले व्यक्ति की बुद्धि बहुत शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है अर्थात् साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तथा उसकी बुद्धि में एक भी सन्देश नहीं रहता।
FAQs
क्या राग-द्वेष से मुक्ति ही सच्चा सुख है?
राग (आसक्ति) और द्वेष (घृणा) मन की दो प्रवृत्तियाँ हैं जो हमें विषयों में बांधती हैं। ये हमारे निर्णयों को असंतुलित करती हैं और मानसिक अशांति का कारण बनती हैं।
क्या राग-द्वेष से मुक्त व्यक्ति जीवन की चुनौतियों से अछूता रहता है?
नहीं, उसे भी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वह उनसे दुखी नहीं होता क्योंकि उसका मन संतुलित और बुद्धि स्थिर रहती है।
आज की जीवनशैली में राग-द्वेष से कैसे बचा जाए?
ध्यान, स्व-निरीक्षण, और निष्काम कर्म की भावना के साथ जीवन जीने से हम धीरे-धीरे राग-द्वेष की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं।
क्या राग-द्वेष से मुक्ति आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है?
हाँ, गीता के अनुसार यह आत्म-शुद्धि का मूल है। जब मन शांत और बुद्धि स्थिर होती है, तभी आत्मज्ञान संभव होता है।











