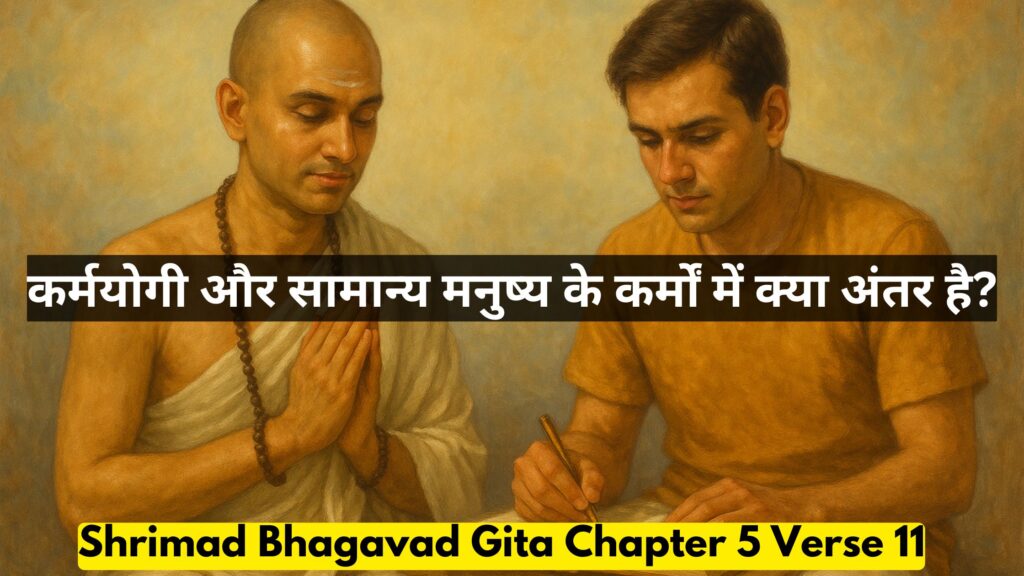
Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 11
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥११॥
अर्थात भगवान कहते हैं, कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके इन्द्रियों, शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से (आसक्ति रहित होकर) केवल हृदय की शुद्धि के लिए कर्म करता है।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 11 Meaning in hindi
भक्तियोगी और कर्मयोगी में क्या अंतर है?
–योगिनः
यहाँ योगिन: पद का प्रयोग कर्मयोगी के लिए किया गया है। जो योगी ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से कर्म करते हैं, उन्हें भक्तियोगी कहते हैं। किन्तु जो योगी संसार की सेवा की इच्छा न रखते हुए कर्म करते हैं, उन्हें कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोगी अपने तथाकथित शरीर, इन्द्रियों, मन आदि से कर्म करते हुए भी, उन्हें अपना नहीं, अपितु संसार का मानता है। क्योंकि शरीर आदि संसार के साथ एकाकार हैं।
कर्मयोग में शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि को ‘अपना न मानने’ का क्या महत्व है?
–कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि
जिन्हें सामान्य मनुष्य अपना मानते हैं, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, वास्तव में किसी भी दृष्टि से उनके अपने नहीं हैं, बल्कि वे हमें दिए गए हैं और पृथक होने के अधीन हैं, उन्हें अपना मानना भूल है। इन सभी का संसार के साथ स्वतः आरोपित एकत्व है।
यदि हम विचारपूर्वक देखें, तो शरीर आदि वस्तुएँ किसी भी दृष्टि से हमारी अपनी नहीं हैं। यदि हम उन्हें मालिकी की दृष्टि से देखें, तो वे प्रकृति की हैं, यदि हम उन्हें कर्म की दृष्टि से देखें, तो वे ईश्वर की हैं और यदि हम उन्हें कारण की दृष्टि से देखें, तो वे संसार की हैं (संसार से स्वतंत्र)। इस प्रकार, उन्हें किसी भी दृष्टि से अपना मानना और उनमें अनुराग रखना भूल है। अनुराग को पूर्णतः दूर करने के लिए यहाँ केवलै: पद का प्रयोग किया गया है।
वास्तव में, कर्ता का स्वयं निष्काम होना आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निष्काम हो, तो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि से आसक्ति सर्वथा दूर हो जाती है। क्योंकि वस्तुतः शरीर इन्द्रियों आदि के स्वरूप से सर्वथा भिन्न है, अतः उनमें आसक्ति केवल अनुभव की जाती है, वस्तुतः होती नहीं।
कर्मयोग के अभ्यास में फल की इच्छा का त्याग ही मुख्य है। सामान्य लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, परन्तु कर्मयोगी फल की आसक्ति दूर करने के लिए कर्म करता है। परन्तु जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता है, वह फल की इच्छा नहीं छोड़ सकता। क्योंकि उसकी ऐसी भावना है कि शरीर आदि मेरे अपने हैं, तो इनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी हमें मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से फल की इच्छा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। अतः फल की इच्छा दूर करने के लिए शरीर आदि को कभी अपना न समझना अत्यन्त आवश्यक है।
यह भी पढ़ें : क्या संन्यास बिना कर्मयोग के संभव है?
क्या अहंकार में भी आसक्ति होती है? गीता इस पर क्या कहती है?
–सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये
सामान्यतः, मलिनता, अशुद्धियों और आवरण दोषों के निवारण को मन की शुद्धि माना जाता है। किन्तु वास्तव में, मन की शुद्धि शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धि से आसक्ति का पूर्णतः निराकरण है। शरीर आदि कभी यह नहीं कहते कि हम आप में हैं और आप हम में हैं। हम इन्हें अपना मानते हैं। इन्हें अपना मानना ही अशुद्धि है। अतः शरीर आदि के प्रति अहंकारपूर्ण माने गए सम्बन्ध का पूर्णतः अभाव ही आत्म-साक्षात्कार है।
अहंकार में भी आसक्ति होती है। जब आसक्ति पूरी तरह से हट जाती है, जब अहंकार में भी आसक्ति नहीं रहती, तब सब कुछ शुद्ध हो जाता है।
कर्मयोगी और सामान्य मनुष्य के कर्मों में क्या अंतर है?
–कर्म कुर्वन्ति
कर्मयोगी शरीर, मन और आत्मा में स्थित सूक्ष्म आत्मा को पूर्णतः हटाने के लिए कर्म करते हैं।
जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार के सुख की कामना करता है, अर्थात् किसी प्रकार के फल की कामना करता है और शरीर, इन्द्रिय, मन आदि को अपना मानता है, तब तक वह कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और फल को अपना न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। क्योंकि योग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मननशील योगी के लिए (दूसरों के हित के लिए) कर्म करना ही एकमात्र साधन कहा गया है। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए कर्म करते ही आसक्ति का लोप हो जाता है और मन शुद्ध हो जाता है।
यह भी पढ़ें :
क्या ईश्वर को अर्पित कर्म पाप से मुक्त करते हैं?
सांख्य योगी क्यों मानता है कि मैं कुछ नहीं करता?
कर्मयोगी इन्द्रियों को वश में करके जीवन में क्या लाभ पाता है?











