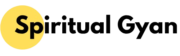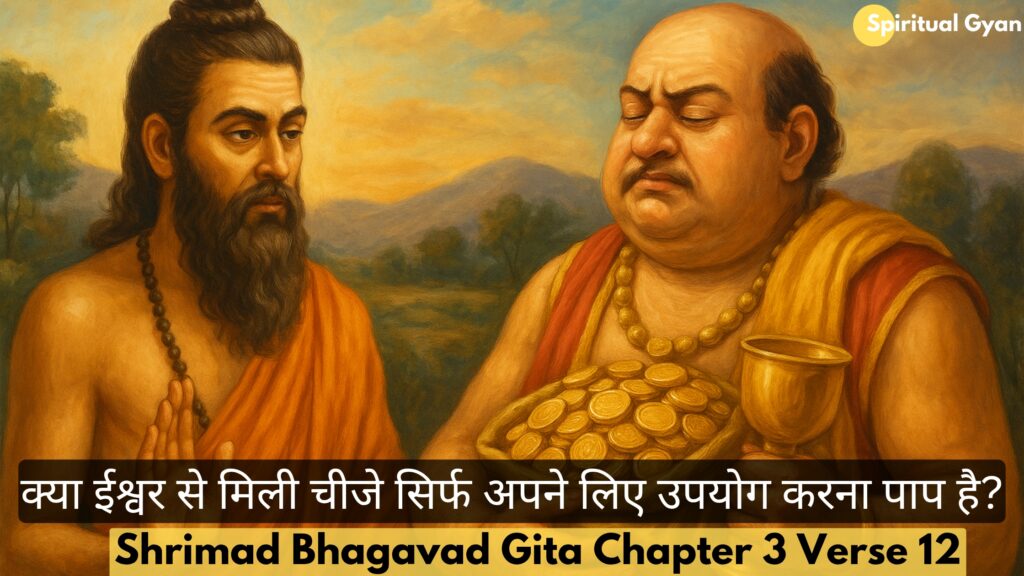
Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 12
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: |
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स: || 12 ||
अर्थात भगवान कहते हैं, यज्ञशक्ति से युक्त देवता भी तुम लोगों को (बिना मांगे) ही तुम्हारे कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार जो मनुष्य उन देवताओं से प्राप्त सामग्री को दूसरों की सेवा में उपयोग किए बिना भोगता है, वह चोर है।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 12 Meaning in hindi
क्या प्रकृति तभी कुछ देती है जब हम अपना फर्ज़ निभाते हैं?
–इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता:
यहाँ ‘यज्ञभावितः देवाः’ पद का तात्पर्य यह है कि देवता अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं, मनुष्यों को ही अपना कर्तव्य निभाना है।
क्या ईश्वर से मिली चीज़ें सिर्फ अपने लिए उपयोग करना पाप है?
–तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते
यह शरीर हमें हमारे माता-पिता ने दिया है और उन्हीं ने इसका पालन-पोषण किया है। ज्ञान हमें हमारे गुरुओं ने दिया है। देवता हमें हमारे कर्तव्यों के लिए सामग्री देते हैं। ऋषि हमें ज्ञान देते हैं। माता-पिता हमें मनुष्यों के सुख और कल्याण के साधन बताते हैं। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी अपने आपको दूसरों के सुख के लिए समर्पित करते हैं (यद्यपि पशु, पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं होता कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं)। इस प्रकार जो भी सामग्री, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति आदि हमें दूसरों से मिली है। इसलिए हमें उनका उपयोग दूसरों की सेवा में करना है।
शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि विगेरे सारे पदार्थ हमें संसार से मिले हैं यह कभी हमारे नहीं और कभी होंगे भी नहीं इसीलिए उनको खुद का और खुद के लिए मनाना तथा उनसे सुख भोगना, वही बंधन है। इस बंधन से छूटने का एक ही शरण उपाय हैं कि हमें जिनके पास से यह पदार्थ मिले हैं उन्हें, उन्हही की सेवा में लगाकर निष्काम भावपूर्वक खर्च कर देने चाहिए, यही हमारा परम कर्तव्य है।
यह भी पढ़ें : समुद्र जैसा संयम कैसे लाएं जीवन में? भगवद गीता से सीख
साधकों के मन में प्रायः यह भावना आती है कि यदि हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें आसक्त हो जायेंगे और संसार में फँस जायेंगे! परन्तु भगवान के वचन सिद्ध करते हैं कि फँसने का कारण सेवा नहीं, अपितु अपने लिए कुछ पाने की इच्छा है। अतः मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह पाने की इच्छा का त्याग कर दे और देवताओं की भाँति दूसरों को सुख पहुँचाये।
कर्मयोग का सिद्धान्त है कि प्राप्त पदार्थ, शक्ति, समय और बुद्धि का सदुपयोग करना। प्राप्त पदार्थ से अधिक (नये पदार्थ आदि) की इच्छा करना कर्मयोग के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अतः प्राप्त पदार्थ का उपयोग दूसरों के हित में करना है। तनिक भी अधिक की आवश्यकता नहीं करनी है। तर्कपूर्ण बात यह है कि जिसके पास जितनी शक्ति है, उसे से उतनी ही अपेक्षा की है, फिर भगवान या देवता उससे अधिक की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं?
क्या सिर्फ अपने लिए जीना वास्तव में चोरी के समान है?
–स्तेन एव स:
जो व्यक्ति दूसरों को दिए बिना अपना हिस्सा भोगता है, वह चोर है, लेकिन जो व्यक्ति किसी भी तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात भौतिक वस्तुओं का उपयोग सेवा में करता है और बदले में सम्मान और महिमा चाहता है, वह भी उसी सीमा तक चोर है। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता।
यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से सम्पूर्ण जगत् से पृथक् नहीं है और पृथक् हो भी नहीं सकता, क्योंकि सम्पूर्ण का एक अंश ही व्यक्ति कहलाता है। अतः व्यष्टि (शरीर) को अपना मानना और सम्पूर्ण जगत् को अपना न मानना ही राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों का कारण है और यही अहंकार, वैयक्तिकता या भेद भी है। यह सब (राग-द्वेष आदि) कर्मयोग के अभ्यास से सरलता से दूर हो जाता है। क्योंकि कर्मयोगी को ऐसा भाव रहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, वह अपने लिए नहीं, अपितु संसार के लिए ही कर रहा हूँ। इसमें एक बड़ी विडम्बना यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं करता, अपितु संसार के कल्याण के उद्देश्य से ही अपने सभी कार्य करता है। क्योंकि अपने कल्याण को सबके कल्याण से पृथक् मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देने के समान है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। हमारे पास जो कुछ भी है, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि, वह सब हमें संसार से मिला है। संसार से जो कुछ भी मिला है, उसका उपयोग केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए करना ईमानदारी नहीं है।