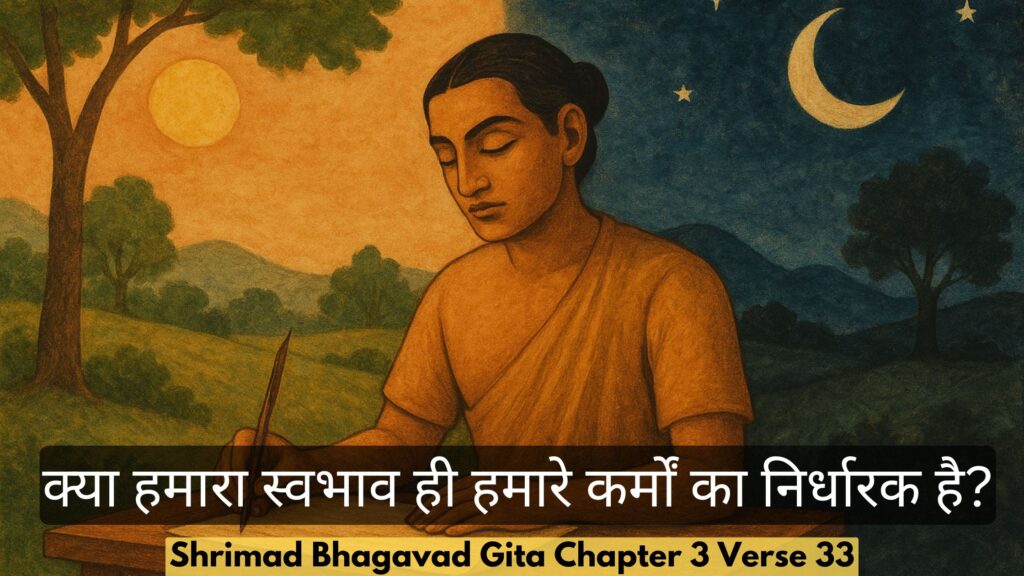
Bhagavad Gita Chapter 3 Verse 33
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥
अर्थात भगवान कहते हैं, सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं। बुद्धिमान और महान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। फिर उसमें किसी की हठ क्या करेगी?
shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 33 Meaning in Hindi
क्या राग-द्वेष से किया गया कर्म ही जीवन में बंधन का कारण है?
–प्रकृतिं यान्ति भूतानि
जो भी कर्म किए जाते हैं, वे स्वभाव और तत्त्व को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है – अनासक्त और आसक्ति सहित। जैसे कोई सड़क पर चलते हुए साइनबोर्ड पढ़ता है, तो वह न आसक्ति से होता है, न तत्त्व से, बल्कि आसक्ति रहित स्वभाव से होता है। यदि कोई मित्र का पत्र राग पूर्वक पढ़ता है, और यदि कोई शत्रु का पत्र द्वेष पूर्वक से पढ़ता है, तो वह पढ़ना रागद्वेषयुक्त स्वभाव से होता है। गीता, रामायण आदि सत्य शास्त्रों का पठन ‘तत्त्व’ से होता है। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी तत्त्वानुसार कर्म करना कहलाता है।
इस प्रकार देखना, स्पर्श करना आदि मन की क्रियाएँ प्रकृति और तत्त्व दोनों के द्वारा होती हैं। राग-द्वेष से रहित प्रकृति दोषयुक्त नहीं होती, किन्तु राग-द्वेष से युक्त प्रकृति दोषयुक्त होती है। राग-द्वेष से किए गए कर्म व्यक्ति को बांधते हैं, क्योंकि वे प्रकृति को अशुद्ध करते हैं, और तत्त्व से किए गए कर्म मुक्तिदायक होते हैं, क्योंकि वे प्रकृति को शुद्ध करते हैं। प्रकृति के अशुद्ध हो जाने से संसार के साथ बोधगम्य संबंध नहीं टूटता। जब प्रकृति शुद्ध हो जाती है, तो संसार के साथ बोधगम्य संबंध सहज ही टूट जाता है।
ज्ञानी महापुरुष के कर्म उसके अपने शरीर द्वारा, जिसे वह अपना कहता है, स्वतः ही होते रहते हैं, क्योंकि उसमें कर्तापन का बोध नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधक के कर्म सिद्धांतानुसार होते हैं। जिस प्रकार लोभी व्यक्ति सदैव सावधान रहता है कि कहीं कोई हानि न हो, उसी प्रकार साधक भी सदैव सावधान रहता है कि कोई भी कर्म द्वेष या क्रोध से न हो। ऐसी सावधानी बरतने से साधक का स्वभाव तत्काल शुद्ध हो जाता है और फलस्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
प्रकृति का मुख्य दोष प्राकृतिक वस्तुओं की इच्छा है। जब तक प्रकृति में इच्छा है, तब तक अशुद्ध कर्म होते रहते हैं। इसलिए साधक के लिए इच्छा ही बंधन का मुख्य कारण है।
क्या हमारा स्वभाव ही हमारे कर्मों का निर्धारक है?
–सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि
यद्यपि ज्ञानी पुरुष का स्वभाव निष्पाप होता है, क्योंकि उसके हृदय में राग-द्वेष का अभाव होता है और वह स्वभाव के अधीन नहीं होता, फिर भी वह अपने स्वभाव (प्रकृति) के अनुसार ही कार्य करता है। जैसे एक ज्ञानी पुरुष, जो अंग्रेजी नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने को कहा जाए, तो बोल नहीं सकता। वह जिस भाषा को जानता है, उसी में बोलेगा।
यहाँ स्वस्याः पद का अर्थ है कि ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव दोषरहित होता है। वह स्वभाव के अधीन नहीं होता, प्रत्युत स्वभाव उसके अधीन हो जाता है। कर्मफल उत्पन्न होने का मूल बीज है कर्म का अभिमान और स्वार्थ की बुद्धि। ज्ञानी महापुरुष में कर्म का अभिमान और स्वार्थ की बुद्धि नहीं होती। उससे केवल कर्म ही होते हैं। कर्म ही बंधनकारक बनता है, चेष्टा या क्रिया नहीं। इसीलिए यहाँ ‘चेष्टते’ शब्द का प्रयोग हुआ है। उसका स्वभाव इतना शुद्ध है कि उसके द्वारा किए गए कर्म भी अत्यंत शुद्ध और साधकों के लिए आदर्श होते हैं।
पूर्व और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता-पिता के संस्कार, वर्तमान की संगति, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, कर्म, भावना आदि के अनुसार स्वभाव का निर्माण होता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न-भिन्न होता है और सभी मनुष्य उसे शुद्ध बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत स्वभाव का भेद ज्ञानी महापुरुषों में भी रहता है। चेतना में कोई भेद नहीं होता और स्वभाव (प्रकृति) में स्वाभाविक भेद होता है। स्वभाव विषमांगी होता है। जैसे आम आदि वृक्षों में एक ही जाति के होने पर भी भेद होता है, वैसे ही ज्ञानी महापुरुषों में स्वभाव (प्रकृति) शुद्ध होने पर भी स्वभाव में भेद होता है।
यह भी पढ़ें : क्या बिना आसक्ति के किया गया काम हमें परमात्मा तक ले जा सकता है?
क्या अशुद्ध स्वभाव पर हठ करने से जीवन की दिशा बदली जा सकती है?
–निग्रहः किं करिष्यति
जिनका स्वभाव अत्यंत शुद्ध और उत्तम है, उनके कर्म भी उनके स्वभाव के अनुसार ही होते हैं, फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध (राग-द्वेष वाला) है, उन मनुष्यों के कर्म भी उनके स्वभाव के अनुसार ही होंगे। इस विषय में हठ उनके किसी काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव होगा, उसे उसके अनुसार ही कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध है, तो वह मनुष्य को अशुद्ध कर्मों में प्रवृत्त करेगा और यदि शुद्ध है, तो वह मनुष्य को शुद्ध कर्मों में प्रवृत्त करेगा।
जब अर्जुन हठपूर्वक युद्ध-कर्तव्य का परित्याग करना चाहता है, तब भी भगवान् उससे कहते हैं: तुम्हारा स्वभाव तुम्हें बलपूर्वक युद्ध में बाँधेगा, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में क्षात्रकर्म (युद्ध आदि) करने का प्रवाह है। अतः स्वाभाविक कर्मों से बँधे हुए तुम पराक्रमी होकर युद्ध करोगे, अर्थात् इसमें तुम्हारा हठ किसी काम का नहीं होगा।
जिस प्रकार सौ मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं चलती, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपने शुद्ध स्वभाव के विरुद्ध कार्य नहीं करता। जिनका स्वभाव अशुद्ध है, वे टूटी हुई मोटर के समान हैं। टूटी हुई मोटर को ठीक करने के दो मुख्य उपाय हैं—(1) मोटर को स्वयं ठीक करना और (2) मोटर को कारखाने में ले जाना। इसी प्रकार अशुद्ध स्वभाव को ठीक करने के भी दो मुख्य उपाय हैं—(1) राग-द्वेष से मुक्त होकर कर्म करना (गीता Ch 3/34) और (2) ईश्वर की शरण लेना (गीताCh 18/62)। यदि मोटर ठीक चल रही है, तो हम मोटर के वश में नहीं हैं और यदि मोटर खराब है, तो हम मोटर के वश में हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष शुद्ध स्वभाव होने के कारण स्वभाव के वश में नहीं होता और अज्ञानी पुरुष अशुद्ध स्वभाव होने के कारण स्वभाव के वश में होता है।
प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के साथ जन्म लेता है; अतः उसे अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करने पड़ते हैं। इसीलिए अब भगवान अगले श्लोक में स्वभाव शुद्धि का उपाय बताते हैं।











