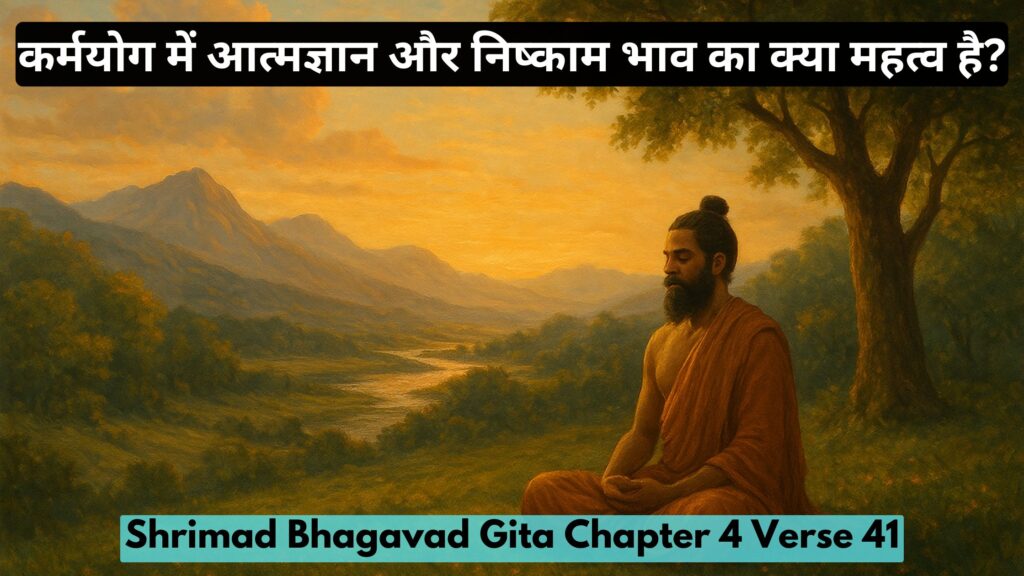
Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 41
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥४१॥
अर्थात भगवान कहते हैं, हे धनंजय! जो योग (समता) के द्वारा सम्पूर्ण कर्मों से पृथक हो गया है और जिसका ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट हो गया है, ऐसा स्वरूप पुरुष कर्मों से नहीं बंधता।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 4 Verse 41 Meaning in hindi
योगसंन्यस्तकर्माणं का क्या अर्थ है और गीता में इसका महत्व क्यों बताया गया है?
–योगसंन्यस्तकर्माणं
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएँ हमें प्राप्त हैं और जिन्हें हम अपनी मानते हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए हैं, अपना अधिकार जताने के लिए नहीं। इस दृष्टि से, जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में (अपना मानकर) व्यवस्थित किया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और व्यक्ति स्वयं में आत्म-सिद्ध समता का अनुभव करता है। इस प्रकार, जिसने योग (समता) द्वारा कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है, वह ‘योगसंन्यस्तकर्मा’ है।
जब कर्मयोगी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, अर्थात् कर्म करते हुए या न करते हुए, वह दोनों अवस्थाओं में निरंतर अनासक्त रहता है, तब वह वास्तव में योगसंन्यस्तकर्मा बनता है।
कर्मयोग में आत्मज्ञान और निष्काम भाव का क्या महत्व है?
–ज्ञानसंछिन्नसंशयम्
मनुष्य के मन में प्रायः यह शंका रहती है कि कर्म करते रहने से कर्म से कैसे विरत हुआ जा सकता है? यदि अपने लिए कुछ न किया जाए तो अपना कल्याण कैसे हो सकता है? आदि। परन्तु जब मनुष्य कर्म के सार को भली-भाँति समझ लेता है, तो उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं। उसे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि कर्म और उसके फल का आदि और अंत तो होता है, परन्तु रूप तो सदैव ज्यों का त्यों रहता है। अतः कर्म का संबंध केवल ”(संसार) से है, ”(स्वरूप) से नहीं। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म से संबंधित हो जाता है और निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म से विमुख हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दूसरों के लिए कर्म करने से ही कल्याण होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं।
गीता के अनुसार आज के जीवन में सच्चे कर्मयोगी की पहचान कैसे करें?
–आत्मवन्तं
कर्मयोग का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए वह सदैव रूप से विमुख रहता है। उसके सभी कर्म संसार के लिए होते हैं, रूप के माध्यम से दूसरों की सेवा की जाती है, जीवन के सभी कर्म जैसे खाना-पीना, सोना-बैठना आदि भी दूसरों के लिए होते हैं, क्योंकि कर्म का संबंध केवल संसार से है, स्वरूप से नहीं।
गीता के अनुसार कर्म से बंधन कैसे टूटते हैं?
–न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय
अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्म योगी सभी कर्मों से विच्छिन्न हो जाता है, अर्थात वह संसार के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधन कारक है ही नहीं, कर्मों में फल की इच्छा, ममता आसकती और कर्तृत्वभिमान ही बांधने वाले हैं।
इस श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान से संशय नष्ट हो जाता है और समता से मनुष्य कर्मों से पृथक हो जाता है। अब अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि तूम ज्ञान से संशय को नष्ट करो और समता में स्थित हो जाव।
यह भी पढ़ें :
गीता के अनुसार संशयी व्यक्ति का क्या होता है?
श्रद्धा और संयम से कैसे मिलती है परम शांति?











