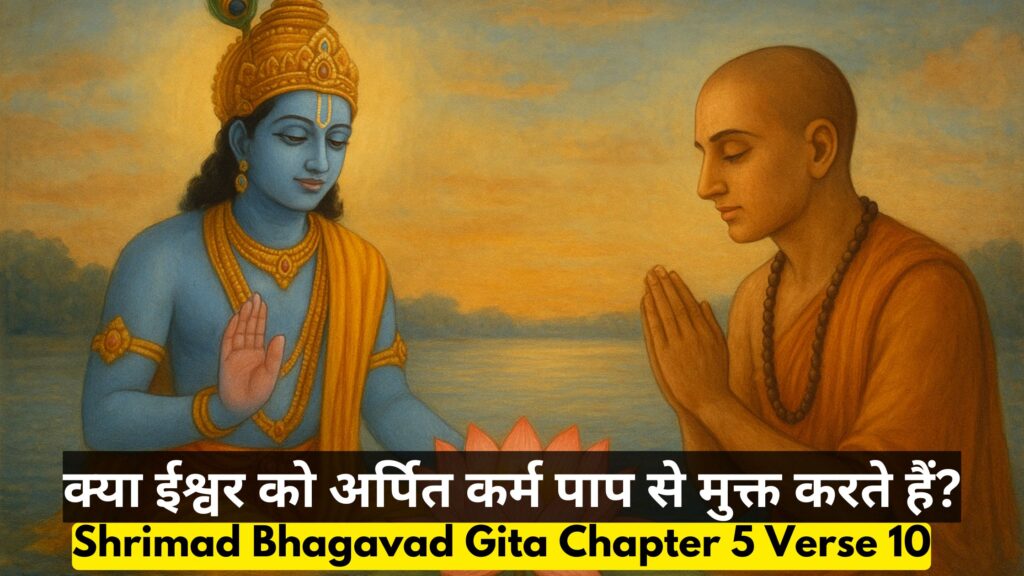
Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 10
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।१०।।
अर्थात भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके तथा आसक्ति का त्याग करके करता है, वह जल में कमल की पंखुड़ियों की तरह पाप में नहीं फंसता।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 10 Meaning in hindi
क्या ईश्वर को अर्पित कर्म पाप से मुक्त करते हैं?
–ब्रह्मण्याधाय कर्माणि
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के हैं, खुदके नहीं! अतः भक्त इनसे होने वाले कर्मों को अपना कैसे मान सकता है? इसीलिए उसे ऐसा भाव होता है कि सभी कर्म भगवान ही कर रहे हैं और भगवान के लिए मैं तो केवल साधन हूँ।
भगवान ही अपनी इंद्रियों द्वारा खुद ही सारी क्रिया करते हैं इस बात को अच्छी तरह से धारण करके सारी क्रियो के कर्तापन को भगवान को ही मनाना चाहिए।
शरीर आदि वस्तुएँ हमारी अपनी नहीं हैं, अपितु प्राप्त होती हैं और अलग होती रहती हैं। ये केवल ईश्वर से प्राप्त होती हैं, ताकि ईश्वर के निमित्त दूसरों की सेवा की जा सके। उन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात् हम उन्हें अपनी इच्छानुसार नहीं रख सकते, न ही उन्हें बदल सकते हैं, न ही मृत्यु के समय उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। अतः इन शरीरों आदि को तथा इनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को अपना मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी से इन्हें उसी का मानना चाहिए जिसके वे हैं, अर्थात् ईश्वर का।
कर्मयोगी सभी कर्मों और पदार्थों को ‘संसार’ को, ज्ञानयोगी ‘प्रकृति’ को और भक्तियोगी ‘ईश्वर’ को अर्पित करता है। प्रकृति और संसार दोनों के स्वामी ईश्वर हैं। अतः कर्मों और पदार्थों को ईश्वर को अर्पित करना ही सर्वोत्तम है।
संसारिक आसक्ति का त्याग ही पापों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग क्यों माना गया है?
–सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः
कोई भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया वगैरह में किंचित मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, जुड़ाव, महत्व, ममता, कामना, विगेरे न रहना! उसे ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना कहलाता है।
यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान ही जन्म-मरण का कारण है, किन्तु माध्यम की दृष्टि से रजोगुण ही जन्म-मरण का मूल कारण है। राग पर ही अज्ञान आधारित है, इसीलिए रजोगुण के दूर होने पर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है।
इसी रजोगुण या आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। इसीलिए यहाँ पापों के मूल कारण राग को त्यागने की बात आई है, क्योंकि जब तक यह रहता है, मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके बिना मनुष्य पापों में लिप्त नहीं होता।
क्यों भक्त ईश्वर के लिए कर्म करते हुए भी पाप से अछूता रहता है, जैसे जल में कमल का पत्ता?
–लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा
यह कितनी विशेष बात है कि ईश्वर के सम्मुख भक्त संसार में रहकर ईश्वर के लिए ही सभी कर्म करता है, फिर भी कर्मों से बंधता नहीं! जिस प्रकार कमल की पंखुड़ी जल में जन्म लेकर और जल में ही रहकर भी अनासक्त रहती है, उसी प्रकार भक्त संसार में सभी कर्म करते हुए भी ईश्वर के सम्मुख होने के कारण संसार की सभी वस्तुओं से अनासक्त रहता है।
ईश्वर से विमुख होकर संसार की इच्छाएँ ही सभी पापों का मूल कारण हैं। इच्छाएँ आसक्ति से उत्पन्न होती हैं। चूँकि आसक्ति पूर्णतः अनुपस्थित है, इसलिए इच्छाएँ अस्तित्व में नहीं रह सकतीं, इसलिए पाप करने की कोई संभावना नहीं रहती।
धुएँ और अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, किन्तु जिसने आशा, कामना और आसक्ति का त्याग कर दिया है, उसे वे दोष नहीं लगते। आसक्ति रहित होकर भगवान के लिए कर्म करने के प्रभाव से सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्त का पाप से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहता।
अब भगवान अगले श्लोक में कर्मयोगि की कर्म करने की शैली बताते हैं।
यह भी पढ़ें :
सांख्य योगी क्यों मानता है कि मैं कुछ नहीं करता?
कर्मयोगी इन्द्रियों को वश में करके जीवन में क्या लाभ पाता है?











