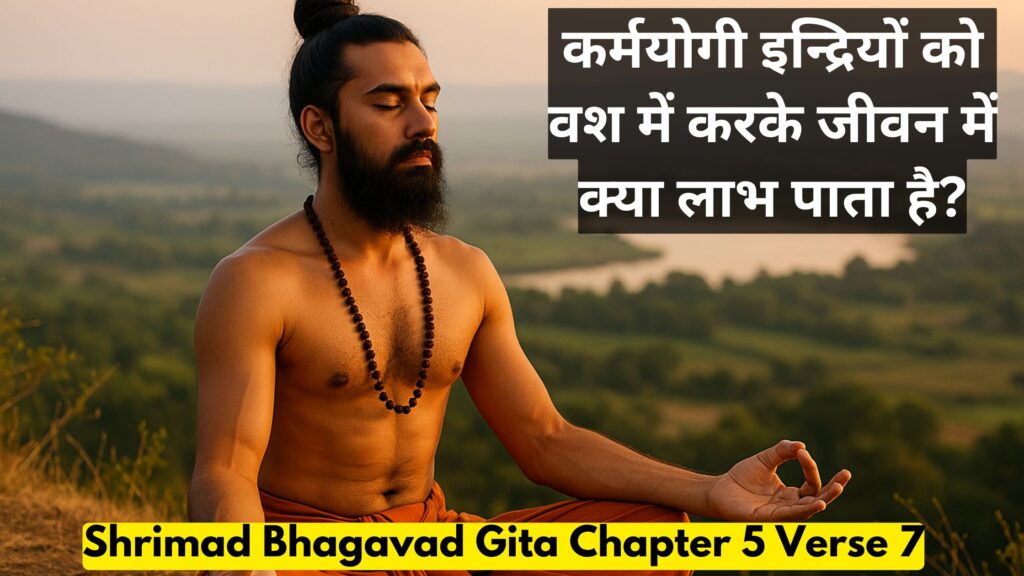
Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 7
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥७॥
अर्थात भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो कर्मयोगी अपनी इन्द्रियों को वश में रखता है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका शरीर वश में है, तथा जिसकी आत्मा समस्त प्राणियों की आत्मा है, वह कर्म करते हुए भी आसक्त नहीं होता।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 7 Meaning in hindi
कर्मयोगी इन्द्रियों को वश में करके जीवन में क्या लाभ पाता है?
–जितेन्द्रियः
इन्द्रियों के वश में होने का अर्थ है कि इन्द्रियाँ आसक्ति से मुक्त हैं। आसक्ति से मुक्त इन्द्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं होती। साधक इन्हें अपनी इच्छानुसार कहीं भी लगा सकता है।
कर्मयोग के साधक के लिए इन्द्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग के विषय में इन्द्रियों को वश में करने की विशेष बात कही है। एकाग्रचित्त योगी का कर्मों से अधिक सम्बन्ध होता है, इसीलिए इन्द्रियों के वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना बनी रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हितार्थ सेवारूपी कर्तव्य करना आवश्यक है, जिसके लिए इन्द्रियों का वश में होना परमावश्यक है। इन्द्रियों को वश में किए बिना कर्मयोग का साधक बनना कठिन है।
परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ संकल्प मन को कैसे शुद्ध करता है?
–विशुद्धात्मा
मन की अशुद्धि का कारण है – सांसारिक वस्तुओं का महत्त्व। जहाँ वस्तुओं का महत्त्व रहता है, वहाँ उनकी कामनाएँ भी रहती हैं। साधक तभी निष्काम होता है जब उसके मन में सांसारिक वस्तुओं का महत्त्व नहीं रहता। जब तक वस्तुओं का महत्त्व है, वह निष्काम नहीं हो सकता।
परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ संकल्प होने पर मन जितनी शीघ्रता से शुद्ध होता है, उतनी ही शीघ्रता से शुद्ध भी होता है। और ऐसी शुद्धि किसी अन्य साधना से नहीं होती। इसीलिए कर्मयोग में ध्येय रखने की महिमा किसी अन्य वस्तु जितनी महान नहीं है।
आलस्य त्यागना कर्मयोग साधक के लिए क्यों जरूरी है?
–विजितात्मा
कर्मयोग में शरीर के सुख-सुविधाओं का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर आलसी हो जाए, तो कर्मयोग का अभ्यास नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ भगवान ने शरीर को नियंत्रित करने की बात कही है।
दूसरों को सुख पहुँचाना कर्मयोगी का स्वभाव क्यों है?
–सर्वभूतात्मभूतात्मा
“कर्म योगी सभी प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है।” जिस प्रकार शरीर के एक अंग पर प्रहार करने पर दूसरा अंग स्वतः ही उसकी सेवा में लग जाता है, बिना किसी अभिमान या कृतज्ञता की इच्छा के, उसी प्रकार कर्म योगी का दूसरों को सुख पहुँचाने का प्रयास स्वाभाविक रूप से होता है, बिना किसी अभिमान, इच्छा या कृतज्ञता की इच्छा के। सेवा करने के लिए, वह किसी भी जीव को अपने से अलग नहीं मानता, वह सभी को अपना ही अंग मानता है।
जिस प्रकार उसके शरीर के विभिन्न अंग अलग-अलग क्रिया करते हुए भी, वह सभी अंगों के साथ एक ही रहता है, उसी प्रकार, संसार के विभिन्न अंग कर्म योगी के साथ उसकी सीमाओं के अनुसार, अलग-अलग क्रिया करते हुए भी, वह सभी के साथ एक ही रहता है।
खुदका राग दूर करने के लिए ‘सर्वभूतात्मा भूतात्मा’ बनना, अर्थात् सभी प्राणियों के साथ अपनी एकता को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। कर्म योगी का स्वभाव है – उदारता। सर्वभूतात्मा बने बिना उदारता नहीं आती।
कर्म करते हुए भी निष्काम रहने का रहस्य क्या है?
–कुर्वन्नपि न लिप्यते
कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं। कर्म बंधन के कारण हैं—कर्म में आसक्ति, कर्मफल की इच्छा, कर्म से प्राप्त सुख और उसके भोग की इच्छा, तथा कर्तापन का अभिमान। संक्षेप में, कर्म द्वारा कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही बंधन का कारण है। थोड़ा सा भी प्राप्त करने की इच्छा न होने के कारण, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं, अर्थात् उसका कर्म अकर्म बन जाता है।
कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कह कर अब भगवान अगले दो श्लोक में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं
यह भी पढ़ें :
क्या संन्यास बिना कर्मयोग के संभव है?
सांख्य योग और कर्म योग में क्या है समानता?











