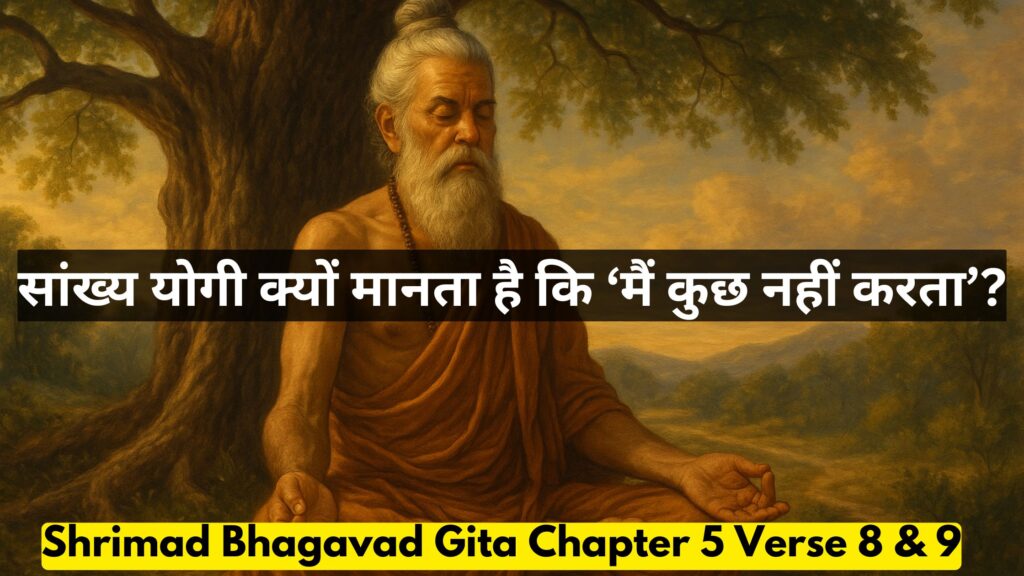
Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 8 & 9
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्नाच्छन्स्वपञ्श्वसन् ॥८॥
प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥९॥
अर्थात भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो सांख्य योगी तत्व को जानता है, वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, ग्रहण करता है, बोलता है, त्यागता है, सोता है, श्वास लेता है, तथा आंखें खोलता और बंद करता है, फिर भी यह जानकर कि समस्त इन्द्रियां इन्द्रियों के विषयों में लगी हुई हैं, वह यह मानता है कि, ‘मैं (स्वयं) कुछ नहीं करता।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 8 & 9 Meaning in hindi
सांख्य योगी क्यों मानता है कि मैं कुछ नहीं करता?
–तत्त्ववित् युक्तः
यहाँ संख्योग के काल में योग के उस विवेकशील साधक का वाचक है जो महान दार्शनिक की भाँति शुद्ध का अनुभव करने के लिए तत्पर है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सभी कर्म प्रकृति में ही हो रहे हैं, उन कर्मों का मुझसे कोई संबंध नहीं है।
जो अपने में, अर्थात् रूप में, क्षण भर के लिए भी, किसी भी कर्म का कर्तापन नहीं देखता, वह है। वह निरंतर और स्वाभाविक रूप से इस बात से अवगत रहता है कि स्वरूप में कोई कर्तापन नहीं है। वह प्रकृति, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदि के कर्मों के साथ अपनी एकता को कभी स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह उनके द्वारा किए गए कर्मों को अपना कर्म कैसे मान सकता है?
वस्तुतः स्वरूप की दृष्टि से उपरोक्त स्थिति सभी मनुष्यों की है, किन्तु वे भ्रमवश स्वरूप को ही कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। जिस शक्ति से ब्रह्माण्ड के कर्म भी हो रहे हैं, उसी शक्ति से जीव के शरीर के कर्म भी हो रहे हैं। किन्तु ब्रह्माण्ड के ही एक छोटे से अंश जीव से अपना सम्बन्ध मानने के कारण मनुष्य जीव के कुछ कर्मों को अपना ही कर्म मानने लगता है। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि साधक को अपने को कभी कर्ता नहीं मानना चाहिए। जब तक किसी सीमा तक कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहलाता है, जब उसमें कर्तापन की मान्यता सर्वथा समाप्त हो जाती है और अपने स्वरूप का अनुभव होता है, तब वह तत्व महापुरुष कहलाता है। जैसे स्वप्न से जागे हुए मनुष्य का स्वप्न से कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे ही तत्व महापुरुष का शरीर आदि से होने वाले कर्मों से कोई सम्बन्ध (कर्तापन) नहीं रहता।
यह भी पढ़ें : क्या संन्यास बिना कर्मयोग के संभव है?
आँख, कान, त्वचा, मन और प्राण से जुड़े कर्मों का वास्तविक अर्थ क्या है?
–पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्नाच्छन्स्वपञ्श्वसन्
यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना—ये पाँच कर्म (क्रमशः आँख, कान, त्वचा, मुख और स्वाद—ये पाँच) इन्द्रियों के हैं। चलना, निगलना, बोलना और मलत्याग—ये चार कर्म (क्रमशः पैर, हाथ, वाणी, जननेन्द्रिय और गुदा—ये पाँच) कर्मेन्द्रियों के हैं। सोना—यह मन की क्रिया है। साँस लेना—यह प्राण की क्रिया है, और आँखें खोलना और बंद करना—ये दो कर्म ‘कूर्म’ नामक उपप्राण के हैं।
उपर्युक्त तेरह कर्म बताकर भगवान ने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन, आत्मा और उपात्मा के द्वारा किये जाने वाले समस्त कर्मों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि समस्त कर्म प्रकृति, शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा आदि के द्वारा ही किये जाते हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा तात्पर्य यह भी स्पष्ट है कि सांख्य योगी के कर्म, जाति, धाम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार, जैसे खाना, पीना, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि, शास्त्रविहित शरीर के कर्मों द्वारा नहीं होते। ये सभी कर्म उसके द्वारा किये जा सकते हैं।
मनुष्य अपने को केवल उन्हीं कर्मों का कर्ता मानता है जिन्हें वह जानकर अर्थात् मन से करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, खाना आदि। किन्तु अनेक कर्म ऐसे भी हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना-जाना, आँखों का खोलना-बंद करना आदि। फिर इस श्लोक में इन कर्मों का कर्ता न मानने को कैसे कहा गया है? इसका उत्तर यह है कि सामान्यतः श्वास का आना-जाना आदि स्वाभाविक है, किन्तु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास आदि की क्रियाएँ जानकर करता है। इसी प्रकार आँखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसीलिए उन कर्मों का कर्ता न मानने को कहा गया है। दूसरी बात, जिस प्रकार मनुष्य मनुष्यासन (श्वास लेना, आँखें खोलना और बंद करना) – उन कर्मों को स्वाभाविक नहीं मानता और अपने को उनका कर्ता नहीं मानता, उसी प्रकार अन्य कर्मों को भी स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए और अपने को उनका कर्ता नहीं मानना चाहिए।
भगवद्गीता में भगवान क्यों कहते हैं कि स्वरूप कर्ता नहीं है?
–इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्
जब स्वरूप में कोई कर्ता नहीं है, तो कर्म कैसे और किसके द्वारा हो रहे हैं?— इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान् उपरोक्त श्लोकों में कहते हैं कि समस्त कर्म इन्द्रियों द्वारा इन्द्रियों के विषयों में हो रहे हैं। यहाँ भगवान् का अभिप्राय इन्द्रियों में उत्तर को दर्शाना नहीं, अपितु स्वरूप को कर्तापन से रहित दर्शाना है।
प्रकृति और पुरुष के संबंध को गीता कैसे समझाती है?
–नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत
यहां मैं स्वरूप से करता नहीं — इसका अर्थ यह नहीं कि मैं (स्वरूप) पहले कर्ता था। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान है, न भूतकाल था और न भविष्य में होगा। कर्म तो प्रकृति में ही हो रहा है, क्योंकि प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है और पुरुष, अर्थात् चेतन तत्त्व, सदैव निष्क्रिय रहता है। जब चेतन तत्त्व भूलवश प्रकृति के कर्म से अपनी पहचान कर लेता है, तब वह प्रकृति के कर्मों को ही अपना कर्म मानने लगता है और स्वयं उन कर्मों का कर्ता बन जाता है।
जैसे कोई व्यक्ति चलती रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा है, पर चल नहीं रहा है, परन्तु रेलगाड़ी के चलने के कारण वह बिना चले ही चल रहा है। रेलगाड़ी में चढ़ जाने मात्र से वह चलने से मुक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब वह किसी भी शरीर – स्थूल, सूक्ष्म या कारण – जो कि क्रिया प्रकृति का कार्य है, के साथ अपने को जोड़ता है, तब भले ही वह स्वयं कोई कर्म न करता हो, फिर भी वह उन शरीरों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का कर्ता बनने से बच नहीं सकता।
सांख्य योगी अपने को शरीर, इन्द्रिय, मन आदि से कभी संबंधित नहीं मानता, इसलिए वह अपने में कभी कर्मों का कर्तापन अनुभव नहीं करता। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए भोजन का पाचन, शरीर का बलवान या दुर्बल होना आदि, ये सभी कर्म स्वाभाविक रूप से (स्वतः) होते हैं, वैसे ही सांख्य योगी अन्य सभी कर्मों को स्वाभाविक रूप से होते हुए अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि वह अपने को किसी भी कर्म का कर्ता अनुभव नहीं करता।
सातवें श्लोक में कर्मयोगी के और आठवें नौवें श्लोक में संख्यायोगी के कर्मों के साथ निर्लिप्तता बता कर अब भगवान भक्तयोगी के कर्मों की निर्लिप्तता बताते हैं।
यह भी पढ़ें :
कर्मयोगी इन्द्रियों को वश में करके जीवन में क्या लाभ पाता है?











