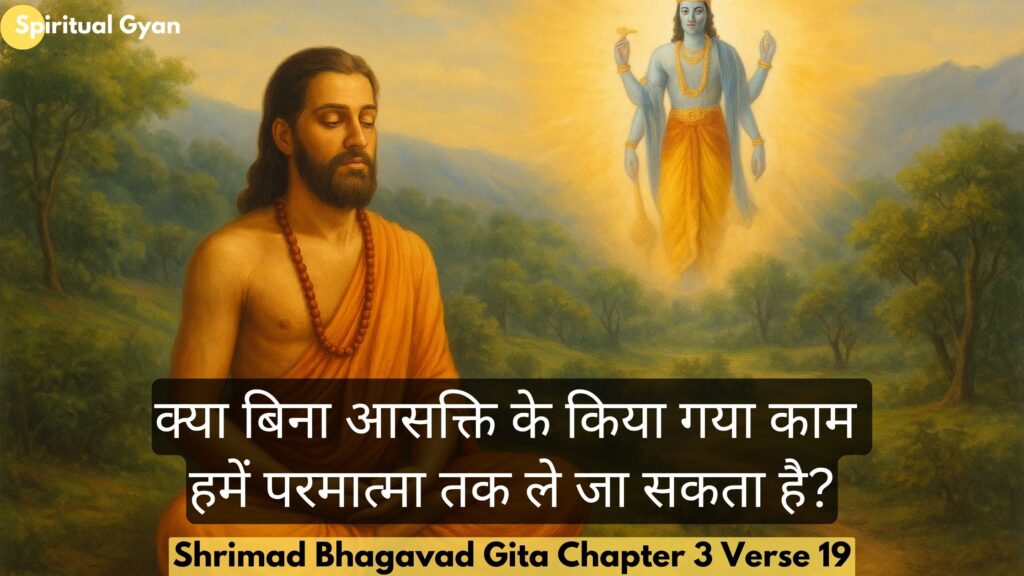
Bhagavad Gita Chapter 3 Verse 19
तस्मादसक्त: सततं कार्यं कर्म समाचर |
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष: || 19 ||
अर्थात भगवान कहते हैं, अतः तुम्हें सदैव आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का भली-भाँति पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 17 Meaning in Hindi
क्या बिना आसक्ति के किया गया काम हमें परमात्मा तक ले जा सकता है?
–तस्मादसक्त: सततं कार्यं कर्म समाचर
अपने स्वरूप से भिन्न जड पदार्थों के प्रति आकर्षण को ‘आसक्ति’ कहते हैं। आसक्ति से मुक्त होने के लिए आसक्ति का कारण जानना आवश्यक है। ‘मैं शरीर हूँ’ और ‘शरीर मेरा है’ ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों की महत्ता मन में अंकित हो जाती है। इससे आसक्ति ही पतन का कारण बनती है, कर्म नहीं।
आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जड पदार्थों के साथ अपना सम्बन्ध मानकर उनके सुख और भोग के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। इस प्रकार जड पदार्थों के साथ जो आसक्ति का सम्बन्ध माना जाता है, वही मनुष्य के बार-बार जन्म-मरण का कारण बनता है। आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने से जड पदार्थों से सम्बन्ध टूट जाता है।
संसार से प्राप्त पदार्थ (शरीर आदि) से हमने अपने लिए ही कर्म किए हैं। उन्हें हमने अपने भोग और संग्रह के लिए व्यवस्थित किया है। इसीलिए संसार का हम पर ऋण है, जिसे चुकाने के लिए संसार के हित के लिए ही कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए (फल की इच्छा से) कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त नहीं होता, बल्कि साथ ही नया ऋण निर्मित हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार-बार संसार में आना पडता है। केवल दूसरों के हित के लिए ही सभी कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से कोई नया ऋण निर्मित नहीं होता। इस प्रकार जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और कोई नया ऋण निर्मित नहीं होता, तो मनुष्य स्वतः ही मुक्त हो जाता है क्योंकि बंधन का कोई कारण नहीं रहता।
यह भी पढ़ें : क्या मनुष्य बिना कर्म के रह सकता है?
कोई भी कर्म स्थायी नहीं रहता, परन्तु वह आसक्ति (अन्तकरण) में स्थायी रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, ‘सतत्म् असक्तः’ इस पद द्वारा निरंतर आसक्ति रहित होनेके लिए। ‘मैं किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होऊँगा -‘ ऐसी भावना साधक को निरन्तर रखनी चाहिए। निरन्तर आसक्ति से मुक्त रहकर जो भी नियत कर्म उसके सामने आये, उसे कर्तव्य मानकर ही करना चाहिए – यही उपरोक्त श्लोक का तात्पर्य है।
‘कार्यम्‘ का अर्थ है कर्तव्य, जिसे हम कर सकते हैं और जिसे हमें अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ है – अपना स्वार्थ त्यागकर दूसरों का उपकार करना, अर्थात् दूसरों की अशास्त्रीय और न्यायोचित माँगों को पूरा करना, जिन्हें पूरा करने की शक्ति हममें है। इस प्रकार कर्तव्य का सम्बन्ध दूसरों के कल्याण से है।
प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य करने में स्वतंत्र और समर्थ है, कोई भी पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, आलस्य और प्रमाद के कारण, अकर्तव्य करने की बुरी आदत और फल की इच्छा के कारण वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन हो जाता है, अन्यथा कर्तव्य पालन जितना सरल कुछ भी नहीं है। कर्तव्य का सम्बन्ध परिस्थिति के अनुसार होता है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से कर्तव्य कर सकता है। कर्तव्य पालन से ही आसक्ति दूर होती है। अकर्तव्य करने और कर्तव्य न करने से आसक्ति बढती है। कर्तव्य करने से, अर्थात् दूसरों के हित के लिए कार्य करने से वर्तमान के प्रति आसक्ति दूर होती है और कुछ न चाहने से भविष्य के प्रति आसक्ति दूर होती है।
समाचार शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बहुत सावधानी, उत्साह और तत्परता से करना चाहिए। अपने कर्तव्यों के पालन में थोडी सी भी लापरवाही कर्मयोग की प्राप्ति में बाधा डाल सकती है।
क्या निष्काम कर्म ही संसार से मुक्ति का उपाय है?
–असक्तो ह्याचरन्कर्म
आसक्ति के द्वारा मनुष्य स्वयं संसार से जुडता है, संसार स्वयं नहीं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सभी कर्म संसार के हित के लिए करे तथा बदले में किसी फल की इच्छा न करे। इस प्रकार आसक्ति से मुक्त होकर अर्थात् संसार के लिए इस भावना से कर्म करने से कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, संसार से सम्बन्ध स्वतः ही टूट जाता है।
क्या हर योग का लक्ष्य एक ही परमात्मा की प्राप्ति है?
–परमाप्नोति पूरुष
जैसे 13वें अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में भगवान ने ‘परम’ शब्द से सांख्ययोगी के परमात्मा की प्राप्ति कही है, वैसे ही यहाँ ‘परः’ शब्द से कर्मयोगी के परमात्मा की प्राप्ति कही है। तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जिस मार्ग पर चले (अपनी रुचि, श्रद्धा और अनुकूलता के अनुसार) – कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग – उसे प्राप्त होने वाला विषय एक परमात्मा ही है। वह प्राप्त होने योग्य तत्त्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में कोई विकल्प, संशय या निराशा न हो तथा जो सदा, सर्वत्र, सब समयों में, सबके लिए, सबका हो तथा जिससे कोई किसी भी अवस्था में एक क्षण के लिए भी पृथक न हो सके अर्थात् जो सबको अविभाज्य रूप में सदैव प्राप्त हो।
आसक्तिरहित होकर कर्म करना अर्थात खुद के लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है?? इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं।











