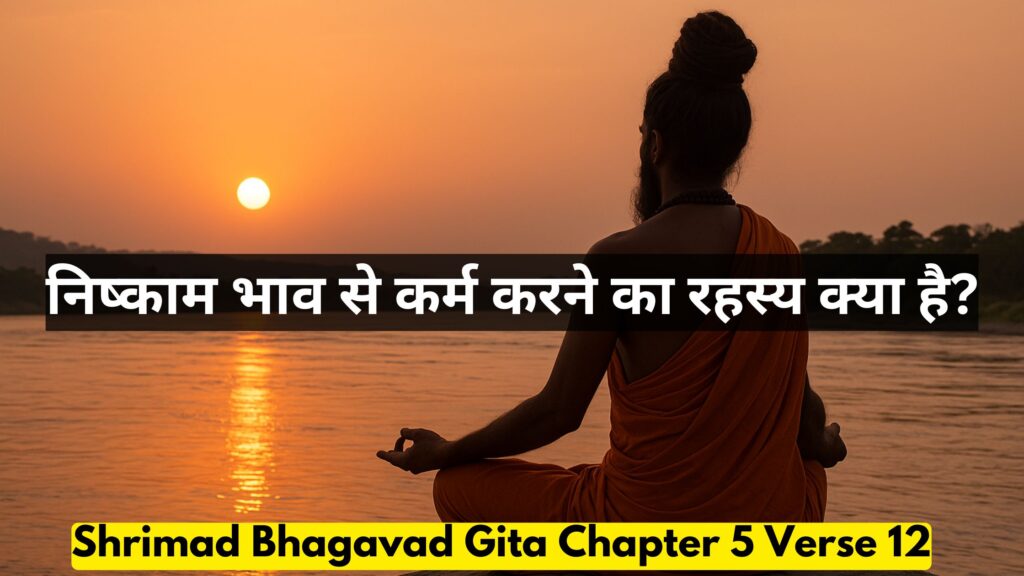
Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 12
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥
अर्थात भगवान कहते हैं, कर्मयोगी अपने कर्मों के फलों का त्याग करके आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति कामनाओं के कारण कर्मों के फलों में आसक्त हो जाता है और बंध जाता है।
Shrimad Bhagavad Gita Chapter 5 Verse 12 Meaning in hindi
निष्काम भाव से कर्म करने का रहस्य क्या है?
–कर्मफलं त्यक्त्वा
यहाँ कर्मफल के त्याग का अर्थ है फल की इच्छा का, आसक्ति का त्याग, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं, बल्कि कर्मफल की इच्छा का है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है – किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए किसी भी प्रकार का सुख पाने की किंचितमात्र भी इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तत्काल (फल) सुख मिलता है और दूसरे फलस्वरूप फल मिलता है – इन दोनों फलों की इच्छा का त्याग करना होता है। अपना कुछ न होना, अपने लिए कुछ न करना और अपने लिए कुछ न चाहना – इस प्रकार कर्ता सर्वथा निष्फल हो जाता है और कर्मफल की इच्छा का त्याग कर देता है।
संचित कर्मों के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्मों के कारण नए कर्म संस्कार संचित होते हैं। किन्तु कर्मफल की इच्छा त्यागकर कर्म करने से, कर्म भुने हुए बीजों के समान संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनका नाम ‘अकर्म’ हो जाता है। वर्तमान में निष्काम भाव से किए गए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार (संचित कर्म) भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण समाप्त हो जाता है।
कर्म फल चार प्रकार के होते हैं—
(1) कर्म के प्रत्यक्ष फल—वर्तमान में किए गए नए कर्मों के फल, जो तुरंत दिखाई देते हैं, जैसे—भोजन के बाद तृप्ति आदि।
(2) कर्म के अदृश्य फल—वर्तमान में किए गए नए कर्मों के फल, जो वर्तमान में संचित रूप में संचित हैं, लेकिन भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में प्राप्त होंगे।
(3) कर्म के प्राप्त फल—पूर्वनिर्धारित प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में प्राप्त शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि।
(4) कर्म के अप्राप्य फल—पूर्वनिर्धारित कर्म के परिणामस्वरूप भविष्य में मिलने वाली अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति।
एक साधारण व्यक्ति किसी न किसी कामना से ही कर्म आरंभ करता है और कर्म पूर्ण होने तक उसी कामना के बारे में सोचता रहता है। जैसे एक व्यापारी धन की कामना से व्यापार आरंभ करता है, तो उसका झुकाव धन के लाभ-हानि की ओर रहता है, कि लाभ हो और हानि न हो। धन प्राप्ति पर वह सुखी होता है और हानि होने पर दुःखी। इसी प्रकार, सभी मनुष्य किसी न किसी शुभ फल की कामना से कर्म करते हैं, जैसे स्त्री, पुत्र, धन, मान, यश आदि। परंतु एक कर्मयोगी फल की कामना का त्याग करके कर्म करता है।
यहाँ स्वाभाविक प्रश्न यह है कि यदि कामना ही न हो, तो कर्म क्यों करें? सबसे पहले उत्तर देने योग्य बात यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का पूर्णतः त्याग नहीं कर सकता। यदि यह मान भी लिया जाए कि मनुष्य अधिकांशतः कर्मों का त्याग कर सकता है, तो भी जब तक मनुष्य के हृदय में संसार के प्रति राग है, तब तक वह (कर्म किए बिना) शान्त नहीं रह सकता। इससे विषयों का चिंतन अवश्यम्भावी रूप से होगा, जो कर्म है। विषयों का चिंतन करते-करते वह क्रमशः पतन की ओर अग्रसर होगा। अतः जब तक राग का पूर्णतः अभाव न हो, तब तक मनुष्य कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म करने से पुराना राग दूर होता है और निष्काम भाव से, केवल लाभ के लिए कर्म करने से नया राग उत्पन्न नहीं होता।
यह भी पढ़ें : क्या संन्यास बिना कर्मयोग के संभव है?
क्या इच्छाओं का अंत ही परम शांति की शुरुआत है?
–शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्
यह सिद्ध तथ्य है कि सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों के त्याग से शांति प्राप्त होती है। जब निद्रा में संसार का विस्मरण हो जाता है, तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जाग्रत अवस्था में ही संसार का विच्छेद (इच्छाओं का त्याग) हो जाए, तो फिर कहना ही क्या! इसी प्रकार, सो जाने, किसी कार्य के पूर्ण हो जाने, कन्या का विवाह हो जाने आदि से भी शांति प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक इच्छाओं, आसक्तियों और मोहों के त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। परंतु उस शांति का भोग करने से, अर्थात् उसमें सुख लेने से और उसे ही लक्ष्य मानकर साधक उस ‘वैराग्य रूपी शांति’ अर्थात् परम शांति से वंचित रह जाता है, जो उस शांति का परिणाम है। क्योंकि वह शांति लक्ष्य नहीं, अपितु परम शांति का कारण है।
फल की आसक्ति मनुष्य को जन्म-मरण के बंधन में कैसे डालती है?
–अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते
यहाँ अयुक्तः शब्द का प्रयोग उस सकाम पुरुष के लिए किया गया है जो कर्मयोगी नहीं, बल्कि कर्मी है।
नयी कामनाओं के कारण सकाम पुरुष फल में आसक्त हो जाता है और जन्म-मरण के बंधन में पड़ जाता है। कोई भी वस्तु केवल कामना से प्राप्त नहीं होती, और यदि प्राप्त भी हो जाए, तो वह सदा हमारे पास नहीं रहती—यह सत्य होते हुए भी, वस्तुओं की कामना करना मूर्खता है। तुलसीदासजी महाराज कहते हैं—
अंतहुँ तोहि तजेंगे पामर तू न तजै अबही ते ॥
इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि पदार्थ को रूप से मुक्त कर दिया जाए, भले ही मुक्ति संभव हो, तो सभी मरने वाले मुक्त हो जाएँगे। पदार्थ स्वयं ही रूप से मुक्त हो जाते हैं। अतः, वास्तव में, उन पदार्थों में विद्यमान काम, ममता और आसक्ति को ही मुक्त करना होता है, क्योंकि काम, ममता और आसक्ति के माध्यम से पदार्थ के साथ जो संबंध बनता है, वही जन्म-मरण के बंधन का कारण है। कर्मयोग (कर्म का प्रवाह केवल दूसरों के हित के लिए होना) के अभ्यास से, यह कल्पित संबंध आसानी से मुक्त हो जाता है।
कर्म योग का वर्णन करके अब भगवान अगले श्लोक में फिर से सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं
यह भी पढ़ें :
कर्मयोगी और सामान्य मनुष्य के कर्मों में क्या अंतर है?
क्या ईश्वर को अर्पित कर्म पाप से मुक्त करते हैं?
सांख्य योगी क्यों मानता है कि मैं कुछ नहीं करता?
कर्मयोगी इन्द्रियों को वश में करके जीवन में क्या लाभ पाता है?











