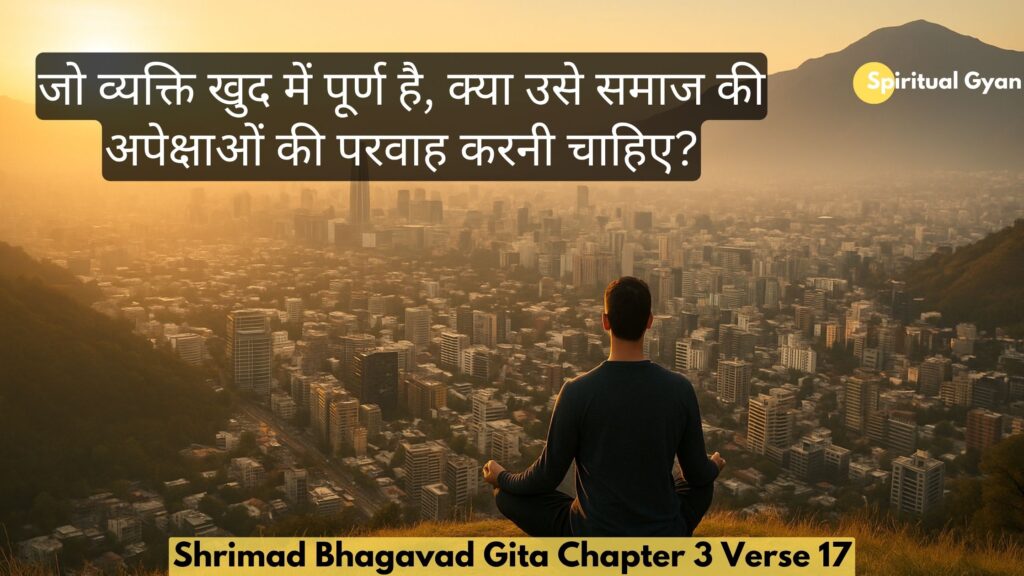
Bhagavad Gita Chapter 3 Verse 17
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव: |
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते || 17 ||
अर्थात भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है और अपने आप में संतुष्ट है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है।
shrimad Bhagavad Gita Chapter 3 Shloka 17 Meaning in Hindi
क्या सच्चा सुख संसार में नहीं, आत्मा में छिपा है?
–यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव:आत्मन्येव च सन्तुष्ट
मनुष्य जब तक संसार से अपना सम्बन्ध मानता है, तब तक वह इन्द्रियों के भोगों में तथा स्त्री, पुत्र, परिवार आदि में अपनी रति, भोजन (अन्न-जल) में तृप्ति तथा धन में तृप्ति मानता है। किन्तु इससे उसका प्रेम, तृप्ति तथा संतोष कभी पूर्ण नहीं होता, न ही वह स्थिर रहता है। क्योंकि संसार नित्य परिवर्तनशील, जड तथा नाशवान है और ‘स्वम’ सदैव निश्चित, चेतन तथा अविनाशी है। तात्पर्य यह है कि ‘स्वम’ का संसार से किंचितमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। अतः संसार में स्व का प्रेम, तृप्ति तथा संतोष कैसे हो सकता है?
हम सबका अनुभव है कि इस संसार में किसी भी मनुष्य का प्रेम चिरस्थायी नहीं रहता। विवाह के समय स्त्री-पुरुष के बीच जो प्रेम या आकर्षण होता है, वह एक-दो बच्चे होने के बाद नहीं रहता। कुछ स्त्रियाँ तो अपने वृद्ध पतियों के बारे में कहती हैं कि अब यह वृद्ध मर जाए तो अच्छा! भोजन करने से जो ‘संतुष्टि’ होती है, वह भी थोडे समय के लिए होती है, धन प्राप्त करने से जो ‘संतुष्टि’ होती है, वह भी क्षणभंगुर होती है, क्योंकि धन की चाह कदम-दर-कदम बढती रहती है। इसीलिए अभाव निरंतर बना रहता है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में प्रेम, संतुष्टि और संतोष कभी भी स्थायी नहीं रह सकते।
सांसारिक पदार्थों में मनुष्य को प्रेम, संतोष और तृप्ति का केवल आभास होता है, वास्तव में वे होते ही नहीं, यदि होते तो फिर अरिती, अतृप्ति और असंतोष न होते। प्रेम, संतोष और तृप्ति रूप से स्वयंसिद्ध हैं। रूप सत्य है। उसमें कभी अभाव नहीं होता- ‘नाभावो विद्यते सतः’ (गीता Ch 2/16) और अभाव के बिना कामना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए रूप में कामनारहितता स्वयंसिद्ध है। परंतु जब जीवात्मा भ्रमवश संसार से अपना संबंध मान लेता है, तब वह संसार में प्रेम, संतोष और तृप्ति ढूँढ़ने लगता है और उसके लिए सांसारिक पदार्थों की कामना करने लगता है। किसी वस्तु (धन आदि) की कामना करने के पश्चात जब मन की कामना समाप्त हो जाती है (दूसरी कामना उत्पन्न होने से पहले) तो उसकी स्थिति शून्य हो जाती है और वह उस शून्यता से सुख अनुभव करता है, परंतु मनुष्य भ्रमवश उस सुख को सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है और उस सुख को प्रेम, संतोष और तृप्ति के रूप में पहचान लेता है। यदि वह सुख किसी वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न होता तो उस वस्तु को पाकर वह सदा सुखी रहता, कभी दुःख नहीं होता और उस वस्तु की फिर इच्छा उत्पन्न नहीं होती। परन्तु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी पूर्ण (सदा के लिए) प्रेम, तृप्ति और संतोष प्राप्त न हो पाने के कारण तथा संसार के साथ आसक्ति का सम्बन्ध निरन्तर बना रहने के कारण उसे फिर से नई-नई इच्छाएँ होने लगती हैं। इच्छा उत्पन्न होने पर उसे अपने में कमी का अनुभव होता है और इच्छित वस्तु मिल जाने पर उसे अपने में पराधीनता का अनुभव होता है। अतः इच्छायुक्त व्यक्ति सदैव दुःखी रहता है।
यह भी पढ़ें : अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करें?
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि साधक का मानना है कि सुख का मूल कारण शून्यता है और दुख का कारण इच्छा है, लेकिन संसार में आसक्त व्यक्ति का मानना है कि सुख वस्तुओं की प्राप्ति से होता है और दुख वस्तुओं की अप्राप्ति से होता है। यदि आसक्त व्यक्ति भी साधक के समान सत्य दृष्टि से वस्तुओं को देखे तो वह प्रत्यक्ष रूप से शून्यता/स्वयंसिद्ध शून्यता का अनुभव कर सकता है।
जो व्यक्ति खुद में पूर्ण है, क्या उसे समाज की अपेक्षाओं की परवाह करनी चाहिए?
–तस्य कार्यं न विद्यते
मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य निर्धारित है, उसका उद्देश्य परम पुरुषोत्तम कल्याण की प्राप्ति है। जब किसी भी साधन (कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग) से उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, तो मनुष्य के लिए करने, जानने या प्राप्त करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता, यही मानव जीवन की परम सफलता है।
यद्यपि मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में कोई कमी नहीं है, फिर भी जब तक वह संसार के साथ सम्बन्ध के कारण अपनी कमी को समझते हुए तथा शरीर को ‘मैं’ और ‘मेरा’ मानते हुए ‘अपने लिए’ कर्म करता रहता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य बना रहता है। किन्तु जब वह अपने लिए कुछ नहीं करता तथा ‘दूसरों के लिए’ अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, आत्मा, माता, पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार, समाज, देश तथा संसार के लिए सब कर्म करता है, तब संसार से उसका सम्बन्ध टूट जाता है। संसार से सम्बन्ध पूरी तरह टूट जाने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। क्योंकि कोई भी कर्म रूप में नहीं होता, जो भी कर्म होता है, वह संसार के सम्बन्ध से तथा सांसारिक पदार्थों के द्वारा ही होता है। इसलिए जिनका संसार से सम्बन्ध है, उनका कर्तव्य है।
यह तस्य कार्यं न विद्यते का अर्थ यह नहीं है कि उस महापुरुष द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। करने को कुछ शेष न रहने पर भी उस महापुरुष द्वारा लोकहितार्थ स्वतः ही कार्य किए जाते हैं। जैसे पलकों का उठना-गिरना, श्वासों का आना-जाना, भोजन का पचना आदि कार्य स्वतः ही (प्रकृति में) होते हैं, वैसे ही शास्त्रविहित समस्त आदर्श कार्य भी उस महापुरुष द्वारा (स्वाभिमान के अभाव के कारण) स्वतः ही किए जाते हैं।











